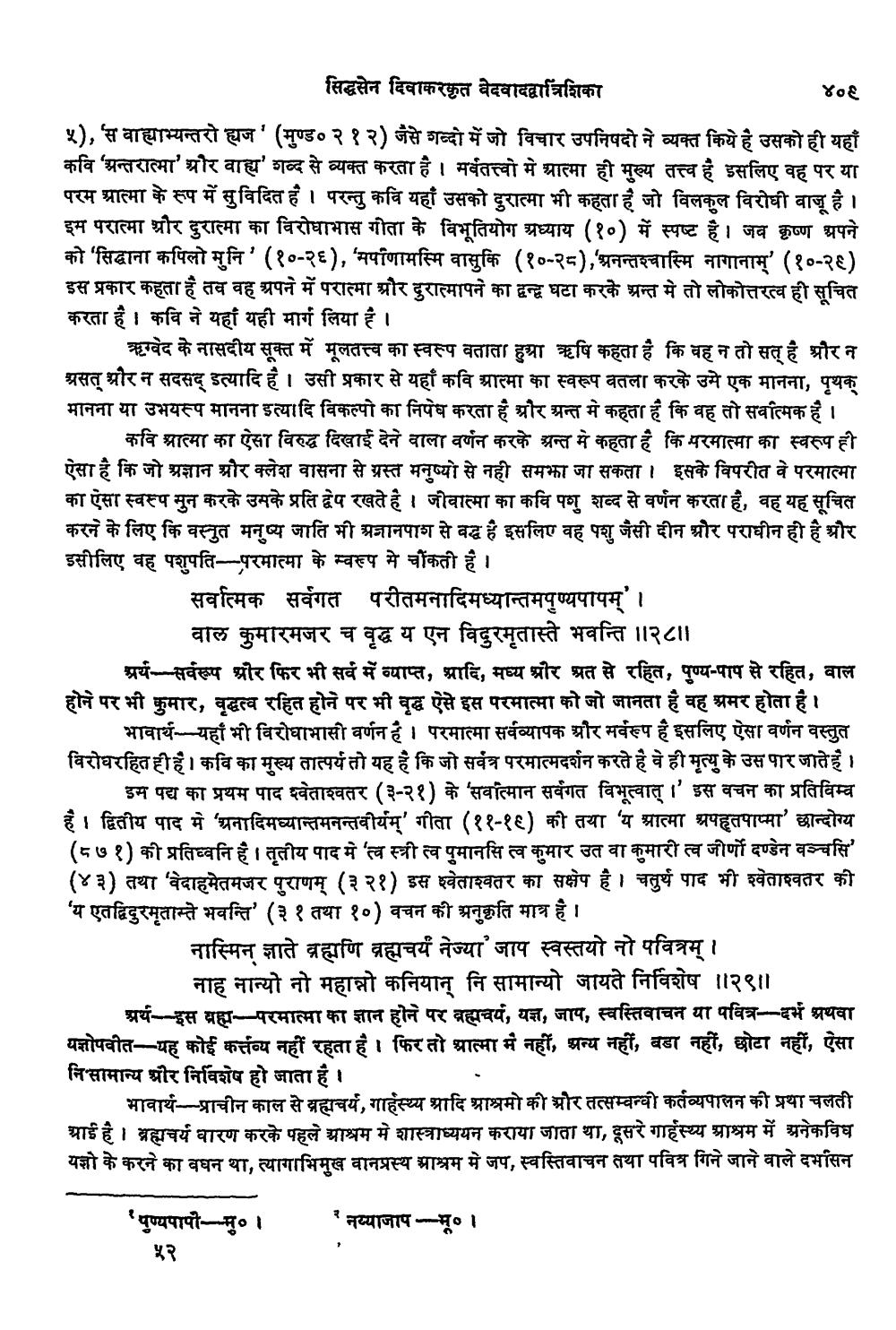________________
सिद्धसेन दिवाकरकृत वेदवादद्वात्रिशिका
૪૨
५), 'स' वाह्याभ्यन्तरो ह्यज' (मुण्ड० २१२) जैसे शब्दो में जो विचार उपनिषदो ने व्यक्त किये है उसको ही यहाँ कवि 'अन्तरात्मा' और वाह्य' शब्द से व्यक्त करता है । मर्वतत्त्वो मे श्रात्मा ही मुख्य तत्त्व है इसलिए वह पर या परम श्रात्मा के रूप में सुविदित है । परन्तु कवि यहाँ उसको दुरात्मा भी कहता है जो विलकुल विरोधी बाजू है । इम परात्मा और दुरात्मा का विरोधाभास गीता के विभूतियोग अध्याय (१०) में स्पष्ट है । जव कृष्ण अपने को 'सिद्धाना कपिलो मुनि ' (१०-२६), 'मर्पाणामस्मि वासुकि ( १०-२८), अनन्तश्चास्मि नागानाम्' ( १०-२६) इस प्रकार कहता है तब वह अपने में परात्मा और दुरात्मापने का द्वन्द्व घटा करके अन्त में तो लोकोत्तरत्व ही सूचित करता है । कवि ने यहाँ यही मार्ग लिया है ।
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मूलतत्त्व का स्वरूप बताता हुया ऋषि कहता है कि वह न तो सत् है और न असत् श्रौर न सदसद् इत्यादि है । उसी प्रकार से यहाँ कवि आत्मा का स्वरूप बतला करके उसे एक मानना, पृथक् मानना या उभयरूप मानना इत्यादि विकल्पो का निषेध करता है और अन्त मे कहता है कि वह तो सर्वात्मक है । कवि आत्मा का ऐसा विरुद्ध दिखाई देने वाला वर्णन करके अन्त मे कहता है कि परमात्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि जो अज्ञान और क्लेश वासना से ग्रस्त मनुष्यों से नही समझा जा सकता। इसके विपरीत वे परमात्मा का ऐसा स्वरूप मुन करके उसके प्रति द्वेष रखते है । जीवात्मा का कवि पशु शब्द से वर्णन करता है, वह यह सूचित करने के लिए कि वस्तुत मनुष्य जाति भी अज्ञानपाग से बद्ध है इसलिए वह पशु जैसी दीन और पराधीन ही है और इसीलिए वह पशुपति --- परमात्मा के स्वरूप मे चौंकती है ।
सर्वात्मक सर्वगत परीतमनादिमध्यान्तमपुण्यपापम्' ।
वाल कुमारमजर च वृद्ध य एन विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २८ ॥
अर्थ-सर्वरूप और फिर भी सर्व में व्याप्त, आदि, मध्य और प्रत से रहित, पुण्य-पाप से रहित, वाल होने पर भी कुमार, वृद्धत्व रहित होने पर भी वृद्ध ऐसे इस परमात्मा को जो जानता है वह अमर होता है । भावार्थ-यहाँ भी विरोधाभासी वर्णन है । परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वरूप है इसलिए ऐसा वर्णन वस्तुत विरोधरहित ही है । कवि का मुख्य तात्पर्य तो यह है कि जो सर्वत्र परमात्मदर्शन करते है वे ही मृत्यु के उस पार जाते हैं । इस पद्य का प्रथम पाद श्वेताश्वतर (३-२१) के 'सर्वात्मान सर्वगत विभूत्वात् ।' इस वचन का प्रतिविम्व है । द्वितीय पाद में 'श्रनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्' गीता ( ११-१९ ) की तया 'य आत्मा अपहृतपाप्मा' छान्दोग्य (८७१ ) की प्रतिध्वनि है। तृतीय पाद में 'त्व स्त्री त्व पुमानसि त्व कुमार उत वा कुमारीत्व जीर्णो दण्डेन वञ्चसि (४३) तथा 'वेदाहमेतमजर पुराणम् (३२१ ) इस श्वेताश्वतर का सक्षेप है । चतुर्थ पाद भी श्वेताश्वतर की 'य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति' ( ३१ तथा १० ) वचन की अनुकृति मात्र है ।
नास्मिन् ज्ञाते ब्रह्मणि ब्रह्मचर्यं नेज्या' जाप स्वस्तयो नो पवित्रम् ।
नाह नान्यो नो महानो कनियान् नि सामान्यो जायते निर्विशेष ॥ २९ ॥
अर्थ - इस ब्रह्म- परमात्मा का ज्ञान होने पर ब्रह्मचर्य, यज्ञ, जाप, स्वस्तिवाचन या पवित्र --दर्भ अथवा यज्ञोपवीत -- यह कोई कर्तव्य नहीं रहता है । फिर तो श्रात्मा में नहीं, अन्य नहीं, बडा नहीं, छोटा नहीं, ऐसा निसामान्य और निर्विशेष हो जाता है ।
भावार्थ --- प्राचीन काल से ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य श्रादि श्राश्रमो की और तत्सम्वन्धी कर्तव्यपालन की प्रथा चलती आई है । ब्रह्मचर्य धारण करके पहले आश्रम में शास्त्राध्ययन कराया जाता था, दूसरे गार्हस्थ्य श्राश्रम में अनेकविध यज्ञो के करने का वघन था, त्यागाभिमुख वानप्रस्थ आश्रम मे जप, स्वस्तिवाचन तथा पवित्र गिने जाने वाले दर्भासन
'पुण्यपापी - मु० । ५२
२
नय्याजाप म० ।