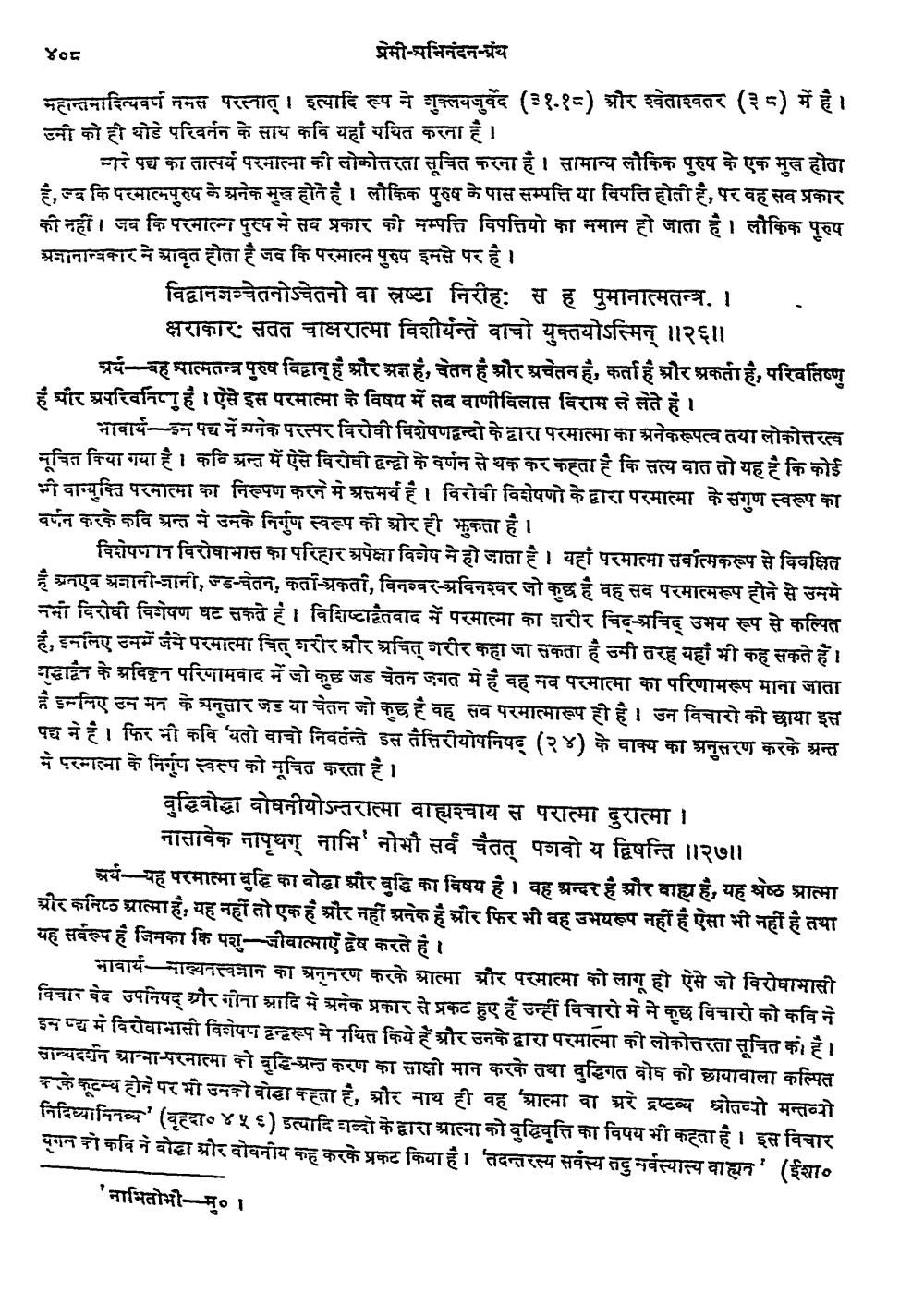________________
प्रेमी-अभिनंदन ग्रंथ
महान्तनादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । इत्यादि रूप ने शुक्लयजुर्वेद (३१.१८) और श्वेताश्वतर (३८) में है । उनी को ही थोडे परिवर्तन के साथ कवि यहाँ यथित करना है ।
४०८
गरे पद्य का तात्पर्य परमात्ना की लोकोत्तरता सूचित करना है । सामान्य लौकिक पुरुष के एक मुख होता हैं, जब कि परमात्मपुरुष के अनेक मुख होते हैं । लौकिक पुरुष के पास सम्पत्ति या विपत्ति होती है, पर वह सब प्रकार की नहीं। जब कि परमात्य पुरुष ने सब प्रकार को नम्पत्ति विपत्तियो का नमान हो जाता है । लौकिक पुरुष अज्ञानान्त्रकार ने आवृत होता है जब कि परमात्न पुरुष इनसे पर है ।
विद्वानज्ञञ्चेतनोऽचेतनो वा स्रष्टा निरीहः सह पुमानात्मतन्त्र । क्षराकारः ततत चाक्षरात्मा विशीर्यन्ते वाचो युक्तयोऽस्मिन् ॥२६॥
अयं -- वह प्रात्मतन्त्र पुरुष विद्वान् है और अज्ञ है, चेतन है और अचेतन है, कर्ता है और अकती है, परिवर्तिष्णु परि है। ऐसे इस परमात्मा के विषय में सब वाणीविलास विराम ले लेते हैं ।
भावार्थ-इन पद्य में अनेक परस्पर विरोधी विशेषणद्वन्दो के द्वारा परमात्मा का अनेकरूपत्व तथा लोकोत्तरत्व नूचित किया गया है । कवि अन्त में ऐसे विरोवी द्वन्द्वो के वर्णन से थक कर कहता है कि सत्य बात तो यह है कि कोई भी वान्युक्ति परमात्मा का निरूपण करने में असमर्थ है । विरोवी विशेषणो के द्वारा परमात्मा के सगुण स्वरूप का वर्णन करके कवि अन्त ने उनके निर्गुण स्वरूप की ओर ही झुकता है ।
विशेषणान विशेषाभास का परिहार अपेक्षा विशेष ने हो जाता है । यहाँ परमात्मा सर्वात्मकरूप से विवक्षित है अतएव अज्ञानी-ज्ञानी, ज्ड-चेतन, कर्ता-कर्ता, विनश्वर-अविनश्वर जो कुछ है वह सव परमात्मरूप होने से उनमे नमी विरोधी विशेषण घट सकते हैं । विशिष्टाद्वैतवाद में परमात्मा का शरीर चिचिद् उभय रूप से कल्पित हैं, इसलिए उनमें जैने परमात्मा चित् शरीर और अचित् शरीर कहा जा सकता है उसी तरह यहाँ भी कह सकते हैं । शुद्धाद्वैन के अविकृत परिणामवाद में जो कुछ जड चेतन जगत में हैं वह नव परमात्मा का परिणामरूप माना जाता है इसलिए उन मत के अनुसार जड या चेतन जो कुछ है वह सव परमात्मारूप ही है । उन विचारो को छाया इस पद्य ने हैं। फिर भी कवि 'यतो वाचो निवर्तन्ते इस तैत्तिरीयोपनिषद् (२४) के वाक्य का अनुसरण करके अन्त ने परमात्ना के निर्गुण स्वरुप को सूचित करता है ।
वुद्धिवोद्धा वोघनीयोऽन्तरात्मा बाह्यश्चाय स परात्मा दुरात्मा । नासावेक नापृथग् नाभि' नोभौ सर्वं चैतत् पावो य द्विषन्ति ॥२७॥
अर्थ ——यह परमात्मा बुद्धि का बोद्धा और बुद्धि का विषय है। वह अन्दर है और वाह्य है, यह श्रेष्ठ श्रात्मा और कनिष्ठ श्रात्मा है, यह नहीं तो एक है और नहीं अनेक है और फिर भी वह उभयरूप नहीं है ऐसा भी नहीं है तथा यह सर्वरूप है जिनका कि पशु — जीवात्माएँ द्वेष करते हैं ।
भावार्य—नाख्यतत्त्वज्ञान का अनुकरण करके आत्मा और परमात्मा को लागू हो ऐसे जो विरोधाभासी विचार वेद उपनिषद् और गोना आदि में अनेक प्रकार से प्रकट हुए हैं उन्हीं विचारो मे ने कुछ विचारो को कवि ने इन पद्य में विरोवाभासी विशेषण हद्वरूप ने रथित किये हैं और उनके द्वारा परमात्मा की लोकोत्तरता सूचित की है। नान्यदर्शन यान्ना-परमात्मा को वृद्धि-अन्त करण का साक्षी मान करके तथा बुद्धिगत बोष को छायावाला कल्पित करके कूटम्य होने पर भी उनको बोद्धा कहता है, और नाथ ही वह 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यानितव्य' (वृदा० ४ ५ ६ ) इत्यादि बन्दो के द्वारा आत्मा को बुद्धिवृत्ति का विषय भी कहता है । इस विचार युगल को कवि ने बोद्धा और वोवनीय कह करके प्रकट किया है । 'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यत' (ईशा०
'नाभितोभी
-म० ।