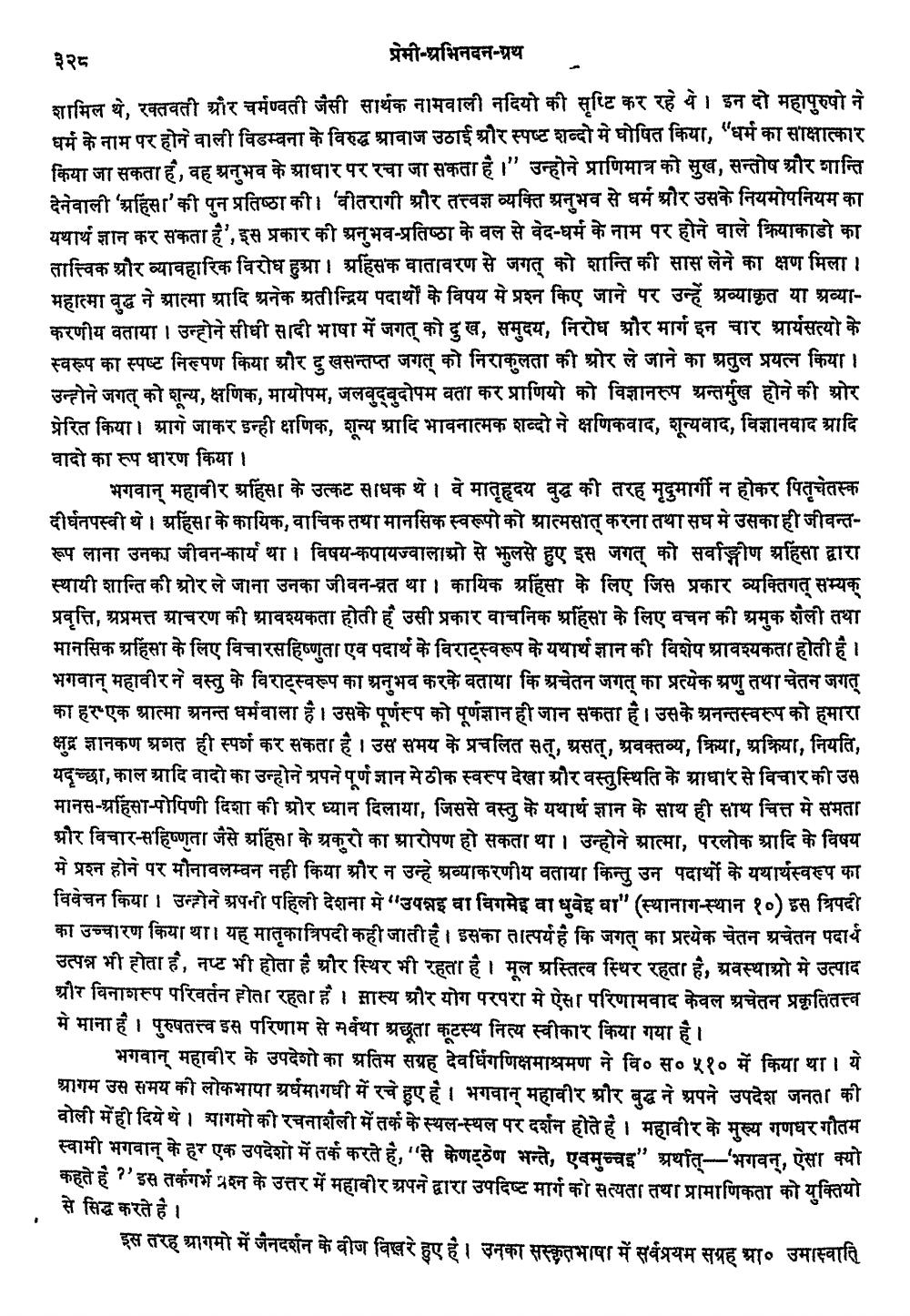________________
३२८
प्रेमी-अभिनदन-प्रथ शामिल थे, रक्तवती और चर्मण्वती जैसी सार्थक नामवाली नदियो की सृष्टि कर रहे थे। इन दो महापुरुषो ने धर्म के नाम पर होने वाली विडम्वना के विरुद्ध आवाज उठाई और स्पष्ट शब्दो मे घोषित किया, "धर्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, वह अनुभव के आधार पर रचा जा सकता है।" उन्होने प्राणिमात्र को सुख, सन्तोष और शान्ति देनेवाली अहिंसा' की पुन प्रतिष्ठा की। 'वीतरागी और तत्त्वज्ञ व्यक्ति अनुभव से धर्म और उसके नियमोपनियम का यथार्थ ज्ञान कर सकता है', इस प्रकार की अनुभव-प्रतिष्ठा के वल से वेद-धर्म के नाम पर होने वाले क्रियाकाडो का तात्त्विक और व्यावहारिक विरोध हुआ। अहिंसक वातावरण से जगत् को शान्ति की सास लेने का क्षण मिला। महात्मा बुद्ध ने आत्मा आदि अनेक अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय मे प्रश्न किए जाने पर उन्हें अव्याकृत या अव्याकरणीय बताया। उन्होने सीधी सादी भाषा में जगत् को दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग इन चार आर्यसत्यो के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण किया और दुःखसन्तप्त जगत् को निराकुलता की ओर ले जाने का अतुल प्रयत्न किया। उन्होने जगत् को शून्य, क्षणिक, मायोपम, जलबुद्बुदोपम बता कर प्राणियो को विज्ञानरूप अन्तर्मुख होने की ओर प्रेरित किया। आगे जाकर इन्ही क्षणिक, शून्य आदि भावनात्मक शब्दो ने क्षणिकवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि वादो का रूप धारण किया।
___भगवान् महावीर अहिंसा के उत्कट साधक थे। वे मातृहृदय बुद्ध की तरह मृदुमार्गी न होकर पितृचेतस्क दीर्घतपस्वी थे। अहिंसा के कायिक, वाचिक तथा मानसिक स्वरूपो को आत्मसात् करना तथा सघ मे उसका ही जीवन्तरूप लाना उनका जीवन-कार्य था। विषय-कपायज्वालामओ से झुलसे हुए इस जगत् को सर्वाङ्गीण अहिंसा द्वारा स्थायी शान्ति की ओर ले जाना उनका जीवन-व्रत था। कायिक अहिंसा के लिए जिस प्रकार व्यक्तिगत् सम्यक् प्रवृत्ति, अप्रमत्त आचरण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वाचनिक अहिंसा के लिए वचन की अमुक शैली तथा मानसिक अहिंसा के लिए विचारसहिष्णुता एव पदार्थ के विराट्स्वरूप के यथार्थ ज्ञान की विशेष आवश्यकता होती है । भगवान् महावीर ने वस्तु के विराट्स्वरूप का अनुभव करके बताया कि अचेतन जगत् का प्रत्येक अणु तथा चेतन जगत् का हर एक आत्मा अनन्त धर्मवाला है। उसके पूर्णस्प को पूर्णज्ञान ही जान सकता है। उसके अनन्तस्वरूप को हमारा क्षुद्र ज्ञानकण अगत ही स्पर्ण कर सकता है । उस समय के प्रचलित सत्, असत्, प्रवक्तव्य, क्रिया, प्रक्रिया, नियति, यदृच्छा, काल अादि वादो का उन्होने अपने पूर्ण ज्ञान मेठीक स्वरूप देखा और वस्तुस्थिति के आधार से विचार की उस मानस-अहिंसा-पोपिणी दिशा की ओर ध्यान दिलाया, जिससे वस्तु के यथार्थ ज्ञान के साथ ही साथ चित्त मे समता और विचार-साहिष्णुता जैसे अहिंसा के अकुरो का प्रारोपण हो सकता था। उन्होने आत्मा, परलोक आदि के विषय मे प्रश्न होने पर मौनावलम्वन नहीं किया और न उन्हे अव्याकरणीय वताया किन्तु उन पदार्थों के यथार्थस्वरूप का विवेचन किया। उन्होने अपनी पहिलो देशना मे "उपन्नइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा" (स्थानाग-स्थान १०) इस त्रिपदी का उच्चारण किया था। यह मातृकात्रिपदी कही जाती है। इसका तात्पर्य है कि जगत् का प्रत्येक चेतन अचेतन पदार्थ उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और स्थिर भी रहता है। मूल अस्तित्व स्थिर रहता है, अवस्थानो मे उत्पाद
और विनाशरूप परिवर्तन होता रहता है। सास्य और योग परपरा मे ऐसा परिणामवाद केवल अचेतन प्रकृतितत्त्व मे माना है। पुरुषतत्त्व इस परिणाम से सर्वथा अछूता कूटस्थ नित्य स्वीकार किया गया है।
भगवान् महावीर के उपदेशो का अतिम सग्रह देवर्धिगणिक्षमाश्रमण ने वि० स० ५१० में किया था। ये अागम उस समय की लोकभापा अर्धमागधी में रचे हुए है। भगवान महावीर और बुद्ध ने अपने उपदेश जनता की वोली में ही दिये थे। भागमो की रचनाशैली में तर्क के स्थल-स्थल पर दर्शन होते है। महावीर के मुख्य गणधर गौतम स्वामी भगवान् के हर एक उपदेशो में तर्क करते है, "से केणठेण भन्ते, एवमुच्चइ" अर्थात्-'भगवन्, ऐसा क्यों कहते है ?' इस तर्कगर्भ प्रश्न के उत्तर में महावीर अपने द्वारा उपदिष्ट मार्ग को सत्यता तथा प्रामाणिकता को युक्तियों से सिद्ध करते है।
इस तरह आगमो में जैनदर्शन के बीज विखरे हुए है। उनका सस्कृतभाषा में सर्वप्रयम सग्रह प्रा० उमास्वाति