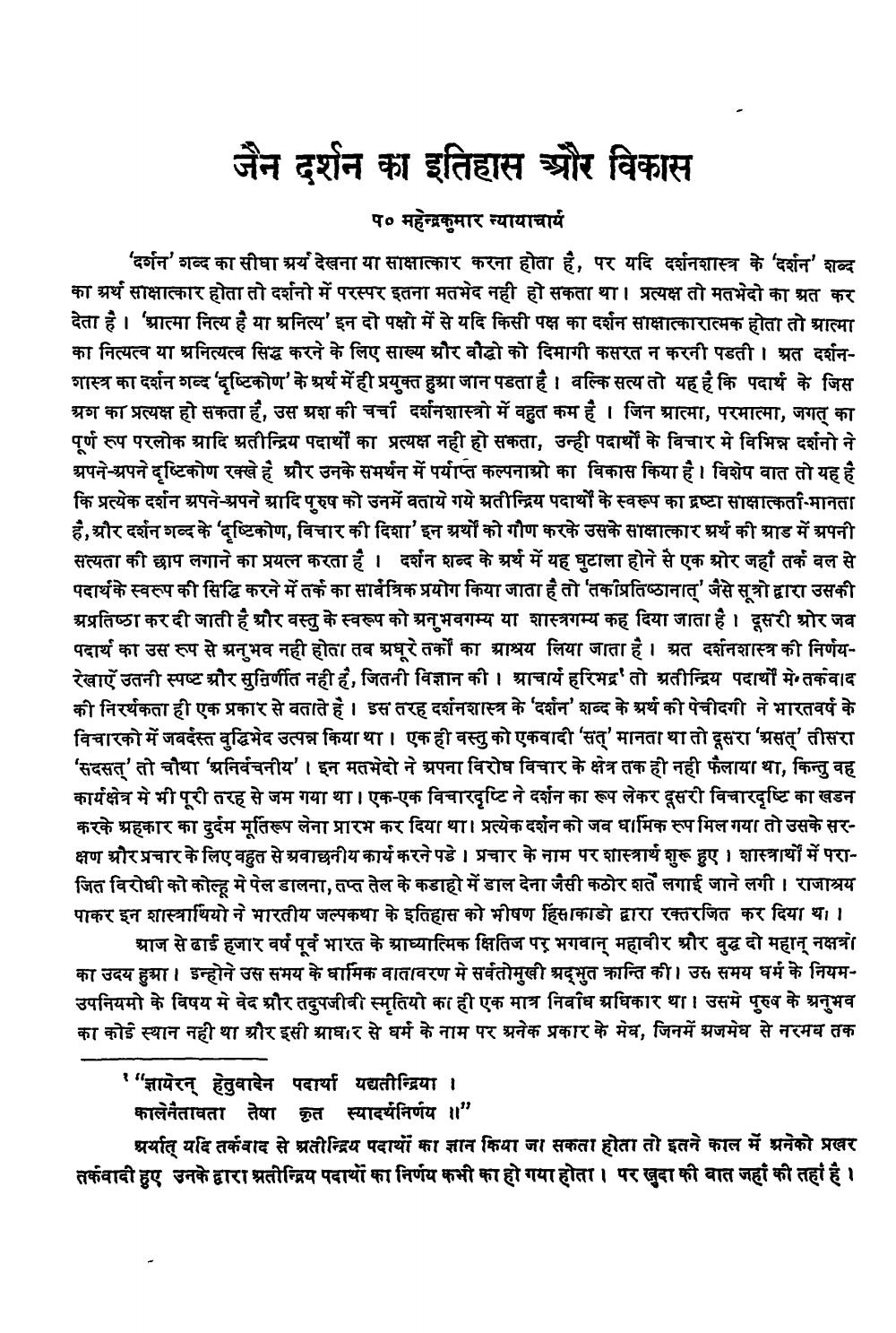________________
जैन दर्शन का इतिहास और विकास
प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य
'दर्शन' शब्द का सीधा अर्थ देखना या साक्षात्कार करना होता है, पर यदि दर्शनशास्त्र के 'दर्शन' शब्द अर्थ साक्षात्कार होता तो दर्शनों में परस्पर इतना मतभेद नही हो सकता था । प्रत्यक्ष तो मतभेदो का श्रत कर देता है । 'आत्मा नित्य है या अनित्य' इन दो पक्षो में से यदि किसी पक्ष का दर्शन साक्षात्कारात्मक होता तो आत्मा का नित्यत्व या अनित्यत्व सिद्ध करने के लिए साख्य और बौद्धो को दिमागी कसरत न करनी पडती । अत दर्शनशास्त्र का दर्शन शब्द 'दृष्टिकोण' के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ जान पडता है । वल्कि सत्य तो यह है कि पदार्थ के जिस अग का प्रत्यक्ष हो सकता है, उस प्रश की चर्चा दर्शनशास्त्रो में बहुत कम है । जिन श्रात्मा, परमात्मा, जगत् का पूर्ण रूप परलोक आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष नही हो सकता, उन्ही पदार्थों के विचार में विभिन्न दर्शनो ने अपने-अपने दृष्टिकोण रक्खे है और उनके समर्थन में पर्याप्त कल्पनाओ का विकास किया है । विशेष बात तो यह है कि प्रत्येक दर्शन अपने-अपने आदि पुरुष को उनमें बताये गये अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप का द्रष्टा साक्षात्कर्ता-मानता है, और दर्शन शब्द के 'दृष्टिकोण, विचार की दिशा' इन अर्थों को गौण करके उसके साक्षात्कार अर्थ की आड में अपनी सत्यता की छाप लगाने का प्रयत्न करता है । दर्शन शब्द के अर्थ में यह घुटाला होने से एक ओर जहाँ तर्क बल से पदार्थके स्वरूप की सिद्धि करने में तर्क का सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है तो 'तक प्रतिष्ठानात्' जैसे सूत्रो द्वारा उसकी अप्रतिष्ठा कर दी जाती है और वस्तु के स्वरूप को अनुभवगम्य या शास्त्रगम्य कह दिया जाता है । दूसरी ओर जव पदार्थ का उस रूप से अनुभव नही होता तब अधूरे तर्कों का आश्रय लिया जाता है । अत दर्शनशास्त्र की निर्णयरेखाएँ उतनी स्पष्ट और सुनिर्णीत नही है, जितनी विज्ञान की । श्राचार्य हरिभद्र' तो अतीन्द्रिय पदार्थों मे तर्कवाद
निरर्थकता ही एक प्रकार से बताते है । इस तरह दर्शनशास्त्र के 'दर्शन' शब्द के अर्थ की पेचीदगी ने भारतवर्ष के विचारको में जबर्दस्त वुद्धिभेद उत्पन्न किया था । एक ही वस्तु को एकवादी 'सत्' मानता था तो दूसरा 'असत्' तीसरा 'सदसत्' तो चौथा 'अनिर्वचनीय' । इन मतभेदो ने अपना विरोध विचार के क्षेत्र तक ही नही फैलाया था, किन्तु वह कार्यक्षेत्र मे भी पूरी तरह से जम गया था। एक-एक विचारदृष्टि ने दर्शन का रूप लेकर दूसरी विचारदृष्टि का खन करके अहकार का दुर्दम मूर्तिरूप लेना प्रारंभ कर दिया था। प्रत्येक दर्शन को जब धार्मिक रूप मिल गया तो उसके सरक्षण और प्रचार के लिए वहुत से प्रवाछनीय कार्य करने पडे । प्रचार के नाम पर शास्त्रार्थं शुरू हुए। शास्त्रार्थों में पराजित विरोधी को कोल्हू मे पेल डालना, तप्त तेल के कडाहो में डाल देना जैसी कठोर शर्तें लगाई जाने लगी । राजाश्रय पाकर इन शास्त्रार्थियो ने भारतीय जल्पकथा के इतिहास को भीषण हिंसाकाडो द्वारा रक्तरजित कर दिया था । आज से ढाई हजार वर्षं पूर्व भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर भगवान् महावीर और बुद्ध दो महान् नक्षत्रो का उदय हुआ। इन्होने उस समय के धार्मिक वातावरण मे सर्वतोमुखी अद्भुत क्रान्ति की। उस समय धर्म के नियमउपनियमो के विषय मे वेद और तदुपजीवी स्मृतियो का ही एक मात्र निर्वाध अधिकार था । उसमें पुरुष के अनुभव का कोई स्थान नही था और इसी आधार से धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के मेव, जिनमें अजमेध से नरमव तक
"ज्ञायेरन् हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रिया ।
कालेनैतावता तेषा कृत स्यादर्थनिर्णय ॥"
श्रर्यात् यदि तर्कवाद से प्रतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान किया जा सकता होता तो इतने काल में अनेको प्रखर तर्कवादी हुए उनके द्वारा श्रतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय कभी का हो गया होता । पर ख़ुदा की बात जहाँ की तहां है ।