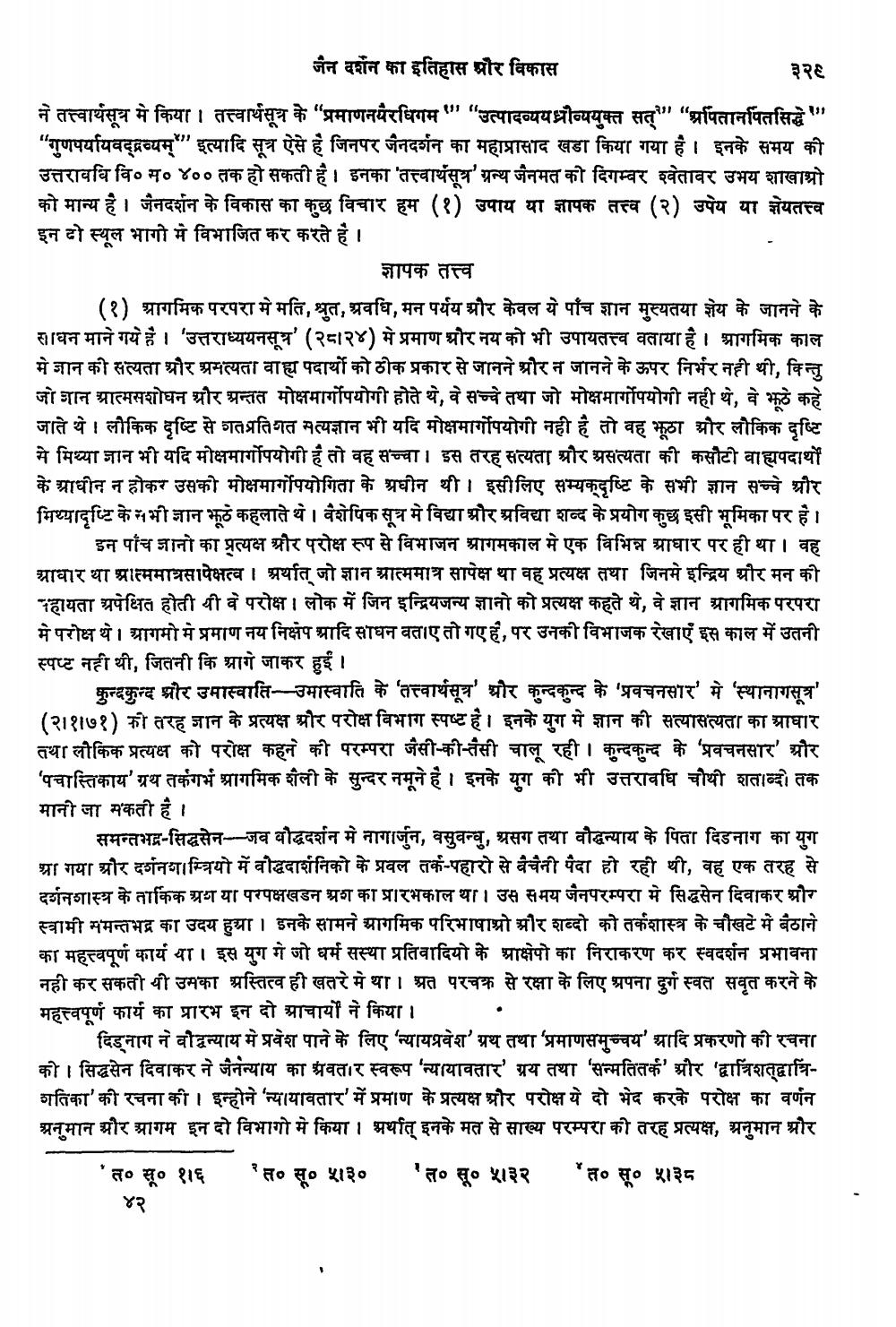________________
जैन दर्शन का इतिहास और विकास
३२६
ने तत्त्वार्थसूत्र मे किया । तत्त्वार्थसूत्र के "प्रमाणनयैरधिगम " "उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त सत्" "अपितानपतसिद्धे " “गुणपर्यायवद्द्द्रव्यम्” इत्यादि सूत्र ऐसे है जिनपर जैनदर्शन का महाप्रासाद खडा किया गया है । इनके समय की उत्तरावधि वि० स० ४०० तक हो सकती है। इनका 'तत्त्वार्थसूत्र' ग्रन्थ जैनमत की दिगम्बर श्वेतावर उभय शाखाश्रो को मान्य है । जैनदर्शन के विकास का कुछ विचार हम (१) उपाय या ज्ञापक तत्त्व (२) उपेय या ज्ञेयतत्त्व इन दो स्थूल भागो में विभाजित कर करते है ।
।
ज्ञापक तत्त्व
(१) श्रागमिक परपरा में मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ये पाँच ज्ञान मुख्यतया ज्ञेय के जानने के सावन माने गये है । 'उत्तराध्ययनसूत्र' ( २८|२४ ) मे प्रमाण और नय को भी उपायतत्त्व वताया है । श्रागमिक काल ज्ञान की सत्यता और श्रमत्यता वाह्य पदार्थों को ठीक प्रकार से जानने और न जानने के ऊपर निर्भर नही थी, किन्तु जो ज्ञान आत्मसशोधन और अन्तत मोक्षमार्गोपयोगी होते थे, वे सच्चे तथा जो मोक्षमार्गोपयोगी नही थे, वे झूठे कहे जाते थे । लौकिक दृष्टि से गतप्रतिशत सत्यज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी नही है तो वह झूठा और लौकिक दृष्टि मे मिथ्या ज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी है तो वह सच्चा । इस तरह सत्यता और असत्यता की कसौटी बाह्यपदार्थो के ग्राधीन न होकर उसको मोक्षमार्गोपयोगिता के अधीन थी । इसीलिए सम्यकदृष्टि के सभी ज्ञान सच्चे और मिथ्यादृष्टि के सभी ज्ञान झूठं कहलाते थे । वैशेषिक सूत्र मे विद्या और अविद्या शब्द के प्रयोग कुछ इसी भूमिका पर है ।
इन पाँच ज्ञानो का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभाजन श्रागमकाल मे एक विभिन्न आधार पर ही था । वह श्रावार था आत्ममात्रसापेक्षत्व । अर्थात् जो ज्ञान ग्रात्ममात्र सापेक्ष था वह प्रत्यक्ष तथा जिनमे इन्द्रिय और मन की हायता अपेक्षित होती थी वे परोक्ष । लोक में जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानो को प्रत्यक्ष कहते थे, वे ज्ञान प्रागमिक परपरा मे परोक्ष थे । यागमो में प्रमाण नय निक्षेप आदि साधन बताए तो गए हैं, पर उनकी विभाजक रेखाएं इस काल में उतनी स्पष्ट नही थी, जितनी कि श्रागे जाकर हुई ।
कुन्दकुन्द और उमास्वाति - - उमास्वाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' श्रौर कुन्दकुन्द के 'प्रवचनसार' में 'स्थानागसूत्र' (२।११७१) को तरह ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष विभाग स्पष्ट है । इनके युग में ज्ञान की सत्यासत्यता का आधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी-की-तंसी चालू रही । कुन्दकुन्द के 'प्रवचनसार' और 'पचास्तिकाय' ग्रंथ तर्कगर्भ श्रागमिक शैली के सुन्दर नमूने है । इनके युग की भी उत्तरावधि चौथी शताब्दी तक मानी जा सकती है ।
समन्तभद्र - सिद्धसेन -- जब बौद्धदर्शन में नागार्जुन, वसुबन्धु, श्रसग तथा वौद्धन्याय के पिता दिडनाग का युग श्रा गया और दर्शनशा स्त्रियो में वौद्धदार्शनिको के प्रवल तर्क-पहारो से वैचैनी पैदा हो रही थी, वह एक तरह से दर्श के तार्किक श्रम या परपक्षखडन श्रश का प्रारंभकाल था । उस समय जैनपरम्परा में सिद्धसेन दिवाकर और स्वामी समन्तभद्र का उदय हुआ । इनके सामने आगमिक परिभाषाश्रो और शब्दो को तर्कशास्त्र के चौखटे में बैठाने का महत्त्वपूर्ण कार्य था । इस युग मे जो धर्म सस्था प्रतिवादियो के आक्षेपो का निराकरण कर स्वदर्शन प्रभावना नही कर सकती थी उसका अस्तित्व ही खतरे में था । अत परचक्र से रक्षा के लिए अपना दुर्ग स्वत सवृत करने के महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ इन दो आचार्यों ने किया ।
दिङ्नाग ने बौद्वन्याय में प्रवेश पाने के लिए 'न्यायप्रवेश' ग्रथ तथा 'प्रमाणसमुच्चय' आदि प्रकरणो की रचना को । सिद्धसेन दिवाकर ने जैनंन्याय का अवतार स्वरूप 'न्यायावतार' ग्रय तथा 'सन्मतितर्क' और 'द्वात्रिंशत्द्वात्रिगतिका' की रचना की । इन्होने 'न्यायावतार' में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद करके परोक्ष का वर्णन अनुमान और आगम इन दो विभागो मे किया । अर्थात् इनके मत से साख्य परम्परा की तरह प्रत्यक्ष, अनुमान और
१] त० सू० ५१३०
" त० सू० ५१३२
'त० सू० ५३३८
त० सू० ११६ ४२