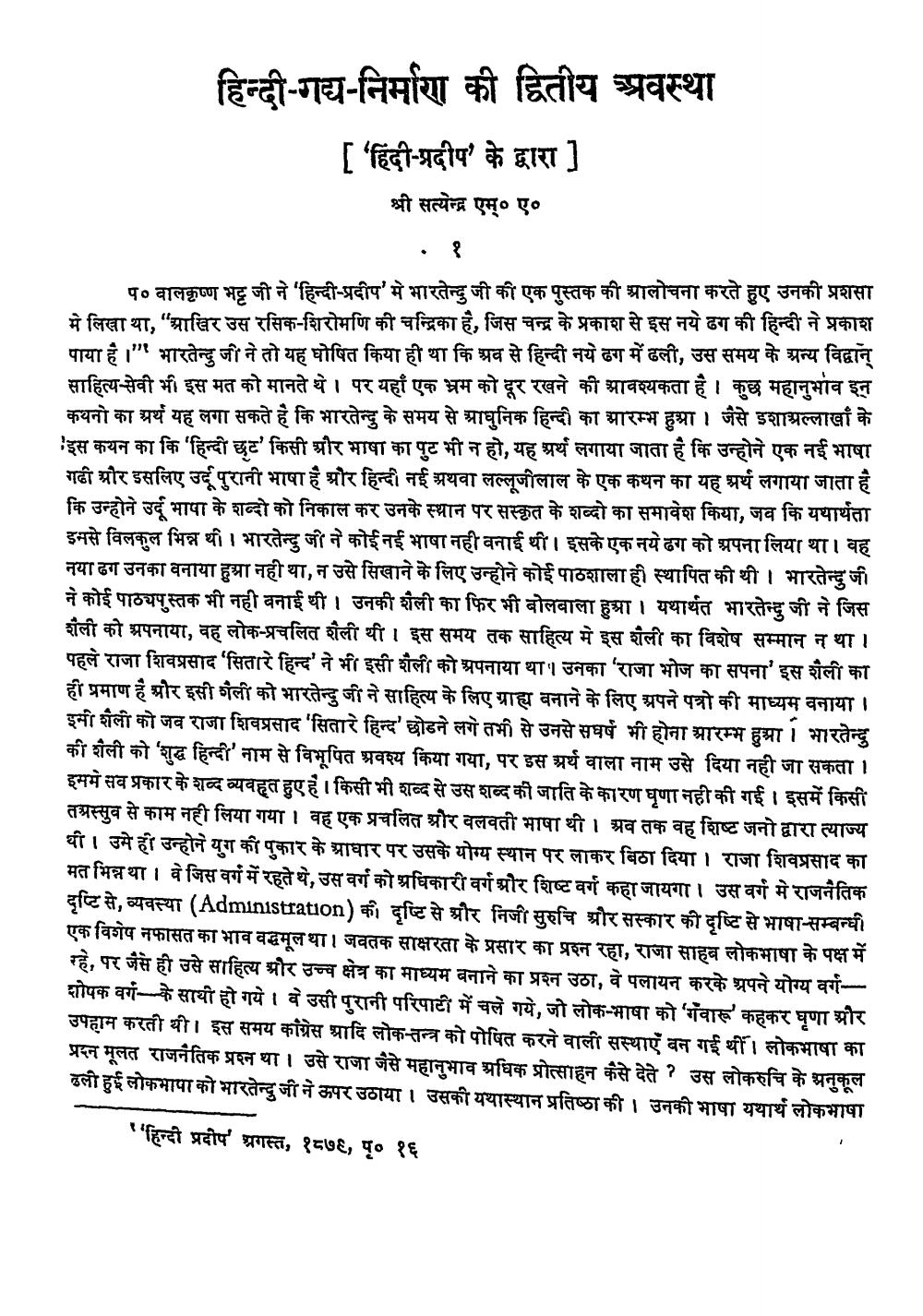________________
हिन्दी-गद्य-निर्माण की द्वितीय अवस्था
[ 'हिंदी-प्रदीप' के द्वारा]
श्री सत्येन्द्र एम० ए०
प० बालकृष्ण भट्ट जी ने 'हिन्दी-प्रदीप' मे भारतेन्दु जी की एक पुस्तक की आलोचना करते हुए उनकी प्रशसा मे लिखा था, "आखिर उस रसिक-शिरोमणि की चन्द्रिका है, जिस चन्द्र के प्रकाश से इस नये ढग की हिन्दी ने प्रकाश पाया है। भारतेन्दु जी ने तो यह घोषित किया ही था कि अव से हिन्दी नये ढग में ढली, उस समय के अन्य विद्वान् साहित्य-सेवी भी इस मत को मानते थे। पर यहाँ एक भ्रम को दूर रखने की आवश्यकता है। कुछ महानुभाव इन कथनो का अर्थ यह लगा सकते है कि भारतेन्दु के समय से आधुनिक हिन्दी का आरम्भ हुआ। जैसे इशाअल्लाखाँ के इस कथन का कि 'हिन्दी छुट' किसी और भाषा का पुट भी न हो, यह अर्थ लगाया जाता है कि उन्होने एक नई भाषा गढी और इसलिए उर्दू पुरानी भाषा है और हिन्दी नई अथवा लल्लूजीलाल के एक कथन का यह अर्थ लगाया जाता है कि उन्होने उर्दू भाषा के शब्दो को निकाल कर उनके स्थान पर सस्कृत के शब्दो का समावेश किया, जव कि यथार्थता इनसे विलकुल भिन्न थी। भारतेन्दु जी ने कोई नई भाषा नही बनाई थी। इसके एक नये ढग को अपना लिया था। वह नया ढग उनका बनाया हुआ नही था, न उसे सिखाने के लिए उन्होने कोई पाठशालाही स्थापित की थी। भारतेन्दुजी ने कोई पाठ्यपुस्तक भी नहीं बनाई थी। उनकी शैली का फिर भी बोलबाला हुआ। यथार्थत भारतेन्दु जी ने जिस शैली को अपनाया, वह लोक-प्रचलित शैली थी। इस समय तक साहित्य मे इस शैली का विशेष सम्मान न था। पहले राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी इसी शैली को अपनाया था। उनका 'राजा भोज का सपना' इस शैली का ही प्रमाण है और इसी शैली को भारतेन्दु जी ने साहित्य के लिए ग्राह्य बनाने के लिए अपने पत्रो की माध्यम बनाया। इमी शैली को जव राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द' छोडने लगे तभी से उनसे सघर्ष भी होना प्रारम्भ हुआ। भारतेन्दु की शैली को 'शुद्ध हिन्दी' नाम से विभूपित अवश्य किया गया, पर इस अर्थ वाला नाम उसे दिया नही जा सकता। इममे सब प्रकार के शब्द व्यवहृत हुए है । किसी भी शब्द से उस शब्द की जाति के कारण घृणा नही की गई। इसमें किसी तअस्सुव से काम नहीं लिया गया। वह एक प्रचलित और वलवती भाषा थी। अब तक वह शिष्ट जनो द्वारा त्याज्य थी। उमे ही उन्होने युग की पुकार के आधार पर उसके योग्य स्थान पर लाकर बिठा दिया। राजा शिवप्रसाद का मत भिन्नथा। वे जिस वर्ग में रहते थे, उस वर्ग को अधिकारी वर्ग और शिष्ट वर्ग कहा जायगा। उस वर्ग मे राजनैतिक दृष्टि से, व्यवस्था (Administration) की दृष्टि से और निजी सुरुचि और सस्कार की दृष्टि से भाषा-सम्बन्धी एक विशेष नफासत का भाव वद्धमूल था। जबतक साक्षरता के प्रसार का प्रश्न रहा, राजा साहब लोकभाषा के पक्ष में रहे, पर जैसे ही उसे साहित्य और उच्च क्षेत्र का माध्यम बनाने का प्रश्न उठा, वे पलायन करके अपने योग्य वर्गशोषक वर्ग के साथी हो गये। वे उसी पुरानी परिपाटी में चले गये, जो लोक-भाषा को 'गवारूकहकर घृणा और उपहाम करती थी। इस समय कांग्रेस आदि लोक-तन्त्र को पोषित करने वाली सस्थाएँ बन गई थीं। लोकभाषा का प्रदन मूलत राजनैतिक प्रश्न था । उसे राजा जैसे महानुभाव अधिक प्रोत्साहन कैसे देते ? उस लोकरुचि के अनुकूल ढली हुई लोकभाषा को भारतेन्दु जी ने ऊपर उठाया। उसकी यथास्थान प्रतिष्ठा की। उनकी भाषा यथार्थ लोकभाषा
"हिन्दी प्रदीप अगस्त, १८७६, पृ० १६