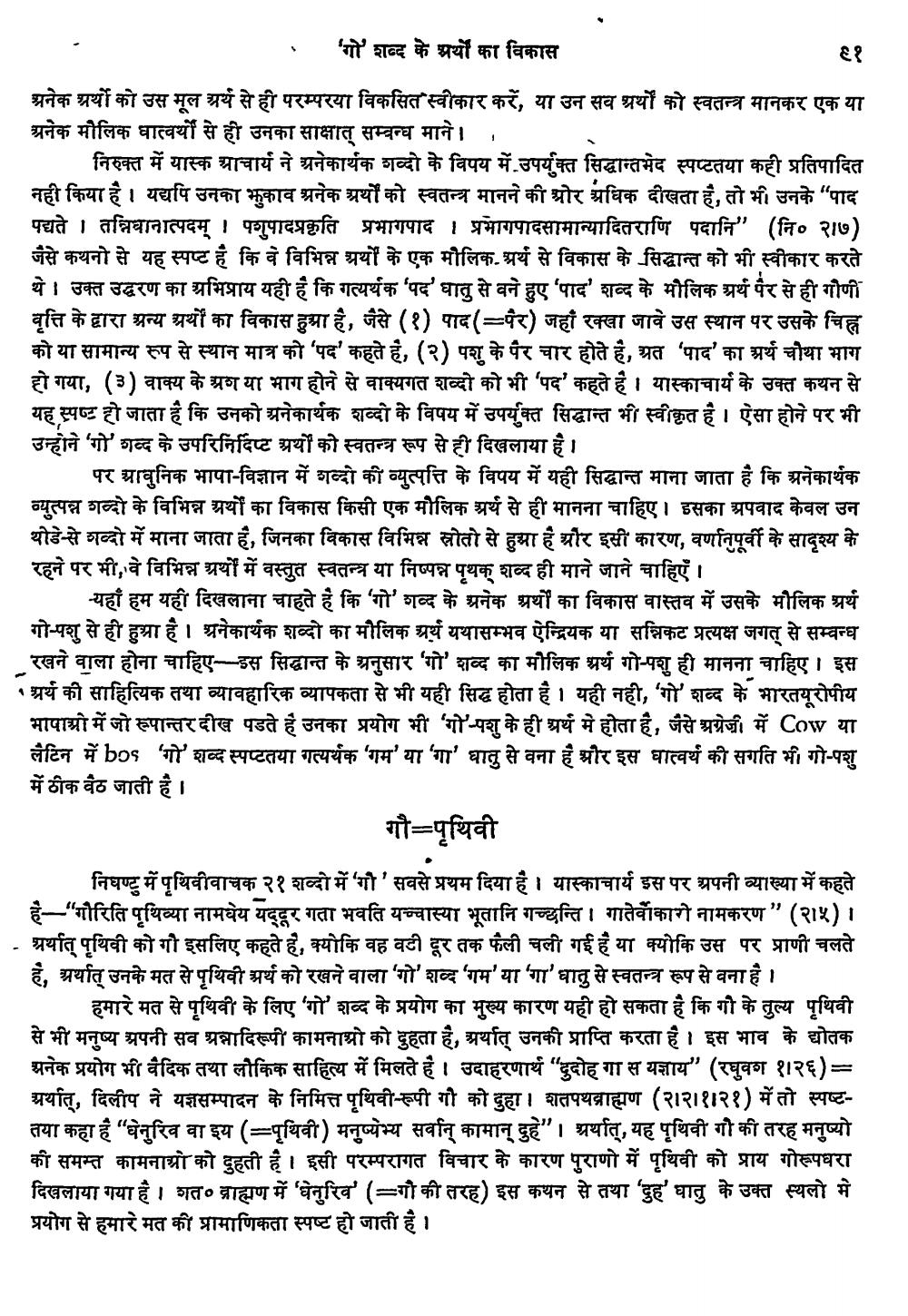________________
' 'गों शब्द के अर्थों का विकास अनेक अर्थो को उस मूल अर्थ से ही परम्परया विकसित स्वीकार करें, या उन सव अर्थों को स्वतन्त्र मानकर एक या अनेक मौलिक धात्वर्थों से ही उनका साक्षात् सम्बन्ध माने। ।
निरुक्त में यास्क प्राचार्य ने अनेकार्थक शब्दो के विपय में उपर्युक्त सिद्धान्तभेद स्पष्टतया कही प्रतिपादित नही किया है । यद्यपि उनका झुकाव अनेक अर्थों को स्वतन्त्र मानने की ओर अधिक दीखता है, तो भी उनके “पाद पद्यते । तनिधानात्पदम् । पशुपादप्रकृति प्रभागपाद । प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि" (नि० २१७) जैसे कथनो से यह स्पष्ट है कि वे विभिन्न अर्थों के एक मौलिक.अर्थ से विकास के सिद्धान्त को भी स्वीकार करते थे। उक्त उद्धरण का अभिप्राय यही है कि गत्यर्थक 'पद' घातु से बने हुए ‘पाद' शब्द के मौलिक अर्थ पर से ही गौणी वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थों का विकास हुआ है, जैसे (१) पाद(पर) जहाँ रक्खा जावे उस स्थान पर उसके चिह्न को या सामान्य रूप से स्थान मात्र को 'पद' कहते है, (२) पशु के पैर चार होते है, अत 'पाद' का अर्थ चौथा भाग हो गया, (३) वाक्य के अग या भाग होने से वाक्यगत शब्दो को भी 'पद' कहते है । यास्काचार्य के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको अनेकार्थक शब्दो के विषय में उपर्युक्त सिद्धान्त भी स्वीकृत है। ऐसा होने पर भी उन्होने 'गो' शब्द के उपरिनिर्दिष्ट अर्थों को स्वतन्त्र रूप से ही दिखलाया है।
पर आधुनिक भापा-विज्ञान में शब्दो की व्युत्पत्ति के विषय में यही सिद्धान्त माना जाता है कि अनेकार्थक व्युत्पन्न शब्दो के विभिन्न अर्थों का विकास किसी एक मौलिक अर्थ से ही मानना चाहिए। इसका अपवाद केवल उन थोडे-से शब्दो में माना जाता है, जिनका विकास विभिन्न स्रोतो से हुआ है और इसी कारण, वर्णानुपूर्वी के सादृश्य के रहने पर भी, वे विभिन्न अर्थों में वस्तुत स्वतन्त्र या निष्पन्न पृथक् शब्द ही माने जाने चाहिएँ।।
___यहाँ हम यही दिखलाना चाहते है कि 'गो' शब्द के अनेक अर्थों का विकास वास्तव में उसके मौलिक अर्थ गो-पशु से ही हुआ है । अनेकार्थक शब्दो का मौलिक अर्थ यथासम्भव ऐन्द्रियक या सन्निकट प्रत्यक्ष जगत् से सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिए-इस सिद्धान्त के अनुसार 'गो' शब्द का मौलिक अर्थ गो-पशु ही मानना चाहिए। इस • अर्थ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक व्यापकता से भी यही सिद्ध होता है। यही नही, 'गो' शब्द के भारतयूरोपीय भाषाओं में जो रूपान्तर दीख पडते है उनका प्रयोग भी 'गों पशु के ही अर्थ मे होता है, जैसे अग्रेजी में Cow या लैटिन में bos 'गो' शब्द स्पप्टतया गत्यर्थक 'गम' या 'गा' धातु से बना है और इस धात्वर्थ की सगति भी गो-पशु में ठीक वैठ जाती है।
गौ=पृथिवी निघण्टु में पृथिवीवाचक २१ शब्दो में 'गो' सवसे प्रथम दिया है। यास्काचार्य इस पर अपनी व्याख्या में कहते है-"गौरिति पृथिव्या नामय यदुर गता भवति यच्चास्या भूतानि गच्छन्ति । गातेवाकारो नामकरण" (२१५) । - अर्थात् पृथिवी को गौ इसलिए कहते है, क्योकि वह वढी दूर तक फैली चली गई है या क्योकि उस पर प्राणी चलते है, अर्थात् उनके मत से पृथिवी अर्थ को रखने वाला 'गो' शब्द 'गम' या 'गा' धातु से स्वतन्त्र रूप से बना है।
हमारे मत से पृथिवी के लिए 'गों' शब्द के प्रयोग का मुख्य कारण यही हो सकता है कि गौ के तुल्य पृथिवी से भी मनुष्य अपनी सव अन्नादिरूपी कामनाओ को दुहता है, अर्थात् उनकी प्राप्ति करता है। इस भाव के द्योतक अनेक प्रयोग भी वैदिक तथा लौकिक साहित्य में मिलते है । उदाहरणार्थ "दुदोह गा स यज्ञाय" (रघुवग श२६)= अर्थात्, दिलीप ने यज्ञसम्पादन के निमित्त पृथिवी-रूपी गौ को दुहा। शतपथब्राह्मण (२२२।१२१) में तो स्पष्टतया कहा है “धनुरिव वा इय (=पृथिवी) मनुष्येभ्य सर्वान् कामान् दुहे"। अर्थात्, यह पृथिवी गौ की तरह मनुष्यो की समस्त कामनायो को दुहती है। इसी परम्परागत विचार के कारण पुराणो में पृथिवी को प्राय गोरूपधरा दिखलाया गया है। शत० ब्राह्मण में 'धेनुरिव' (=गौ की तरह) इस कथन से तथा 'दुह' धातु के उक्त स्थलो मे प्रयोग से हमारे मत की प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाती है।