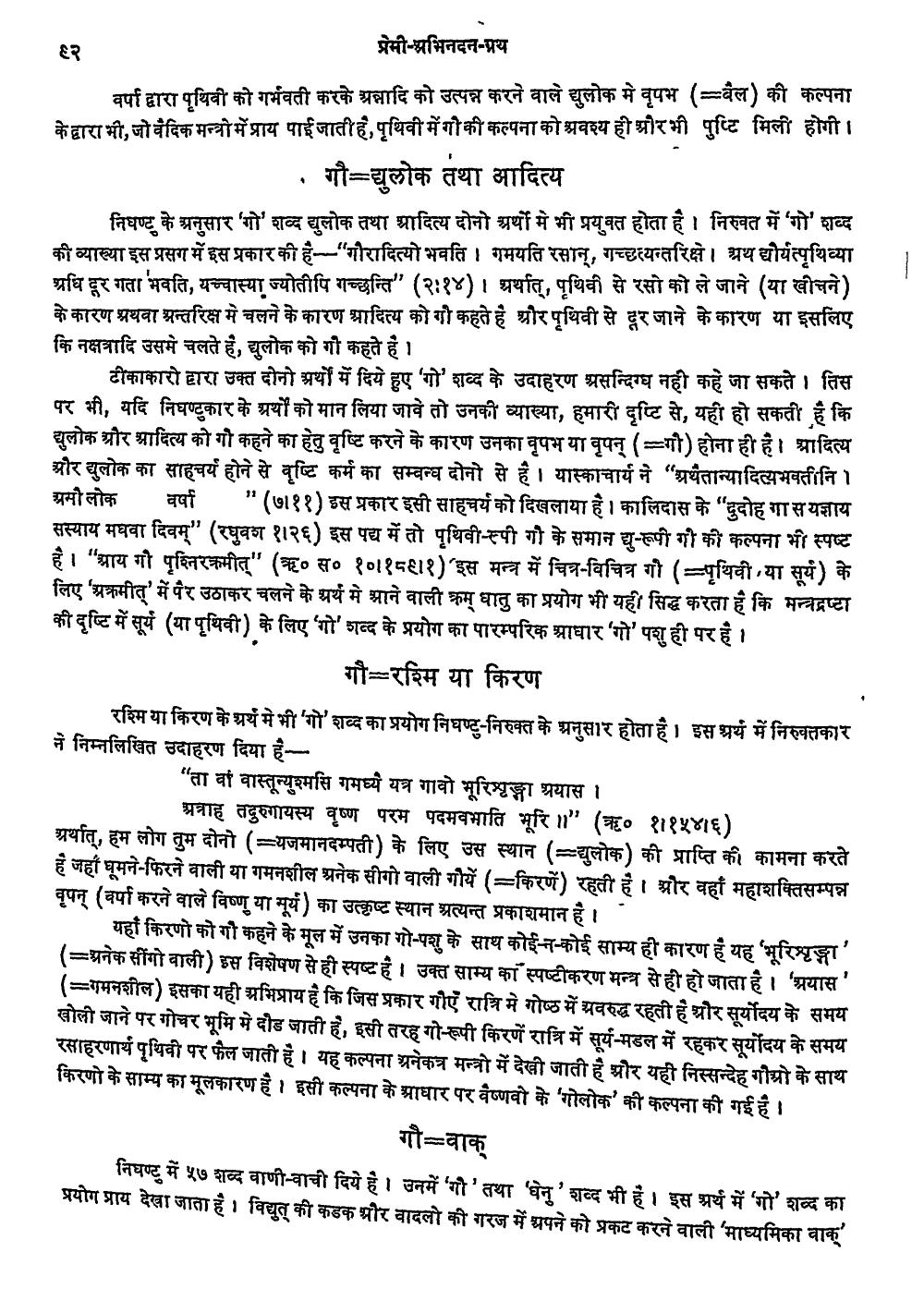________________
प्रेमी-प्रभिनदन- प्रथ
वर्षा द्वारा पृथिवी को गर्भवती करके अन्नादि को उत्पन्न करने वाले द्युलोक मे वृपभ (बैल) की कल्पना के द्वारा भी, जो वैदिक मन्त्रो में प्राय पाई जाती है, पृथिवी में गो की कल्पना को अवश्य ही और भी पुष्टि मिली होगी ।
गौ= द्युलोक तथा आदित्य
1
निघण्ट के अनुसार 'गो' शव्द द्युलोक तथा श्रादित्य दोनो अर्थो मे भी प्रयुक्त होता है । निरुक्त में 'गो' शब्द की व्याख्या इस प्रसग में इस प्रकार की है - "गौरादित्यो भवति । गमयति रसान्, गच्छत्यन्तरिक्षे । श्रथ द्यौर्यत्पृथिव्या श्रधि दूर गता भवति, यच्चास्या ज्योतीपि गच्छन्ति” (२:१४) । श्रर्थात् पृथिवी से रसो को ले जाने (या खीचने) के कारण अथवा अन्तरिक्ष में चलने के कारण श्रादित्य को गो कहते है और पृथिवी से दूर जाने के कारण या इसलिए कि नक्षत्रादि उसमे चलते हैं, द्युलोक को गो कहते हैं ।
टीकाकारो द्वारा उक्त दोनो अर्थों में दिये हुए 'गो' शब्द के उदाहरण असन्दिग्घ नही कहे जा सकते । तिस पर भी, यदि निघण्टुकार के प्रर्थों को मान लिया जावे तो उनकी व्याख्या, हमारी दृष्टि से, यही हो सकती है कि द्युलोक और आदित्य को गो कहने का हेतु वृष्टि करने के कारण उनका वृपभ या वृपन् (गो) होना ही है। श्रादित्य और द्युलोक का साहचर्य होने से वृष्टि कर्म का सम्वन्ध दोनो से है । यास्काचार्य ने “ श्रथैतान्यादित्यभवतीनि । श्रमौ लोक वर्षा (७११) इस प्रकार इसी साहचर्य को दिखलाया है। कालिदास के "दुदोह गास यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्” (रघुवग १।२६ ) इस पद्य में तो पृथिवी-स्पी गौ के समान द्यु-रूपी गौ को कल्पना भी स्पष्ट है । "आय गौ पृश्निरक्रमीत्" (ऋ० स० १० १८९१ ) इस मन्त्र में चित्र-विचित्र गो (पृथिवी/ या सूर्य) के लिए 'अक्रमीत्' में पैर उठाकर चलने के अर्थ मे आने वाली क्रम् धातु का प्रयोग भी यही सिद्ध करता है कि मन्त्रद्रष्टा की दृष्टि में सूर्य (या पृथिवी) के लिए 'गो' शब्द के प्रयोग का पारम्परिक श्राधार 'गो' पशु ही पर है ।
गौ- रश्मि या किरण
६२
31
•
रश्मि या किरण के अर्थं मे भी 'गो' शब्द का प्रयोग निघण्टु-निरुक्त के अनुसार होता है । इस अर्थ में निरुवतकार ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है-
"ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा प्रयास ।
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण परम पदमवभाति भूरि ||" (ऋ० १११५४६) अर्थात्, हम लोग तुम दोनो (यजमानदम्पती ) के लिए उस स्थान ( = द्युलोक ) की प्राप्ति की कामना करते है जहाँ घूमने-फिरने वाली या गमनशील अनेक सीगो वाली गौयें (= किरणें ) रहती है । और वहाँ महाशक्तिसम्पन्न वृपन् (वर्षा करने वाले विष्णु या सूर्य ) का उत्कृष्ट स्थान अत्यन्त प्रकाशमान है ।
यहाँ किरणो को गौ कहने के मूल में उनका गो-पशु के साथ कोई-न-कोई साम्य ही कारण है यह 'भूरिशृङ्गा' ( अनेक सींगो वाली) इस विशेषण से ही स्पष्ट है । उक्त साम्य का स्पष्टीकरण मन्त्र से ही हो जाता है । 'प्रयास' ( = गमनशील) इसका यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार गौएँ रात्रि में गोष्ठ में अवरुद्ध रहती है और सूर्योदय के समय खोली जाने पर गोचर भूमि मे दौड जाती है, इसी तरह गो-रूपी किरणें रात्रि में सूर्य - मंडल में रहकर सूर्योदय के समय रसाहरणार्थं पृथिवी पर फैल जाती है । यह कल्पना अनेकत्र मन्त्रो में देखी जाती है और यही निस्सन्देह गौत्रो के साथ किरणो के साम्य का मूलकारण है । इसी कल्पना के आधार पर वैष्णवो के 'गोलोक' की कल्पना की गई है ।
गौ=वाक्
निघण्टु में ५७ शब्द वाणी-वाची दिये है । उनमें 'गो' तथा 'घेनु' शब्द भी हैं। इस अर्थ में 'गो' शब्द का प्रयोग प्राय देखा जाता है । विद्युत् की कडक और वादलो की गरज में अपने को प्रकट करने वाली 'माध्यमिका वाक्