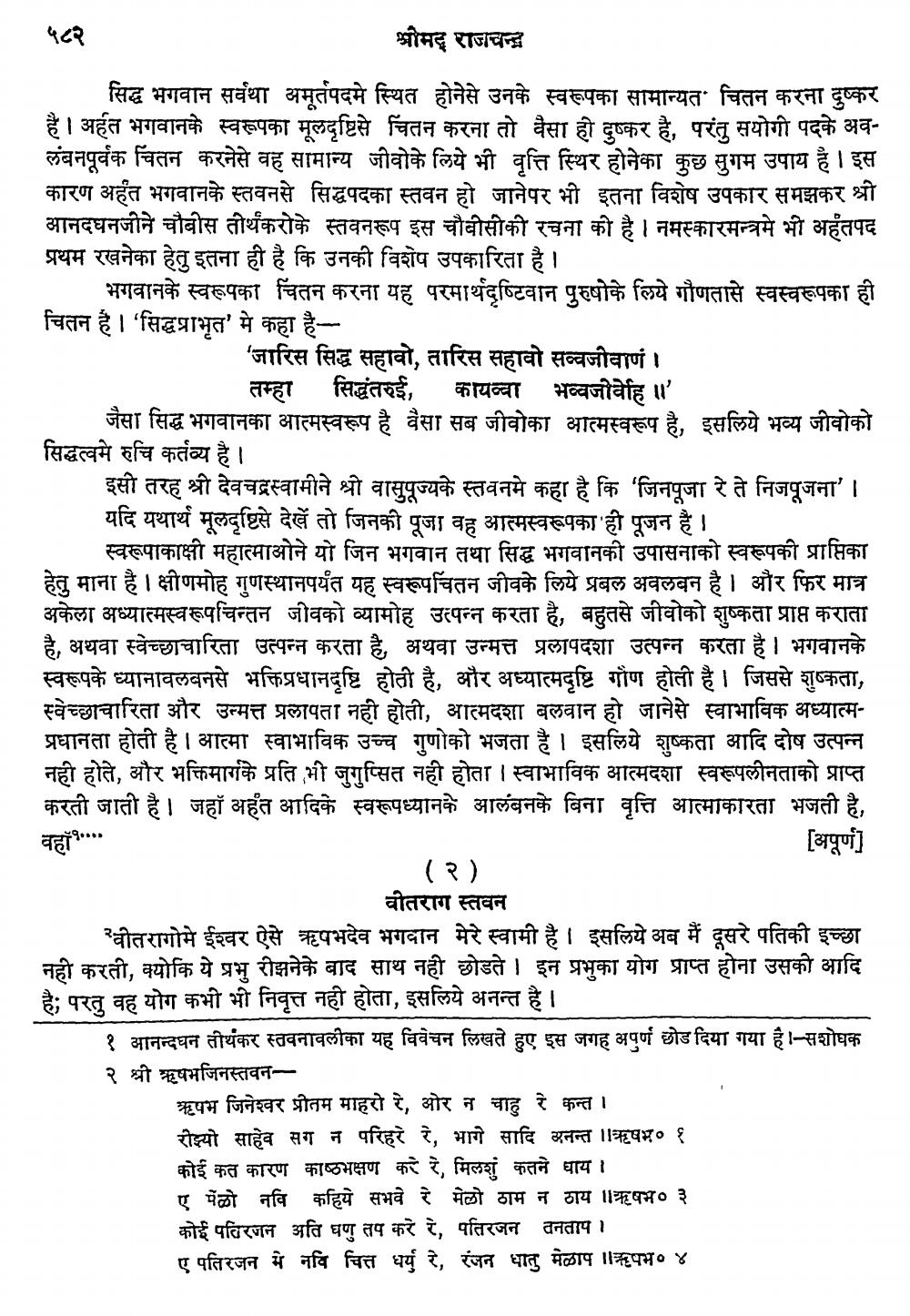________________
५८२
श्रीमद् राजचन्द्र सिद्ध भगवान सर्वथा अमूर्तपदमे स्थित होनेसे उनके स्वरूपका सामान्यतः चितन करना दुष्कर है । अर्हत भगवानके स्वरूपका मूलदृष्टिसे चिंतन करना तो वैसा ही दुष्कर है, परंतु सयोगी पदके अवलंबनपूर्वक चिंतन करनेसे वह सामान्य जीवोके लिये भी वृत्ति स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय है । इस कारण अहंत भगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझकर श्री आनदधनजीने चौबीस तीर्थंकरोके स्तवनरूप इस चौबीसीकी रचना की है । नमस्कारमन्त्रमे भी अहंतपद प्रथम रखनेका हेतु इतना ही है कि उनकी विशेष उपकारिता है।
भगवानके स्वरूपका चिंतन करना यह परमार्थदृष्टिवान पुरुषोके लिये गौणतासे स्वस्वरूपका ही चितन है । 'सिद्धप्राभृत' मे कहा है
'जारिस सिद्ध सहावो, तारिस सहावो सव्वजीवाणं ।
तम्हा सिद्धंतरई, कायव्वा भव्वजोहि ॥' जैसा सिद्ध भगवानका आत्मस्वरूप है वैसा सब जीवोका आत्मस्वरूप है, इसलिये भव्य जीवोको सिद्धत्वमे रुचि कर्तव्य है।।
इसी तरह श्री देवचद्रस्वामीने श्री वासुपूज्यके स्तवनमे कहा है कि 'जिनपूजा रे ते निजपूजना' । यदि यथार्थ मूलदृष्टिसे देखें तो जिनकी पूजा वह आत्मस्वरूपका ही पूजन है ।
स्वरूपाकाक्षी महात्माओने यो जिन भगवान तथा सिद्ध भगवानकी उपासनाको स्वरूपकी प्राप्तिका हेतु माना है । क्षीणमोह गुणस्थानपर्यंत यह स्वरूपचिंतन जीवके लिये प्रबल अवलबन है। और फिर मात्र अकेला अध्यात्मस्वरूपचिन्तन जीवको व्यामोह उत्पन्न करता है, बहुतसे जीवोको शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्वेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रलापदशा उत्पन्न करता है। भगवानके स्वरूपके ध्यानावलवनसे भक्तिप्रधानदृष्टि होती है, और अध्यात्मदृष्टि गौण होती है। जिससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त प्रलापता नही होती, आत्मदशा बलवान हो जानेसे स्वाभाविक अध्यात्मप्रधानता होती है । आत्मा स्वाभाविक उच्च गुणोको भजता है। इसलिये शुष्कता आदि दोष उत्पन्न नही होते, और भक्तिमार्गके प्रति भी जुगुप्सित नही होता । स्वाभाविक आत्मदशा स्वरूपलीनताको प्राप्त करती जाती है। जहाँ अहंत आदिके स्वरूपध्यानके आलंबनके बिना वृत्ति आत्माकारता भजती है,
[अपूर्ण (२)
वीतराग स्तवन वीतरागोमे ईश्वर ऐसे ऋषभदेव भगवान मेरे स्वामी है। इसलिये अब मैं दूसरे पतिकी इच्छा नही करती, क्योकि ये प्रभु रीझनेके बाद साथ नही छोडते । इन प्रभुका योग प्राप्त होना उसको आदि है; परतु वह योग कभी भी निवृत्त नही होता, इसलिये अनन्त है।
१ आनन्दघन तीर्थकर स्तवनावलीका यह विवेचन लिखते हुए इस जगह अपुर्ण छोड दिया गया है। सशोधक २ श्री ऋषभजिनस्तवन
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहु रे कन्त । रीझ्यो साहेव सग न परिहरे रे, भागे सादि अनन्त ||ऋषभ० १ कोई कत कारण काष्ठभक्षण करे रे, मिलशं कतने धाय । ए मेळो नवि कहिये सभवे रे मेळो ठाम न ठाय |ऋषभ० ३ कोई पविरजन अति घणु तप करे रे, पतिरजन तनताप । ए पतिरजन मे नवि चित्त धर्य रे, रंजन धातु मेळाप ॥ऋषभ० ४
वहाँ..."