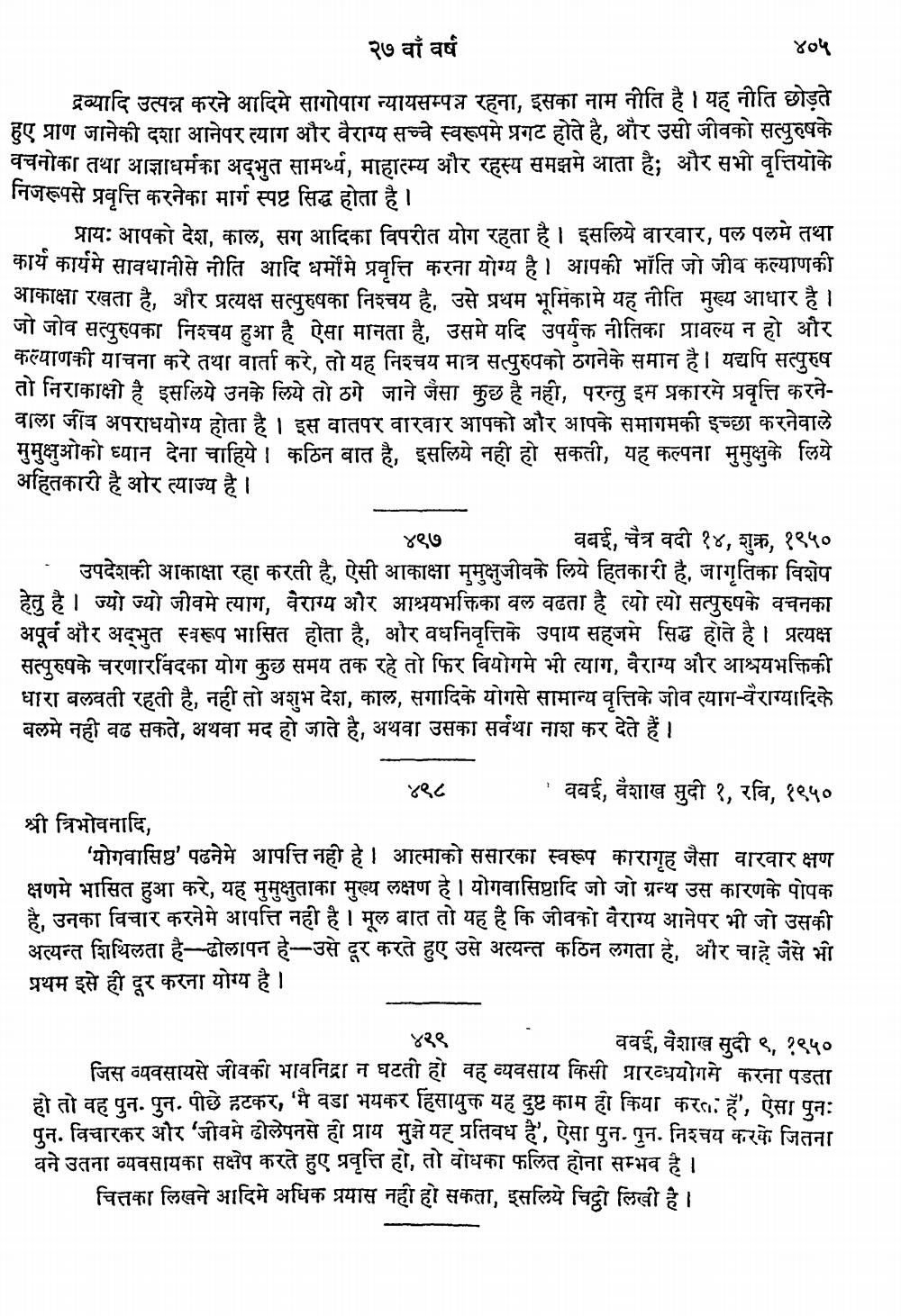________________
२७ वाँ वर्ष
४०५ द्रव्यादि उत्पन्न करने आदिमे सागोपाग न्यायसम्पन्न रहना, इसका नाम नीति है । यह नीति छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग और वैराग्य सच्चे स्वरूपमे प्रगट होते है, और उसी जीवको सत्पुरुषके वचनोका तथा आज्ञाधर्मका अद्भुत सामर्थ्य, माहात्म्य और रहस्य समझमे आता है; और सभी वृत्तियोके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है।
प्रायः आपको देश, काल, सग आदिका विपरीत योग रहता है। इसलिये वारवार, पल पलमे तथा काय कार्यमे सावधानीसे नीति आदि धर्मो मे प्रवृत्ति करना योग्य है। आपकी भॉति जो जीव कल्याणकी आकाक्षा रखता है, और प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामे यह नीति मुख्य आधार है। जो जोव सत्पुरुषका निश्चय हुआ है ऐसा मानता है, उसमे यदि उपर्युक्त नीतिका प्रावल्य न हो और कल्याणकी याचना करे तथा वार्ता करे, तो यह निश्चय मात्र सत्पुरुपको ठगनेके समान है। यद्यपि सत्पुरुष तो निराकाक्षी है इसलिये उनके लिये तो ठगे जाने जैसा कुछ है नही, परन्तु इस प्रकारमे प्रवृत्ति करनेवाला जीव अपराधयोग्य होता है। इस बातपर वारवार आपको और आपके समागमकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओको ध्यान देना चाहिये। कठिन बात है, इसलिये नही हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुके लिये अहितकारी है ओर त्याज्य है।
४९७
बबई, चैत्र वदी १४, शुक्र, १९५० - उपदेशकी आकाक्षा रहा करती है, ऐसी आकाक्षा मुमुक्षुजीवके लिये हितकारी है, जागृतिका विशेप हेतु है। ज्यो ज्यो जीवमे त्याग, वैराग्य और आश्रयभक्तिका बल बढता है त्यो त्यो सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भासित होता है, और वधनिवृत्तिके उपाय सहजमे सिद्ध होते है। प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका योग कुछ समय तक रहे तो फिर वियोगमे भी त्याग, वैराग्य और आश्रयभक्तिकी धारा बलवती रहती है, नही तो अशुभ देश, काल, सगादिके योगसे सामान्य वृत्तिके जीव त्याग-वैराग्यादिके बलमे नही बढ सकते, अथवा मद हो जाते है, अथवा उसका सर्वथा नाश कर देते हैं।
४९८
' ववई, वैशाख सुदी १, रवि, १९५० श्री त्रिभोवनादि,
'योगवासिष्ठ' पढनेमे आपत्ति नही हे । आत्माको ससारका स्वरूप कारागृह जैसा वारवार क्षण क्षणमे भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण हे । योगवासिष्ठादि जो जो ग्रन्थ उस कारणके पोपक है, उनका विचार करने मे आपत्ति नहीं है । मूल बात तो यह है कि जीवको वैराग्य आनेपर भी जो उसकी अत्यन्त शिथिलता है-ढोलापन हे-उसे दूर करते हुए उसे अत्यन्त कठिन लगता है, और चाहे जैसे भी प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है ।
ववई, वैशाख सुदी ९, १९५० जिस व्यवसायसे जीवको भावनिद्रा न घटती हो वह व्यवसाय किसी प्रारब्धयोगमे करना पड़ता हो तो वह पून. पुन. पीछे हटकर, 'मे बडा भयकर हिसायुक्त यह दुष्ट काम हो किया करत . ऐसा प. पून. विचारकर और 'जीवमे ढोलेपनसे ही प्राय मुझे यह प्रतिवध है', ऐसा पुन. पून. निश्चय करके जितना बने उतना व्यवसायका सक्षेप करते हुए प्रवृत्ति हो, तो वोधका फलित होना सम्भव है।
चित्तका लिखने आदिमे अधिक प्रयास नहीं हो सकता, इसलिये चिट्ठी लिखी है।