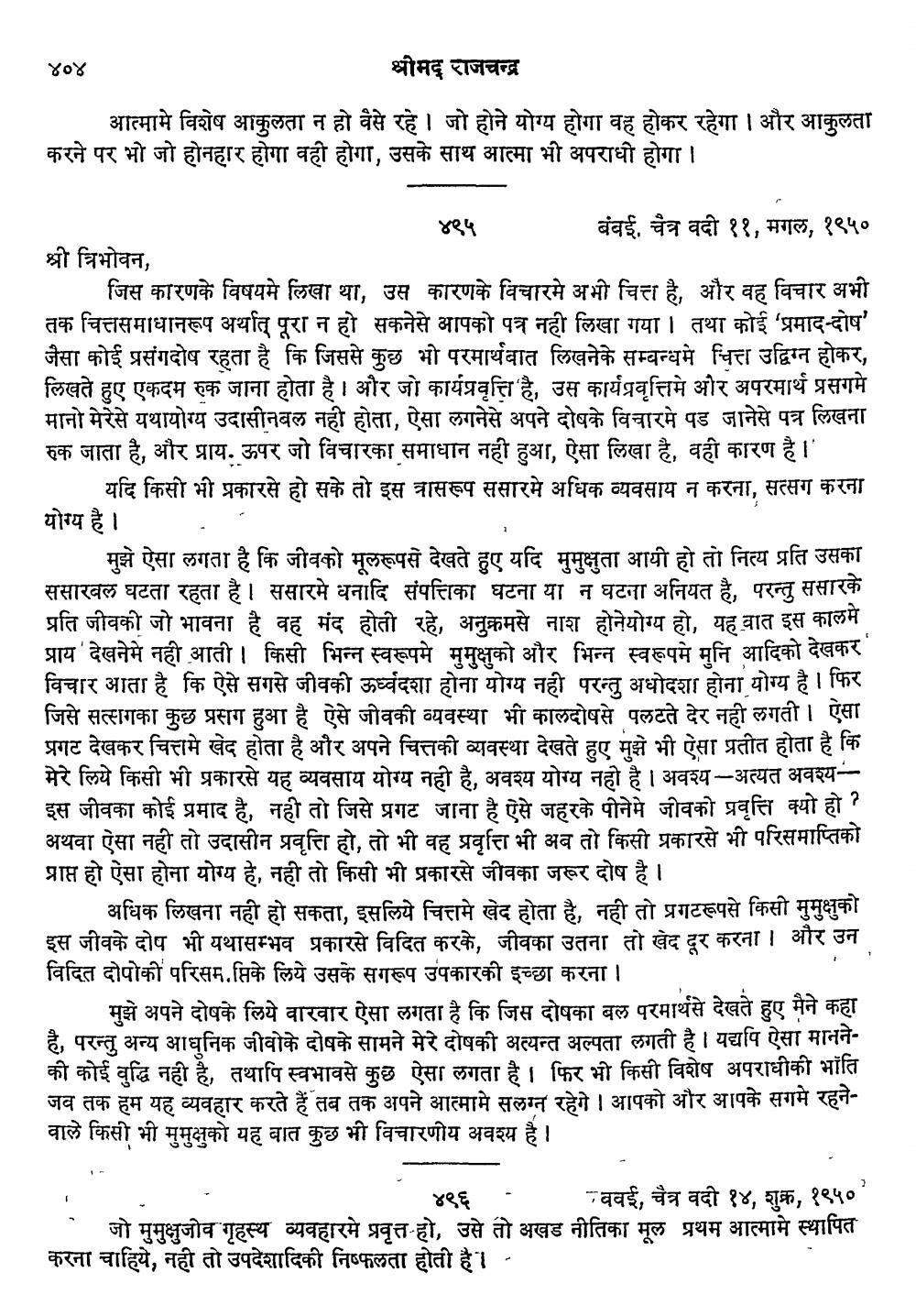________________
श्रीमद राजचन्द्र
आत्मा विशेष आकुलता न हो वैसे रहे । जो होने योग्य होगा वह होकर रहेगा । और आकुलता करने पर भी जो होनहार होगा वही होगा, उसके साथ आत्मा भी अपराधी होगा ।
४०४
बंबई, चैत्र वदी ११, मंगल, १९५०
श्री त्रिभोवन,
जिस कारणके विषयमे लिखा था, उस कारणके विचारमे अभी चित्त है, और वह विचार अभी तक चित्तसमाधानरूप अर्थात् पूरा न हो सकनेसे आपको पत्र नही लिखा गया । तथा कोई 'प्रमाद-दोष' जैसा कोई प्रसंगदोष रहता है कि जिससे कुछ भी परमार्थबात लिखनेके सम्बन्धमे चित्त उद्विग्न होकर, लिखते हुए एकदम रुक जाना होता है । और जो कार्यप्रवृत्ति है, उस कार्य प्रवृत्तिमे और अपरमार्थ प्रसगमे मानो मेरेसे यथायोग्य उदासीनबल नही होता, ऐसा लगनेसे अपने दोषके विचारमे पड जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है, और प्राय. ऊपर जो विचारका समाधान नही हुआ, ऐसा लिखा है, वही कारण है ।'
४९५
यदि किसी भी प्रकार से हो सके तो इस त्रासरूप ससारमे अधिक व्यवसाय न करना, सत्संग करना योग्य है ।
मुझे ऐसा लगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आयी हो तो नित्य प्रति उसका ससारवल घटता रहता है । ससारमे धनादि संपत्तिका घटना या न घटना अनियत है, परन्तु ससारके प्रति जीवकी जो भावना है वह मंद होती रहे, अनुक्रमसे नाश होनेयोग्य हो, यह बात इस कालमे प्राय' देखनेमे नही आती । किसी भिन्न स्वरूपमे मुमुक्षुको और भिन्न स्वरूपमे मुनि आदिको देखकर विचार आता है कि ऐसे सगसे जीवकी ऊर्ध्वदशा होना योग्य नही परन्तु अधोदशा होना योग्य है । फिर जिसे सत्सगका कुछ प्रसग हुआ है ऐसे जीवकी व्यवस्था भी कालदोषसे पलटते देर नही लगती । ऐसा प्रगट देखकर चित्तमे खेद होता है और अपने चित्तको व्यवस्था देखते हुए मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है मेरे लिये किसी भी प्रकारसे यह व्यवसाय योग्य नही है, अवश्य योग्य नही है । अवश्य - अत्यत अवश्यइस जीवका कोई प्रमाद है, नही तो जिसे प्रगट जाना है ऐसे जहरके पीनेमे जीवको प्रवृत्ति क्यो हो अथवा ऐसा नही तो उदासीन प्रवृत्ति हो, तो भी वह प्रवृत्ति भी अब तो किसी प्रकारसे भी परिसमाप्तिको प्राप्त हो ऐसा होना योग्य है, नही तो किसी भी प्रकारसे जीवका जरूर दोष है ।
?
अधिक लिखना नही हो सकता, इसलिये चित्तमे खेद होता है, नही तो प्रगटरूप से किसी मुमुक्षु इस जीवके दोष भी यथासम्भव प्रकारसे विदित करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना । और उन विदित दोपोकी परिसमाप्तिके लिये उसके सगरूप उपकारकी इच्छा करना ।
मुझे अपने दोषके लिये वारवार ऐसा लगता है कि जिस दोषका बल परमार्थसे देखते हुए मैने कहा है, परन्तु अन्य आधुनिक जीवोके दोषके सामने मेरे दोषकी अत्यन्त अल्पता लगती है । यद्यपि ऐसा माननेकी कोई बुद्धि नही है, तथापि स्वभावसे कुछ ऐसा लगता है । फिर भी किसी विशेष अपराधी की भाँति जब तक हम यह व्यवहार करते हैं तब तक अपने आत्मामे सलग्न रहेगे । आपको और आपके सगमे रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी विचारणीय अवश्य है ।
'
४९६
ववई, चैत्र वदी १४, शुक्र, १९५० जो मुमुक्षुजीव गृहस्थ व्यवहारमे प्रवृत्त हो, उसे तो अखड नीतिका मूल प्रथम आत्मामे स्थापित करना चाहिये, नही तो उपदेशादिकी निष्फलता होती है ।