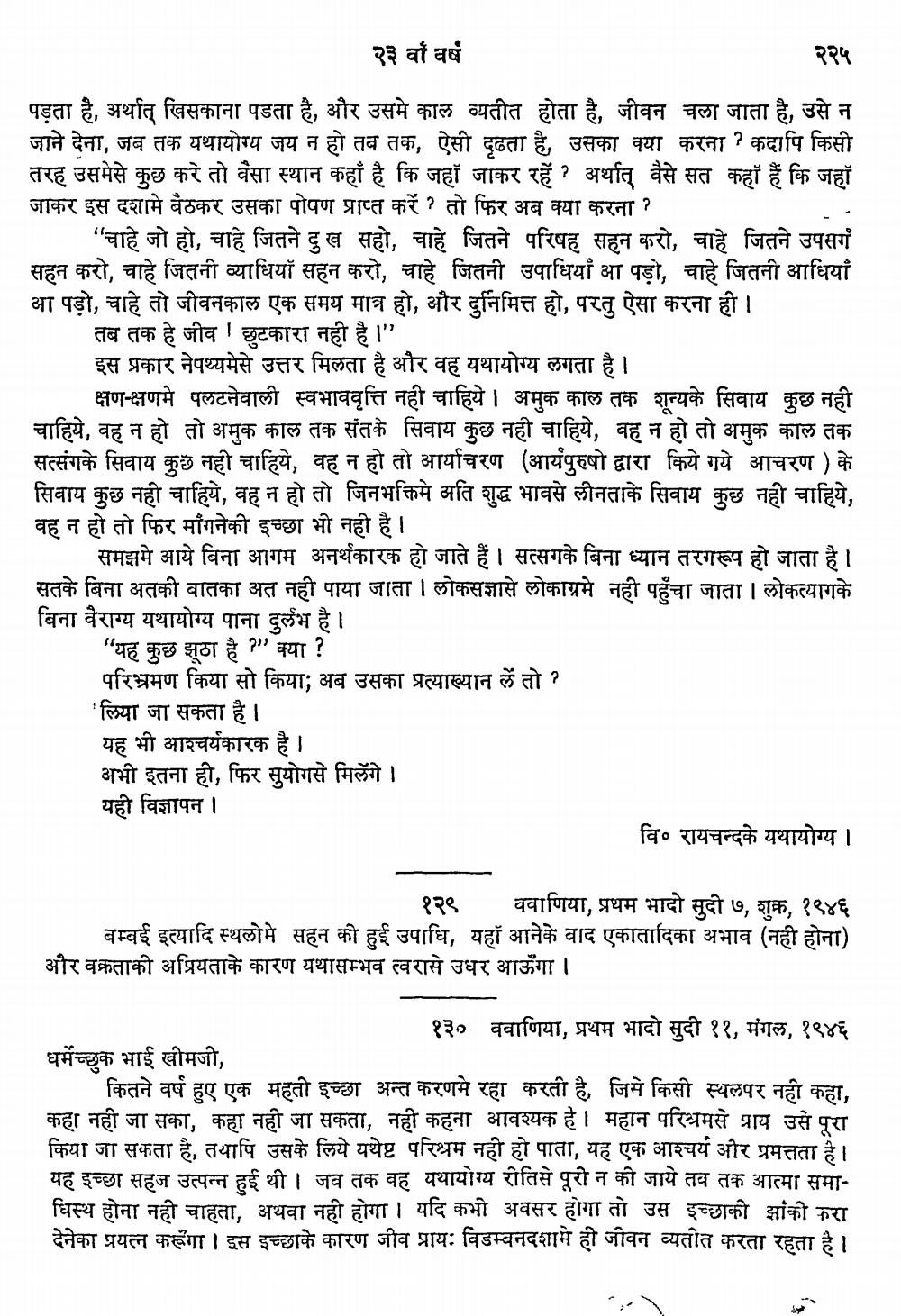________________
२३ व वर्ष
२२५
पड़ता है, अर्थात् खिसकाना पडता है, और उसमे काल व्यतीत होता है, जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना, जब तक यथायोग्य जय न हो तब तक, ऐसी दृढता है, उसका क्या करना ? कदापि किसी तरह उसमेसे कुछ करे तो वैसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहें ? अर्थात् वैसे सत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशामे बैठकर उसका पोपण प्राप्त करें ? तो फिर अब क्या करना ?
"चाहे जो हो, चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिषह सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियाँ सहन करो, चाहे जितनी उपाधियाँ आ पड़ो, चाहे जितनी आधियाँ आ पड़ो, चाहे तो जीवनकाल एक समय मात्र हो, और दुनिमित्त हो, परतु ऐसा करना ही।
तब तक हे जीव । छुटकारा नही है।" इस प्रकार नेपथ्यमेसे उत्तर मिलता है और वह यथायोग्य लगता है।
क्षण-क्षणमे पलटनेवाली स्वभाववृत्ति नही चाहिये । अमुक काल तक शून्यके सिवाय कुछ नही चाहिये, वह न हो तो अमुक काल तक संतके सिवाय कुछ नही चाहिये, वह न हो तो अमुक काल तक सत्संगके सिवाय कुछ नही चाहिये, वह न हो तो आर्याचरण (आयपुरुषो द्वारा किये गये आचरण ) के सिवाय कुछ नही चाहिये, वह न हो तो जिनभक्तिमे अति शुद्ध भावसे लीनताके सिवाय कुछ नही चाहिये, वह न हो तो फिर मांगनेकी इच्छा भी नही है।
समझमे आये विना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं । सत्सगके बिना ध्यान तरगख्य हो जाता है। सतके बिना अतकी बातका अत नही पाया जाता । लोकसज्ञासे लोकानमे नही पहुँचा जाता । लोकत्यागके बिना वैराग्य यथायोग्य पाना दुर्लभ है।
"यह कुछ झूठा है ?" क्या ? परिभ्रमण किया सो किया; अब उसका प्रत्याख्यान लें तो ? लिया जा सकता है। यह भी आश्चर्यकारक है। अभी इतना ही, फिर सुयोगसे मिलेंगे। यही विज्ञापन ।
वि० रायचन्दके यथायोग्य ।
१२९ ववाणिया, प्रथम भादो सुदी ७, शुक्र, १९४६ बम्बई इत्यादि स्थलोमे सहन को हुई उपाधि, यहाँ आनेके बाद एकातादिका अभाव (नही होना) और वक्रताकी अप्रियताके कारण यथासम्भव त्वरासे उधर आऊँगा।
१३० ववाणिया, प्रथम भादो सुदी ११, मंगल, १९४६ धर्मेच्छुक भाई खीमजी,
कितने वर्ष हुए एक महती इच्छा अन्त करणमे रहा करती है, जिसे किसी स्थलपर नही कहा, कहा नहीं जा सका, कहा नहीं जा सकता, नही कहना आवश्यक है। महान परिश्रमसे प्राय उसे पूरा किया जा सकता है, तथापि उसके लिये यथेष्ट परिश्रम नही हो पाता, यह एक आश्चर्य और प्रमत्तता है। यह इच्छा सहज उत्पन्न हुई थी। जब तक वह यथायोग्य रीतिसे पूरी न की जाये तब तक आत्मा समाधिस्थ होना नही चाहता, अथवा नहीं होगा। यदि कभी अवसर होगा तो उस इच्छाको झांकी करा देनेका प्रयत्न करूँगा । इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडम्बनदशामे हो जीवन व्यतीत करता रहता है।