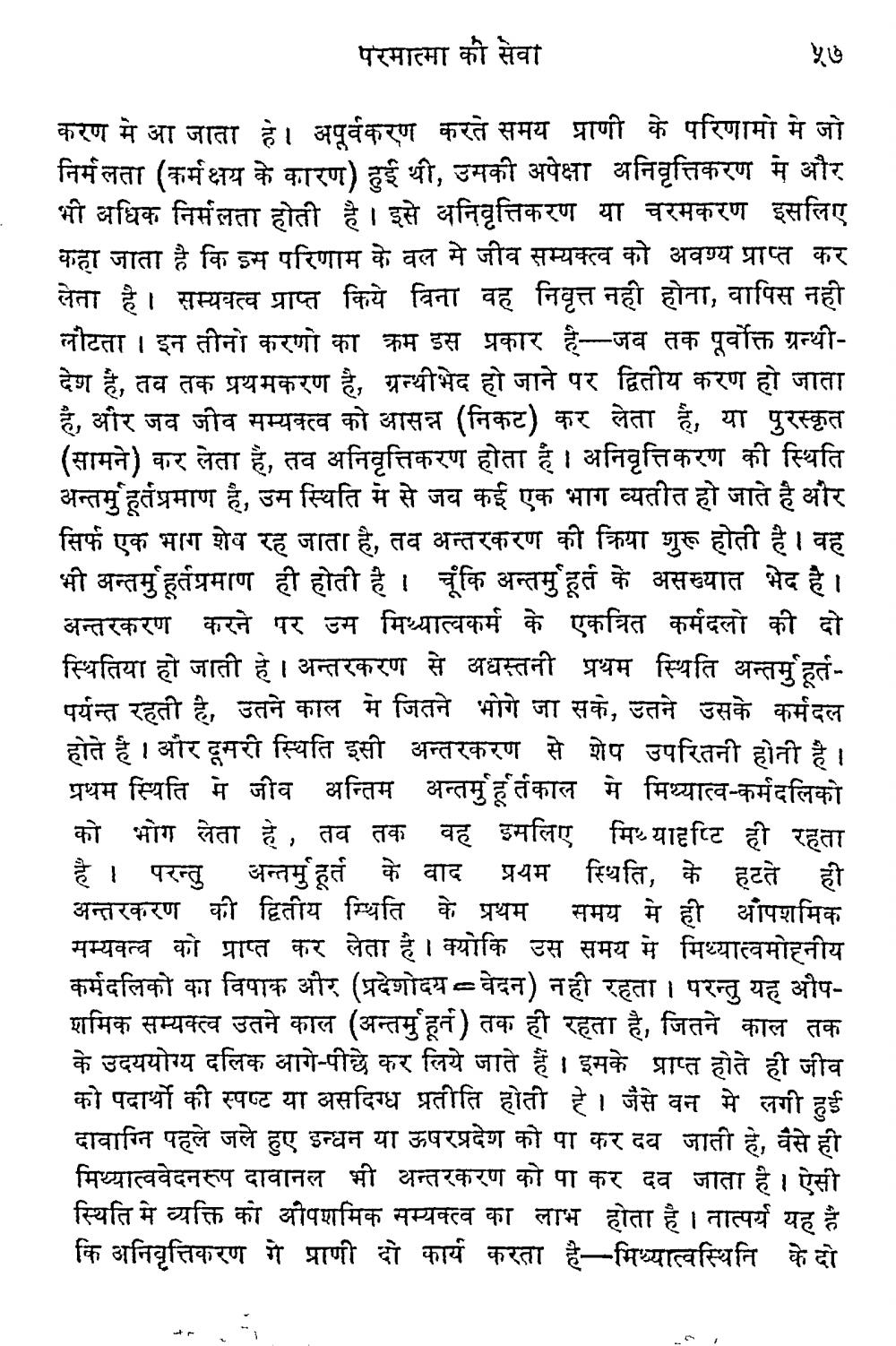________________
परमात्मा की सेवा
करण मे आ जाता है। अपूर्वकरण करते समय प्राणी के परिणामो मे जो निर्मलता (कर्मक्षय के कारण) हुई थी, उमकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरण में और भी अधिक निर्मलता होती है। इसे अनिवृत्तिकरण या चरमकरण इसलिए कहा जाता है कि इम परिणाम के बल मे जीव सम्यक्त्व को अवश्य प्राप्त कर लेता है। सस्यवत्व प्राप्त किये बिना वह निवृत्त नहीं होता, वापिस नही लौटता । इन तीनो करणो का क्रम इस प्रकार है-जव तक पूर्वोक्त ग्रन्थीदेश है, तव तक प्रथमकरण है, ग्रन्थीभेद हो जाने पर द्वितीय करण हो जाता है, और जव जीव सम्यक्त्व को आसन्न (निकट) कर लेता है, या पुरस्कृत (सामने) कर लेता है, तव अनिवृत्तिकरण होता है। अनिवृत्तिकरण की स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है, उस स्थिति में से जव कई एक भाग व्यतीत हो जाते है और सिर्फ एक भाग शेष रह जाता है, तब अन्तरकरण की क्रिया शुरू होती है। वह भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही होती है। चूंकि अन्तर्मुहूर्त के असख्यात भेद है। अन्तरकरण करने पर उस मिथ्यात्वकर्म के एकत्रित कर्मदलो की दो स्थितिया हो जाती है । अन्तरकरण से अधस्तनी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहर्तपर्यन्त रहती है, उतने काल में जितने भोगे जा सके, उतने उसके कर्मदल होते है । और दूसरी स्थिति इसी अन्तरकरण से शेप उपरितनी होती है। प्रथम स्थिति में जीव अन्तिम अन्तर्मुहूंर्तकाल मे मिथ्यात्व-कर्मदलिको को भोग लेता हे , तव तक वह इमलिए मि यादृष्टि ही रहता है। परन्तु अन्तर्मुहूर्त के बाद प्रयम स्थिति, के हटते ही अन्तरकरण की द्वितीय स्थिति के प्रथम समय मे ही औपशमिक मम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। क्योकि उस समय में मिथ्यात्वमोहनीय कर्मदलिको का विपाक और (प्रदेशोदय = वेदन) नही रहता। परन्तु यह औपशमिक सम्यक्त्व उतने काल (अन्तर्मुहूर्त) तक ही रहता है, जितने काल तक के उदययोग्य दलिक आगे-पीछे कर लिये जाते हैं। इसके प्राप्त होते ही जीव को पदार्थों की स्पष्ट या असदिग्ध प्रतीति होती है। जैसे वन मे लगी हुई दावाग्नि पहले जले हुए इन्धन या ऊपरप्रदेश को पा कर दब जाती है, वैसे ही मिथ्यात्ववेदनरूप दावानल भी अन्तरकरण को पा कर दव जाता है। ऐसी स्थिति मे व्यक्ति को औपशमिक सम्यक्त्व का लाभ होता है । तात्पर्य यह है कि अनिवृत्तिकरण गे प्राणी दो कार्य करता है-मिथ्यात्वस्थिति के दो