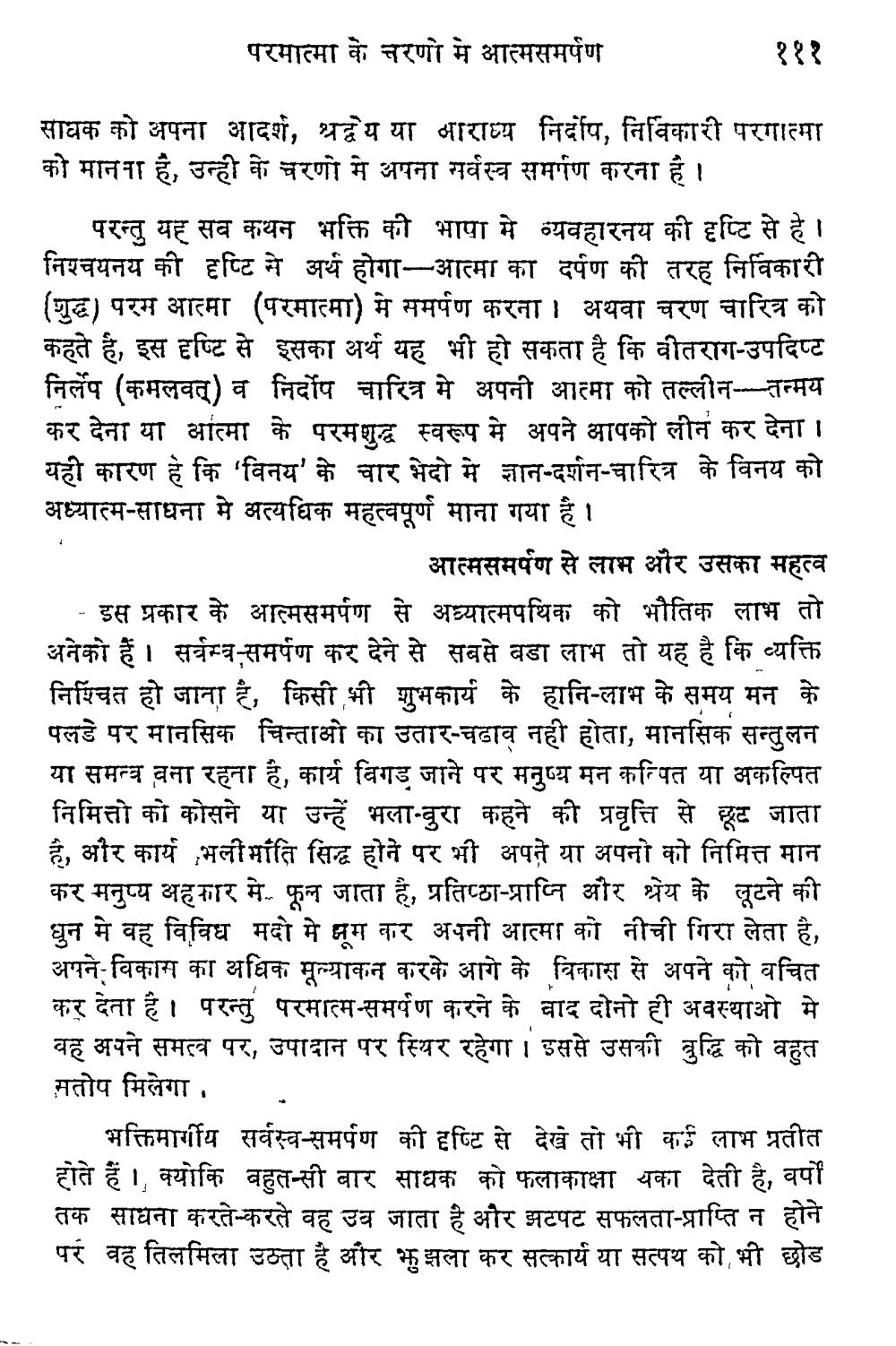________________
परमात्मा के चरणो मे आत्मसमर्पण
१११
साधक को अपना आदर्श, श्रद्वेय या आराध्य निर्दोप, निर्विकारी परमात्मा को मानना है, उन्ही के चरणो मे अपना सर्वस्व समर्पण करना है।
परन्तु यह सब कथन भक्ति की भापा मे व्यवहारनय की दृष्टि से है। निश्चयनय की दृष्टि में अर्थ होगा-आत्मा का दर्पण की तरह निर्विकारी (शुद्ध) परम आत्मा (परमात्मा) मे समर्पण करना। अथवा चरण चारित्र को कहते है, इस दृष्टि से इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वीतराग-उपदिष्ट निर्लेप (कमलवत्) व निर्दोप चारित्र मे अपनी आत्मा को तल्लीनतन्मय कर देना या आत्मा के परमशुद्ध स्वरूप में अपने आपको लीन कर देना । यही कारण है कि 'विनय' के चार भेदो मे ज्ञान-दर्शन-चारित्र के विनय को अध्यात्म-साधना मे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है।
आत्मसमर्पण से लाभ और उसका महत्व - इस प्रकार के आत्मसमर्पण से अध्यात्मपथिक को भौतिक लाभ तो अनेको हैं। सर्वम्व-समर्पण कर देने से सबसे बडा लाभ तो यह है कि व्यक्ति निश्चित हो जाता है, किसी भी शुभकार्य के हानि-लाभ के समय मन के पलडे पर मानसिक चिन्ताओ का उतार-चढाव नहीं होता, मानसिक सन्तुलन या समन्व बना रहता है, कार्य बिगड़ जाने पर मनुष्य मन कल्पित या अकल्पित निमित्तो को कोसने या उन्हें भला-बुरा कहने की प्रवृत्ति से छूट जाता है, और कार्य भलीभांति सिद्ध होने पर भी अपने या अपनो को निमित्त मान कर मनुष्य अहकार मे. फूल जाता है, प्रतिष्ठा-प्राप्ति और श्रेय के लूटने की धुन मे वह विविध मदो मे झूम कर अपनी आत्मा को नीची गिरा लेता है, अपने विकास का अधिक मूल्याकन करके आगे के विकास से अपने को वचित कर देता है। परन्तु परमात्म-समर्पण करने के बाद दोनो ही अवस्थाओ मे वह अपने समत्व पर, उपादान पर स्थिर रहेगा। इससे उसकी बुद्धि को बहुत मतोप मिलेगा . .
भक्तिमार्गीय सर्वस्व-समर्पण की दृष्टि से देखे तो भी कई लाभ प्रतीत होते हैं। क्योकि बहुत-सी बार साधक को फलाकाक्षा यका देती है, वो तक साधना करते-करते वह उब जाता है और झटपट सफलता प्राप्ति न होने पर वह तिलमिला उठता है और झु झला कर सत्कार्य या सत्पथ को भी छोड