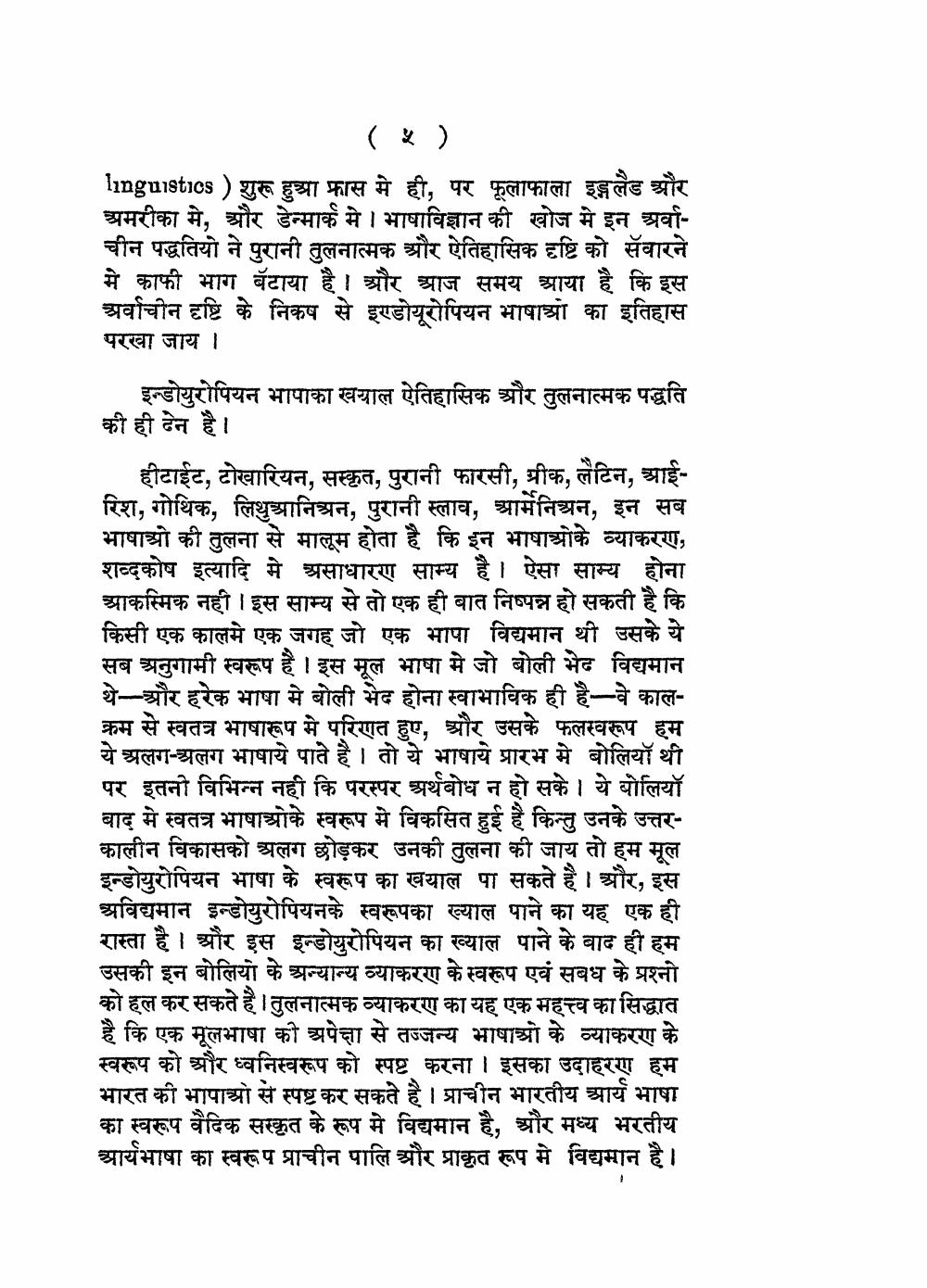________________
( ५ )
linguistics ) शुरू हुआ फ्रास मे ही, पर फूलाफाला इङ्गलैड और अमरीका मे, और डेन्मार्क मे । भाषाविज्ञान की खोज मे इन अर्वा - चीन पद्धतियों ने पुरानी तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि को सँवारने मे काफी भाग बॅटाया है । और आज समय आया है कि इस अर्वाचीन दृष्टि के निकष से इण्डोयूरोपियन भाषाओ का इतिहास
परखा जाय ।
इन्डोयुरोपियन भाषाका खयाल ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति की ही देन है ।
टाईट, टोखारियन, सस्कृत, पुरानी फारसी, ग्रीक, लैटिन, आई - रिश, गोथिक, लिथुआनिन, पुरानी स्लाव, आर्मेनियन इन सब भाषा की तुलना से मालूम होता है कि इन भाषाओके व्याकरण, शब्दकोष इत्यादि मे असाधारण साम्य है । ऐसा साम्य होना आकस्मिक नही । इस साम्य से तो एक ही बात निष्पन्न हो सकती है कि किसी एक कालमे एक जगह जो एक भाषा विद्यमान थी उसके ये सब अनुगामी स्वरूप है । इस मूल भाषा मे जो बोली भेद विद्यमान थे— और हरेक भाषा मे बोली भेद होना स्वाभाविक ही है - वे कालक्रम से स्वतंत्र भाषारूप में परिणत हुए, और उसके फलस्वरूप हम
लग-अलग भाषाये पाते है । तो ये भाषाये प्रारभ मे बोलियाँ थी पर इतनी विभिन्न नही कि परस्पर अर्थबोध न हो सके। ये बोलियाँ बाद मे स्वतंत्र भाषाओके स्वरूप मे विकसित हुई है किन्तु उनके उत्तरकालीन विकासको अलग छोड़कर उनकी तुलना की जाय तो हम मूल इन्डोयुरोपियन भाषा के स्वरूप का खयाल पा सकते है । और, इस
विद्यमान इन्डोयुरोपियनके स्वरूपका ख्याल पाने का यह एक ही रास्ता है । और इस इन्डोयुरोपियन का ख्याल पाने के बाद ही हम उसकी इन बोलियो के अन्यान्य व्याकरण के स्वरूप एवं सबध के प्रश्नो
हल कर सकते है । तुलनात्मक व्याकरण का यह एक महत्त्व का सिद्धात है कि एक मूलभाषा की अपेक्षा से तज्जन्य भाषाओ के व्याकरण के स्वरूप को और ध्वनिस्वरूप को स्पष्ट करना । इसका उदाहरण हम भारत की भाषाओ से स्पष्ट कर सकते है । प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप वैदिक संस्कृत के रूप मे विद्यमान है, और मध्य भरतीय आर्यभाषा का स्वरूप प्राचीन पालि और प्राकृत रूप मे विद्यमान है ।