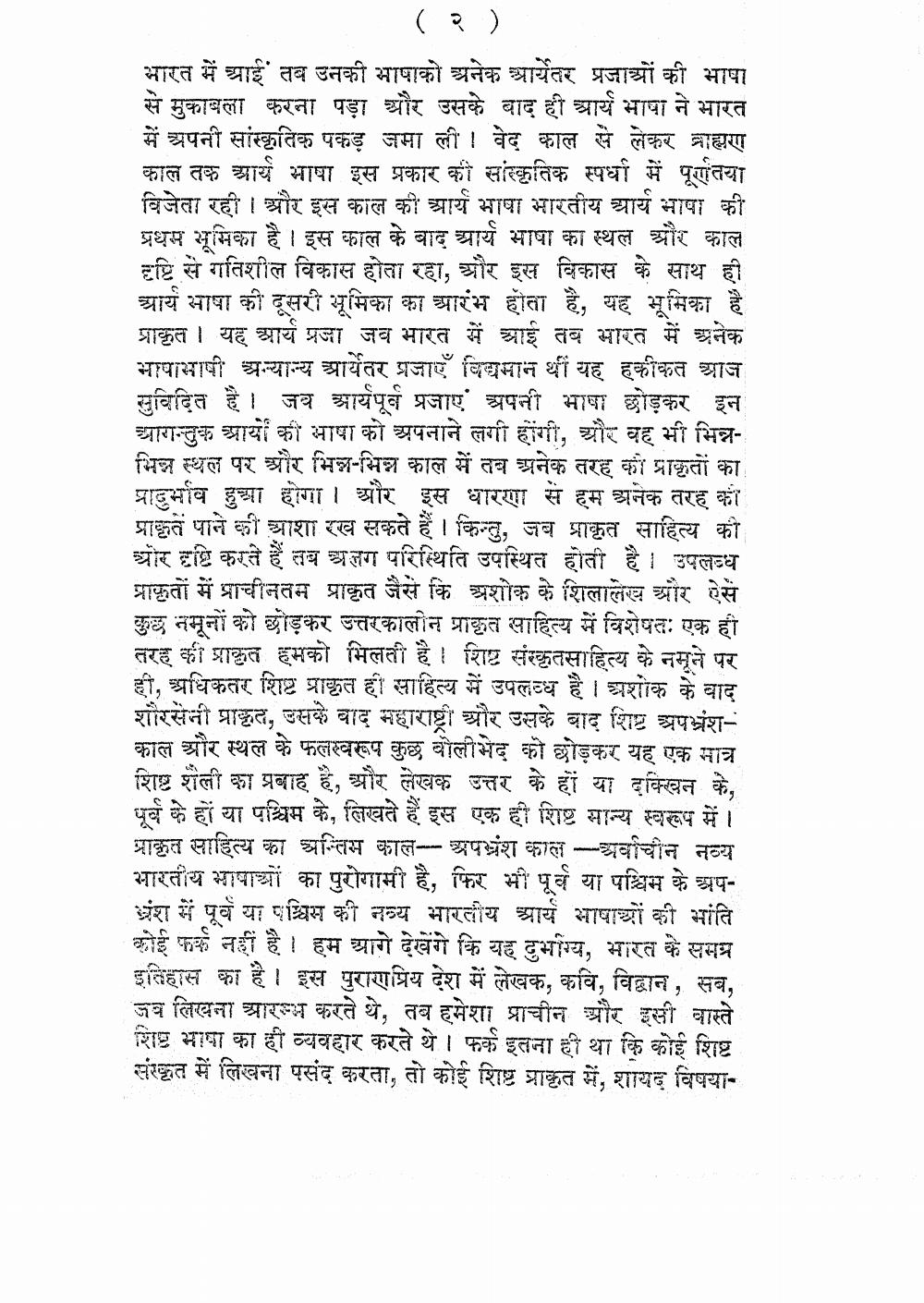________________
भारत में आई तब उनकी भाषाको अनेक आर्येतर प्रजाओं की भाषा से मुकाबला करना पड़ा और उसके बाद ही आर्य भाषा ने भारत में अपनी सांस्कृतिक पकड़ जमा ली। वेद काल से लेकर ब्राह्मण काल तक आर्य भाषा इस प्रकार की सांस्कृतिक स्पर्धा में पूर्णतया विजेता रही। और इस काल की आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा की प्रथम सूमिका है । इस काल के बाद आर्य भाषा का स्थल और काल दृष्टि से गतिशील विकास होता रहा, और इस विकास के साथ ही आर्य भाषा की दूसरी सूमिका का आरंभ होता है, यह भूमिका है प्राकृत । यह आर्य प्रजा जब भारत में आई तब भारत में अनेक भाषाभाषी अन्यान्य आर्येतर प्रजाएँ विद्यमान थीं यह हकीकत आज सुविदित है। जब आर्यपूर्व प्रजाएं अपनी भाषा छोड़कर इन अागन्तुक आर्यों की भाषा को अपनाने लगी होंगी, और वह भी भिन्नभिन्न स्थल पर और भिन्न-भिन्न काल में तब अनेक तरह की प्राकृतों का प्रादुर्भाव हुआ होगा। और इस धारणा से हम अनेक तरह की प्राकृते पाने की आशा रख सकते हैं । किन्तु, जब प्राकृत साहित्य की
और दृष्टि करते हैं तब अजग परिस्थिति उपस्थित होती है। उपलब्ध प्राकृतों में प्राचीनतम प्राकृत जैसे कि अशोक के शिलालेख और ऐसे कुछ नमूनों को छोड़कर उत्तरकालीन प्राकृत साहित्य में विशेषतः एक ही तरह की प्राकृत हमको मिलती है। शिष्ट संस्कृतसाहित्य के नमूने पर ही, अधिकतर शिष्ट प्राकृत ही साहित्य में उपलब्ध है । अशोक के बाद शौरसेनी प्राकृत, उसके बाद महाराष्ट्री और उसके बाद शिष्ट अपभ्रंशकाल और स्थल के फलस्वरूप कुछ बोलीभेद को छोड़कर यह एक मात्र शिष्ट शैली का प्रबाह है, और लेखक उत्तर के हों या दक्खिन के, पूर्व के हों या पश्चिम के, लिखते हैं इस एक ही शिष्ट मान्य स्वरूप में। प्राकृत साहित्य का अन्तिम काल- अपभ्रंश काल -अर्वाचीन नव्य भारतीय भाषाओं का पुरोगामी है, फिर भी पूर्व या पश्चिम के अपभ्रंश में पूर्व या पश्चिम की नव्य भारतीय आर्य भाषाओं की भांति कोई फर्क नहीं है। हम आगे देखेंगे कि यह दुर्भाग्य, भारत के समय इतिहास का है। इस पुराणप्रिय देश में लेखक, कवि, विद्वान , सब, जब लिखना प्रारम्भ करते थे, तब हमेशा प्राचीन और इसी वास्ते शिष्ट भाषा का ही व्यवहार करते थे। फर्क इतना ही था कि कोई शिष्ट संस्कृत में लिखना पसंद करता, तो कोई शिष्ट प्राकृत में, शायद विषया