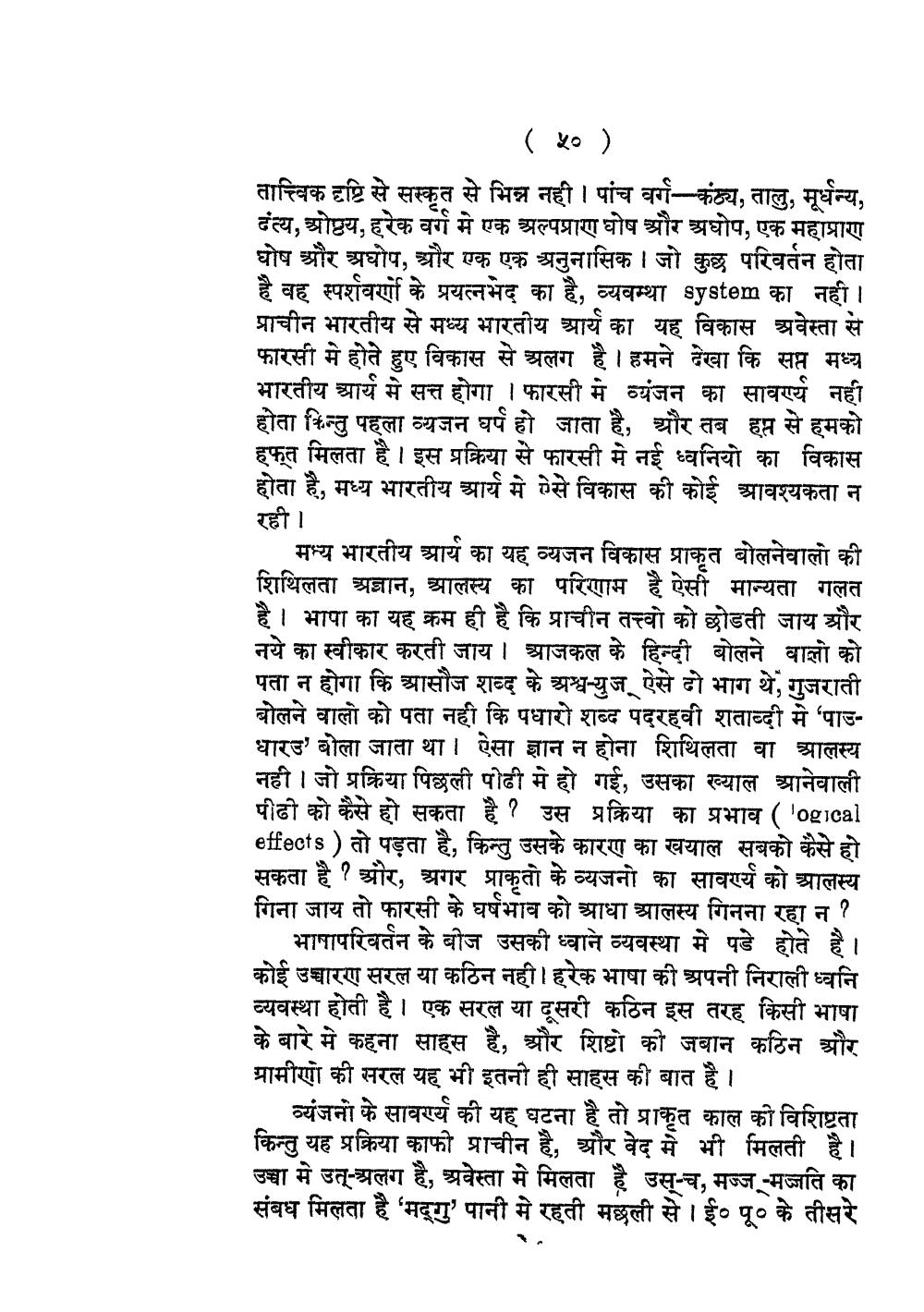________________
( ५० ) तात्त्विक दृष्टि से सस्कृत से भिन्न नही । पांच वर्ग-कंठ्य, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, अोष्ठय, हरेक वर्ग मे एक अल्पप्राण घोष और अघोप, एक महाप्राण घोष और अघोप, और एक एक अनुनासिक । जो कुछ परिवर्तन होता है वह स्पर्शवों के प्रयत्नभेद का है, व्यवस्था system का नहीं । प्राचीन भारतीय से मध्य भारतीय आर्य का यह विकास अवेस्ता से फारसी मे होते हुए विकास से अलग है। हमने देखा कि सप्त मध्य भारतीय आर्य मे सत्त होगा । फारसी में व्यंजन का सावर्ण्य नहीं होता किन्तु पहला व्यजन घर्प हो जाता है, और तब हप्त से हमको हफ्त मिलता है । इस प्रक्रिया से फारसी मे नई ध्वनियो का विकास होता है, मध्य भारतीय आर्य मे ऐसे विकास की कोई आवश्यकता न रही।
मन्य भारतीय आर्य का यह व्यजन विकास प्राकृत बोलनेवालो की शिथिलता अनान, आलस्य का परिणाम है ऐसी मान्यता गलत है। भापा का यह क्रम ही है कि प्राचीन तत्त्वो को छोडती जाय और नये का स्वीकार करती जाय । आजकल के हिन्दी बोलने वालो को पता न होगा कि आसौज शब्द के अश्व-युज ऐसे दो भाग थे, गुजराती बोलने वालो को पता नहीं कि पधारो शब्द पदरहवी शताब्दी मे 'पाउधारउ' बोला जाता था। ऐसा ज्ञान न होना शिथिलता वा आलस्य नही । जो प्रक्रिया पिछली पोढी मे हो गई, उसका ख्याल आनेवाली पीढी को कैसे हो सकता है ? उस प्रक्रिया का प्रभाव ( 'ogical effects ) तो पड़ता है, किन्तु उसके कारण का खयाल सबको कैसे हो सकता है ? और, अगर प्राकृतो के व्यजनो का सावर्ण्य को आलस्य गिना जाय तो फारसी के घर्षभाव को आधा आलस्य गिनना रहा न ? ___ भाषापरिवर्तन के बीज उसकी ध्वाने व्यवस्था मे पडे होते है। कोई उच्चारण सरल या कठिन नही। हरेक भाषा की अपनी निराली ध्वनि व्यवस्था होती है। एक सरल या दूसरी कठिन इस तरह किसी भाषा के बारे मे कहना साहस है, और शिष्टो को जबान कठिन और ग्रामीणो की सरल यह भी इतनी ही साहस की बात है।
व्यंजनों के सावर्य की यह घटना है तो प्राकृत काल को विशिष्टता किन्तु यह प्रक्रिया काफी प्राचीन है, और वेद में भी मिलती है। उच्चा मे उत्-अलग है, अवेस्ता मे मिलता है उस्-च, मज्ज-मज्जति का संबध मिलता है 'मद्गु' पानी मे रहती मछली से । ई० पू० के तीसरे