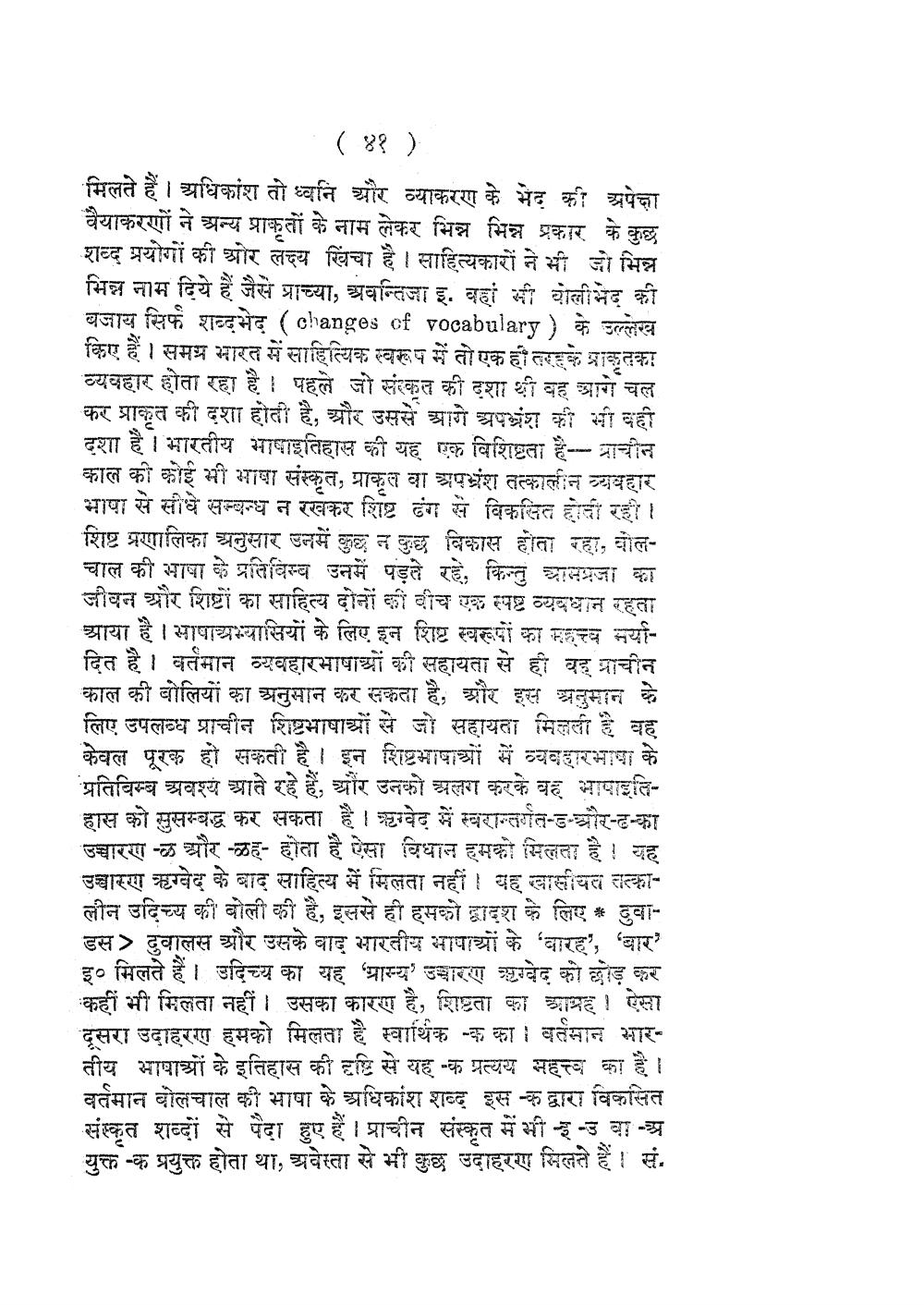________________
( ४१ ) मिलते हैं। अधिकांश तो ध्वनि और व्याकरण के भेद की अपेक्षा वैयाकरणों ने अन्य प्राकृतों के नाम लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ शब्द प्रयोगों की ओर लक्ष्य खिंचा है । साहित्यकारों ने भी जो भिन्न भिन्न नाम दिये हैं जैसे प्राच्या, अवन्तिजा इ. वहां भी बोलीभेद की बजाय सिर्फ शब्दभेद (changes of vocabulary ) के उल्लेख किए हैं। समग्र भारत में साहित्यिक स्वरूप में तो एक ही तरह प्राकृतका व्यवहार होता रहा है। पहले जो संस्कृत की दशा थी वह आगे चल कर प्राकृत की दशा होती है, और उससे आगे अपभ्रंश की भी वही दशा है । भारतीय भाषाइतिहास की यह एक विशिष्टता है-- प्राचीन काल की कोई भी भाषा संस्कृत, प्राकल वा अपभ्रंश तत्कालीन व्यवहार भाषा से सीधे सम्बन्ध न रखकर शिष्ट ढंग से विकसित होती रही। शिष्ट प्रणालिका अनुसार उनमें कुछ न कुछ विकास होता रहा, बोलचाल की भाषा के प्रतिविम्व उनमें पड़ते रहे, किन्तु बामप्रजा का जीवन और शिष्टों का साहित्य दोनों की बीच एक स्पष्ट व्यवधान रहता
आया है । सापाअभ्यासियों के लिए इन शिष्ट स्वरूपों का महत्त्व भर्यादित है। वर्तमान व्यवहारभाषाओं की सहायता से ही वह प्राचीन काल की बोलियों का अनुमान कर सकता है, और इस अनुमान के लिए उपलब्ध प्राचीन शिष्टभाषाओं से जो सहायता मिली है वह केवल पूरक हो सकती है। इन शिष्टभाषाओं में व्यवहारभाषा के प्रतिबिम्ब अवश्य आते रहे हैं, और उनको अलग करके वह भाषा इतिहास को सुसम्बद्ध कर सकता है। ऋग्वेद में स्वरान्तर्गत-ड-और-ढ-का उच्चारण - और ळह- होता है ऐसा विधान हमको मिलता है। यह उच्चारण ऋग्वेद के बाद साहित्य में मिलता नहीं। यह खासीयत तत्कालीन उदिच्य की बोली की है, इससे ही हमको द्वादश के लिए * दुवाडस > दुवालस और उसके बाद भारतीय भाषाओं के 'बारह', 'बार' इ० मिलते हैं। उदिच्य का यह 'प्रास्य' उचारण ऋग्वेद को छोड़ कर कहीं भी मिलता नहीं। उसका कारण है, शिष्टता का आग्रह ! ऐसा दूसरा उदाहरण हमको मिलता है स्वार्थिक -क का। वर्तमान भारतीय भाषाओं के इतिहास की दृष्टि से यह कि प्रत्यय महत्त्व का है। वर्तमान बोलचाल की भाषा के अधिकांश शब्द इस क द्वारा विकसित संस्कृत शब्दों से पैदा हुए हैं। प्राचीन संस्कृत में भी-इ-उ वा-अ युक्त -क प्रयुक्त होता था, अवेस्ता से भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। सं.