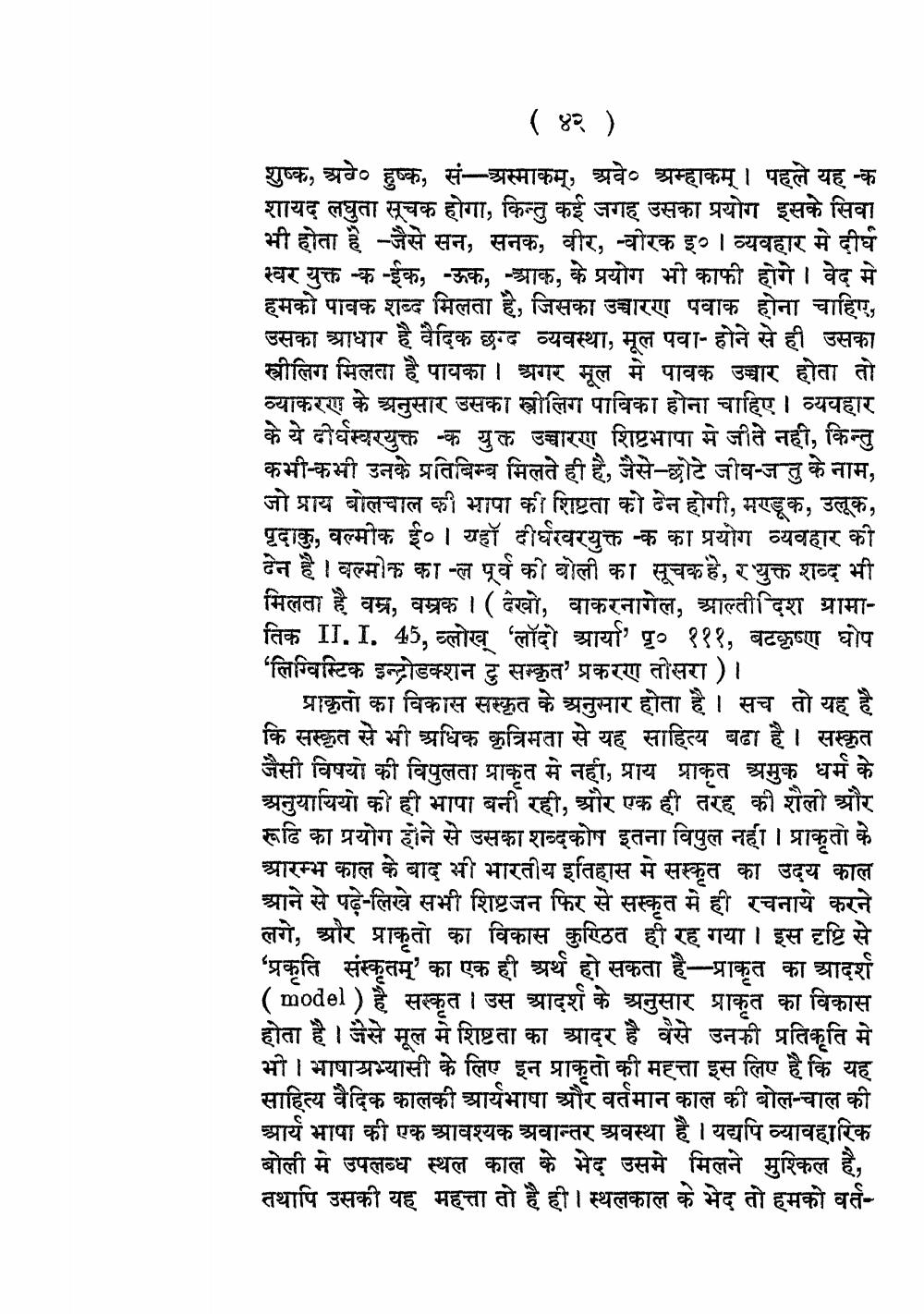________________
( ४२ ) शुष्क, अ० हुष्क, सं-अस्माकम्, अवे० अम्हाकम् । पहले यह क शायद लघुता सूचक होगा, किन्तु कई जगह उसका प्रयोग इसके सिवा भी होता है -जैसे सन, सनक, वीर, वीरक इ० । व्यवहार मे दीघ स्वर युक्त -क -ईक, -ऊक, आक, के प्रयोग भी काफी होगे । वेद मे हमको पावक शब्द मिलता है, जिसका उच्चारण पवाक होना चाहिए, उसका आधार है वैदिक छन्द व्यवस्था, मूल पवा- होने से ही उसका स्त्रीलिग मिलता है पावका । अगर मूल में पावक उच्चार होता तो व्याकरण के अनुसार उसका स्त्रीलिग पाविका होना चाहिए । व्यवहार के ये दीर्घस्वरयुक्त -क युक्त उच्चारण शिष्टभापा मे जीते नही, किन्तु कभी-कभी उनके प्रतिबिम्ब मिलते ही है, जैसे-छोटे जीव-जतु के नाम, जो प्राय बोलचाल की भाषा की शिष्टता को देन होगी, मण्डूक, उलूक, पृदाकु, वल्मीक ई० । यहाँ दीर्घरवरयुक्त -क का प्रयोग व्यवहार की देन है । बल्मोक का -ल पूर्व की बोली का सूचक है, रयुक्त शब्द भी मिलता है वन, वम्रक । ( देखो, वाकरनागेल, आल्तीदिश ग्रामातिक II. I. 45, ब्लोख 'लॉदो आर्या' पृ० १११, बटकृष्ण घोप 'लिग्विस्टिक इन्द्रोडक्शन टु सस्कृत' प्रकरण तीसरा)। __प्राकृतो का विकास सस्कृत के अनुसार होता है। सच तो यह है कि सस्कृत से भी अधिक कृत्रिमता से यह साहित्य बढा है। सस्कृत जैसी विषयो की विपुलता प्राकृत मे नहीं, प्राय प्राकृत अमुक धर्म के अनुयायियो को ही भापा बनी रही, और एक ही तरह की शैली और रूढि का प्रयोग होने से उसका शब्दकोष इतना विपुल नहीं । प्राकृतो के आरम्भ काल के बाद भी भारतीय इतिहास मे सस्कृत का उदय काल आने से पढ़े-लिखे सभी शिष्टजन फिर से सस्कृत में ही रचनाये करने लगे, और प्राकृतो का विकास कुण्ठित ही रह गया। इस दृष्टि से 'प्रकृति संस्कृतम्' का एक ही अर्थ हो सकता है-प्राकृत का आदर्श ( model ) है सस्कृत । उस आदर्श के अनुसार प्राकृत का विकास होता है । जैसे मूल मे शिष्टता का आदर है वैसे उनकी प्रतिकृति मे भी। भाषाअभ्यासी के लिए इन प्राकृतो की महत्ता इस लिए है कि यह साहित्य वैदिक कालकी आर्यभाषा और वर्तमान काल की बोल-चाल की आर्य भाषा की एक आवश्यक अवान्तर अवस्था है । यद्यपि व्यावहारिक बोली मे उपलब्ध स्थल काल के भेद उसमे मिलने मुश्किल है, तथापि उसकी यह महत्ता तो है ही। स्थलकाल के भेद तो हमको वर्त