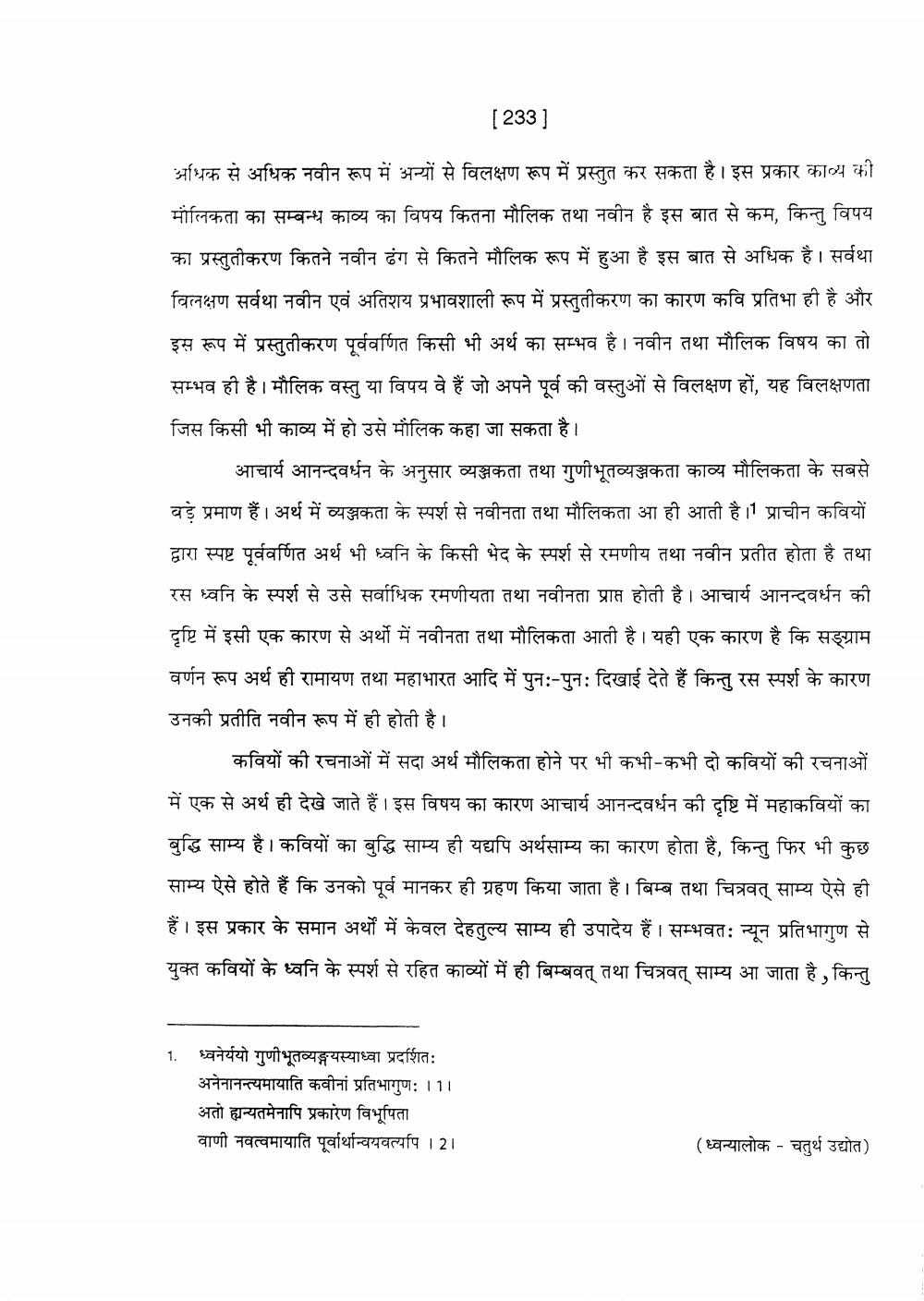________________
[233]
अधिक से अधिक नवीन रूप में अन्यों से विलक्षण रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार काव्य की मौलिकता का सम्बन्ध काव्य का विषय कितना मौलिक तथा नवीन है इस बात से कम, किन्तु विषय का प्रस्तुतीकरण कितने नवीन ढंग से कितने मौलिक रूप में हुआ है इस बात से अधिक है। सर्वथा विलक्षण सर्वथा नवीन एवं अतिशय प्रभावशाली रूप में प्रस्तुतीकरण का कारण कवि प्रतिभा ही है और इस रूप में प्रस्तुतीकरण पूर्ववर्णित किसी भी अर्थ का सम्भव है। नवीन तथा मौलिक विषय का तो सम्भव ही है। मौलिक वस्तु या विषय वे हैं जो अपने पूर्व की वस्तुओं से विलक्षण हों, यह विलक्षणता जिस किसी भी काव्य में हो उसे मौलिक कहा जा सकता है।
आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार व्यञ्जकता तथा गुणीभूतव्यञ्जकता काव्य मौलिकता के सबसे
बड़े प्रमाण हैं। अर्थ में व्यञ्जकता के स्पर्श से नवीनता तथा मौलिकता आ ही आती है। प्राचीन कवियों
द्वारा स्पष्ट पूर्ववर्णित अर्थ भी ध्वनि के किसी भेद के स्पर्श से रमणीय तथा नवीन प्रतीत होता है तथा रस ध्वनि के स्पर्श से उसे सर्वाधिक रमणीयता तथा नवीनता प्राप्त होती है। आचार्य आनन्दवर्धन की दृष्टि में इसी एक कारण से अर्थों में नवीनता तथा मौलिकता आती है। यही एक कारण है कि सङ्ग्राम वर्णन रूप अर्थ ही रामायण तथा महाभारत आदि में पुनः-पुनः दिखाई देते हैं किन्तु रस स्पर्श के कारण उनकी प्रतीति नवीन रूप में ही होती है।
कवियों की रचनाओं में सदा अर्थ मौलिकता होने पर भी कभी-कभी दो कवियों की रचनाओं
में एक से अर्थ ही देखे जाते हैं। इस विषय का कारण आचार्य आनन्दवर्धन की दृष्टि में महाकवियों का बुद्धि साम्य है। कवियों का बुद्धि साम्य ही यद्यपि अर्थसाम्य का कारण होता है, किन्तु फिर भी कुछ साम्य ऐसे होते हैं कि उनको पूर्व मानकर ही ग्रहण किया जाता है। बिम्ब तथा चित्रवत् साम्य ऐसे ही हैं। इस प्रकार के समान अर्थों में केवल देहतुल्य साम्य ही उपादेय हैं । सम्भवतः न्यून प्रतिभागुण से युक्त कवियों के ध्वनि के स्पर्श से रहित काव्यों में ही बिम्बवत् तथा चित्रवत् साम्य आ जाता है , किन्तु
1. ध्वनेर्ययो गुणीभूतव्यङ्गयस्याध्वा प्रदर्शितः
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः । 1। अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि । 2।
(ध्वन्यालोक - चतुर्थ उद्योत)