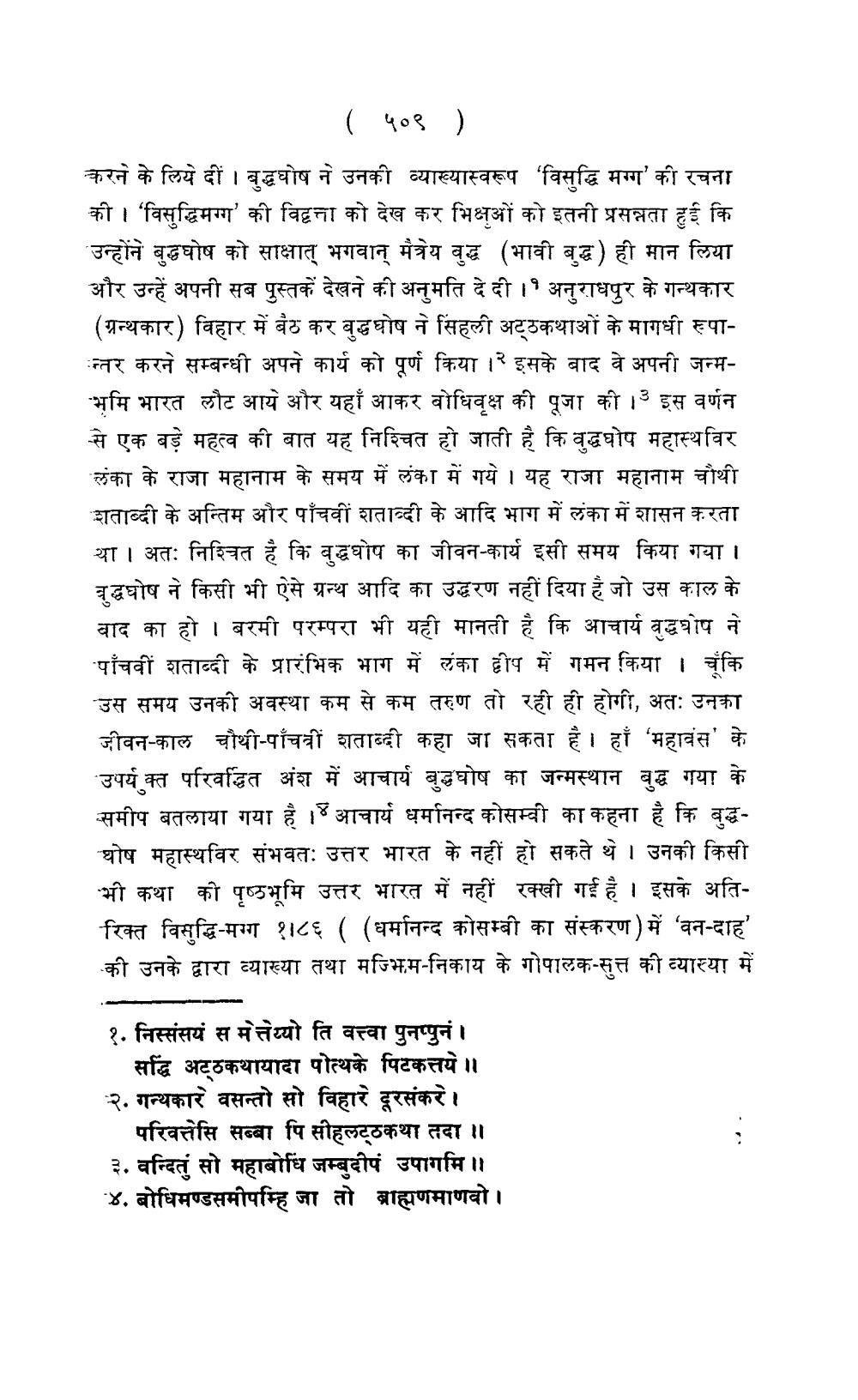________________
( ५०९ ) करने के लिये दीं । बुद्धघोष ने उनकी व्याख्यास्वरूप 'विसुद्धि मग्ग' की रचना की। 'विसुद्धिमग्ग' की विद्वत्ता को देख कर भिक्षुओं को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने बुद्धघोष को साक्षात् भगवान् मैत्रेय बुद्ध (भावी बुद्ध) ही मान लिया और उन्हें अपनी सब पुस्तकें देखने की अनुमति दे दी ।' अनुराधपुर के गन्थकार (ग्रन्थकार) विहार में बैठ कर बुद्धघोष ने सिंहली अट्ठकथाओं के मागधी रूपान्तर करने सम्बन्धी अपने कार्य को पूर्ण किया। इसके बाद वे अपनी जन्म‘भमि भारत लौट आये और यहाँ आकर बोधिवृक्ष की पूजा की। इस वर्णन से एक बड़े महत्व की बात यह निश्चित हो जाती है कि वृद्धघोष महास्थविर लंका के राजा महानाम के समय में लंका में गये । यह राजा महानाम चौथी शताब्दी के अन्तिम और पाँचवीं शताब्दी के आदि भाग में लंका में शासन करता था। अतः निश्चित है कि बुद्धघोष का जीवन-कार्य इसी समय किया गया। बुद्धघोष ने किसी भी ऐसे ग्रन्थ आदि का उद्धरण नहीं दिया है जो उस काल के वाद का हो । बरमी परम्परा भी यही मानती है कि आचार्य बुद्धघोष ने पाँचवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में लंका द्वीप में गमन किया । चूंकि उस समय उनकी अवस्था कम से कम तरुण तो रही ही होगी, अतः उनका जीवन-काल चौथी-पाँचवीं शताब्दी कहा जा सकता है। हाँ 'महावंस' के उपर्य क्त परिवद्धित अंश में आचार्य बुद्धघोष का जन्मस्थान बुद्ध गया के समीप बतलाया गया है । आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी का कहना है कि बुद्धथोष महास्थविर संभवतः उत्तर भारत के नहीं हो सकते थे। उनकी किसी भी कथा की पृष्ठभूमि उत्तर भारत में नहीं रक्खी गई है । इसके अतिरिक्त विसुद्धि-मग्ग ११८६ ( (धर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण) में 'वन-दाह' की उनके द्वारा व्याख्या तथा मज्झिम-निकाय के गोपालक-सुत्त की व्याख्या में
१. निस्संसयं स मेत्तेय्यो ति वत्त्वा पुनप्पुनं ।
सद्धि अट्ठकथायादा पोत्थके पिटकत्तये ॥ २. गन्थकारे वसन्तो सो विहारे दूरसंकरे।
परिवत्तेसि सब्बा पि सीहलट्ठकथा तदा ॥ ३. वन्दितुं सो महाबोधि जम्बुदीपं उपागमि॥ ४. बोधिमण्डसमीपम्हि जा तो ब्राह्मणमाणवो।