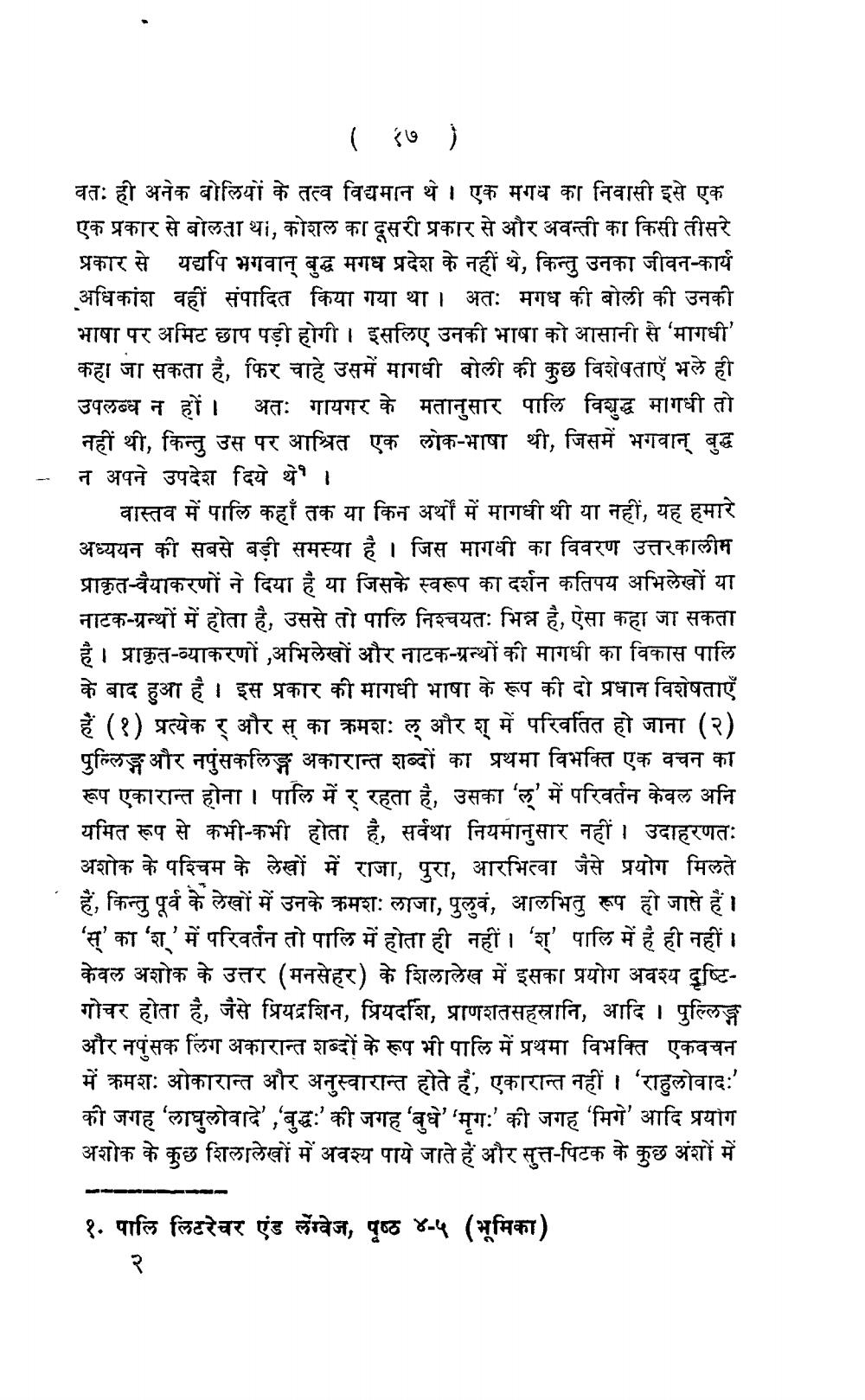________________
वतः ही अनेक बोलियों के तत्व विद्यमान थे। एक मगध का निवासी इसे एक एक प्रकार से बोलता था, कोशल का दूसरी प्रकार से और अवन्ती का किसी तीसरे प्रकार से यद्यपि भगवान् बुद्ध मगध प्रदेश के नहीं थे, किन्तु उनका जीवन-कार्य अधिकांश वहीं संपादित किया गया था। अतः मगध की बोली की उनकी भाषा पर अमिट छाप पड़ी होगी। इसलिए उनकी भाषा को आसानी से 'मागधी' कहा जा सकता है, फिर चाहे उसमें मागधी बोली की कुछ विशेषताएँ भले ही उपलब्ध न हों। अतः गायगर के मतानुसार पालि विशुद्ध मागधी तो नहीं थी, किन्तु उस पर आश्रित एक लोक-भाषा थी, जिसमें भगवान् बुद्ध न अपने उपदेश दिये थे ।
वास्तव में पालि कहाँ तक या किन अर्थों में मागधी थी या नहीं, यह हमारे अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या है । जिस मागवी का विवरण उत्तरकालीम प्राकृत-वैयाकरणों ने दिया है या जिसके स्वरूप का दर्शन कतिपय अभिलेखों या नाटक-ग्रन्थों में होता है, उससे तो पालि निश्चयतः भिन्न है, ऐसा कहा जा सकता है। प्राकृत-व्याकरणों ,अभिलेखों और नाटक-ग्रन्थों की मागधी का विकास पालि के बाद हुआ है। इस प्रकार की मागधी भाषा के रूप की दो प्रधान विशेषताएँ हैं (१) प्रत्येक र् और स् का क्रमशः ल और श् में परिवर्तित हो जाना (२) पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग अकारान्त शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप एकारान्त होना। पालि में र् रहता है, उसका 'ल' में परिवर्तन केवल अनि यमित रूप से कभी-कभी होता है, सर्वथा नियमानुसार नहीं। उदाहरणतः अशोक के पश्चिम के लेखों में राजा, पुरा, आरभित्वा जैसे प्रयोग मिलते हैं, किन्तु पूर्व के लेखों में उनके क्रमशः लाजा, पुलुवं, आलभितु रूप हो जाते हैं। 'स्' का 'श' में परिवर्तन तो पालि में होता ही नहीं। 'श्' पालि में है ही नहीं। केवल अशोक के उत्तर (मनसेहर) के शिलालेख में इसका प्रयोग अवश्य दृष्टिगोचर होता है, जैसे प्रियदशिन, प्रियदशि, प्राणशतसहस्रानि, आदि । पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिंग अकारान्त शब्दों के रूप भी पालि में प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्रमशः ओकारान्त और अनुस्वारान्त होते हैं, एकारान्त नहीं । 'राहुलोवादः' की जगह 'लाघुलोवादे' ,'बुद्धः' की जगह बुधे' 'मृगः' की जगह 'मिगे' आदि प्रयोग अशोक के कुछ शिलालेखों में अवश्य पाये जाते हैं और सुत्त-पिटक के कुछ अंशों में
१. पालि लिटरेचर एंड लेंग्वेज, पृष्ठ ४-५ (भूमिका)