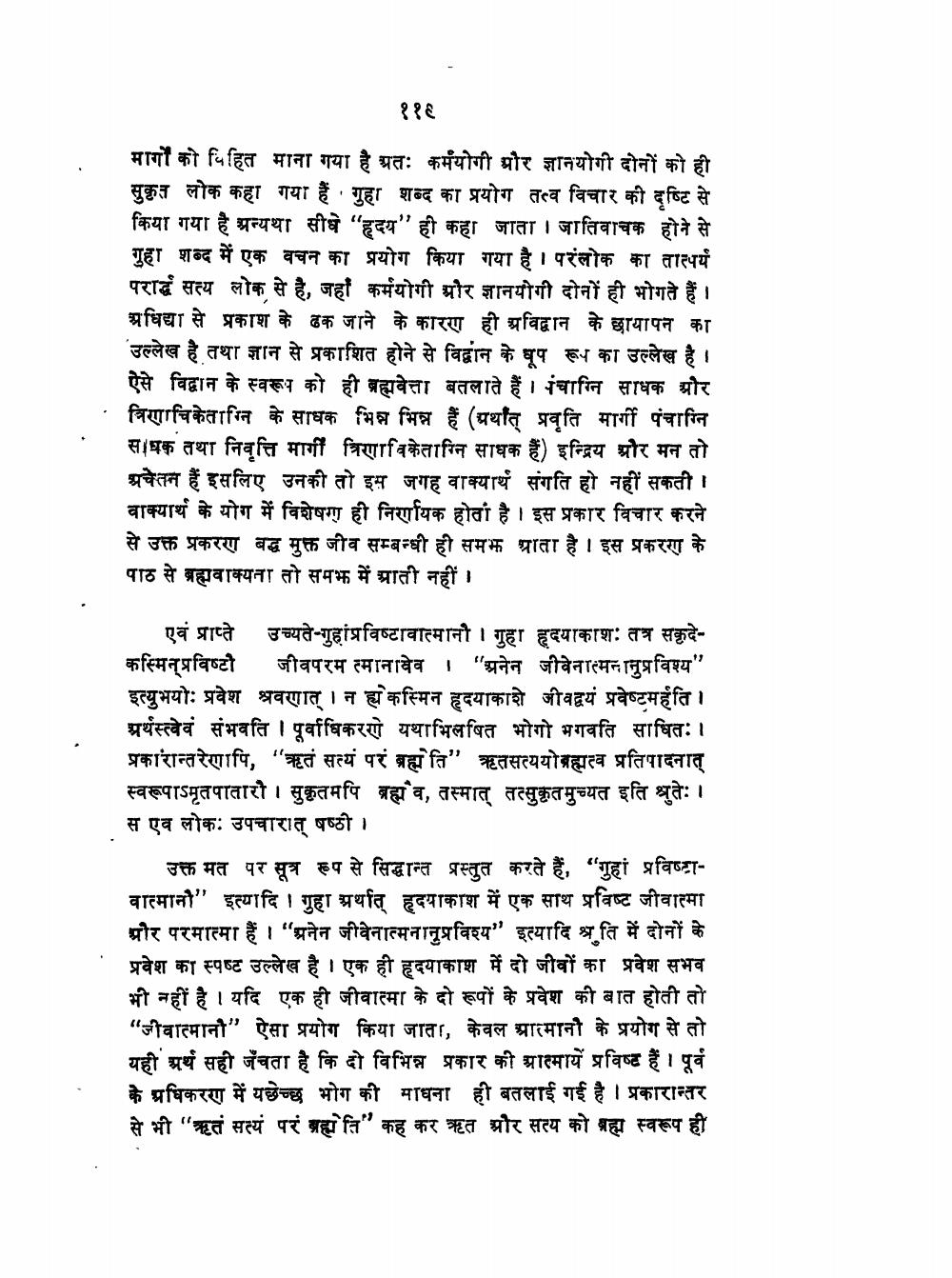________________
११६
मार्गों को विहित माना गया है अतः कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों को ही सुकृत लोक कहा गया हैं • गुहा शब्द का प्रयोग तत्व विचार की दृष्टि से किया गया है अन्यथा सीधे "हृदय" ही कहा जाता । जातिवाचक होने से गुहा शब्द में एक वचन का प्रयोग किया गया है । परलोक का तात्पर्य परार्द्ध सत्य लोक से है, जहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों ही भोगते हैं। अधिद्या से प्रकाश के ढक जाने के कारण ही अविद्वान के छायापन का उल्लेख है तथा ज्ञान से प्रकाशित होने से विद्वान के धूप रूप का उल्लेख है । ऐसे विद्वान के स्वरूप को ही ब्रह्मवेत्ता बतलाते हैं । संचाग्नि साधक और त्रिणाचिकेताग्नि के साधक भिन्न भिन्न हैं (अर्थात् प्रवृति मार्गी पंचाग्नि साधक तथा निवृत्ति मागी त्रिणाविकेताग्नि साधक हैं) इन्द्रिय और मन तो अचेतन हैं इसलिए उनकी तो इस जगह वाक्यार्थ संगति हो नहीं सकती। वाक्यार्थ के योग में विशेषण ही निर्णायक होता है । इस प्रकार विचार करने से उक्त प्रकरण बद्ध मुक्त जीव सम्बन्धी ही समझ पाता है । इस प्रकरण के पाठ से ब्रह्मवाक्यना तो समझ में आती नहीं।
एवं प्राप्ते उच्यते-गुहांप्रविष्टावात्मानौ । गुहा हृदयाकाशः तत्र सकृदेकस्मिन्प्रविष्टौ जीवपरम मानावेव । "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य" इत्युभयोः प्रवेश श्रवणात् । न ह्य कस्मिन हृदयाकाशे जीवद्वयं प्रवेष्टमर्हति । अर्थस्त्वेवं संभवति । पूर्वाधिकरणे यथाभिलषित भोगो भगवति साधितः । प्रकारान्तरेणापि, "ऋतं सत्यं परं ब्रह्मति" ऋतसत्ययोब्रह्मत्व प्रतिपादनात् स्वरूपाऽमृतपातारौ । सुकृतमपि ब्रह्मव, तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति श्रुतेः । स एव लोकः उपचारात् षष्ठी।
उक्त मत पर सूत्र रूप से सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं, "गुहां प्रविष्टावात्मानौ" इत्यादि । गुहा अर्थात् हृदयाकाश में एक साथ प्रविष्ट जीवात्मा
और परमात्मा हैं । "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य" इत्यादि श्रुति में दोनों के प्रवेश का स्पष्ट उल्लेख है । एक ही हृदयाकाश में दो जीवों का प्रवेश सभव भी नहीं है । यदि एक ही जीवात्मा के दो रूपों के प्रवेश की बात होती तो "जीवात्मानौ" ऐसा प्रयोग किया जाता, केवल प्रात्मानी के प्रयोग से तो यही अर्थ सही जंचता है कि दो विभिन्न प्रकार की आत्मायें प्रविष्ट हैं । पूर्व के अधिकरण में यछेच्छ भोग की माधना ही बतलाई गई है । प्रकारान्तर से भी "ऋतं सत्यं परं ब्रह्म ति" कह कर ऋत और सत्य को ब्रह्म स्वरूप ही