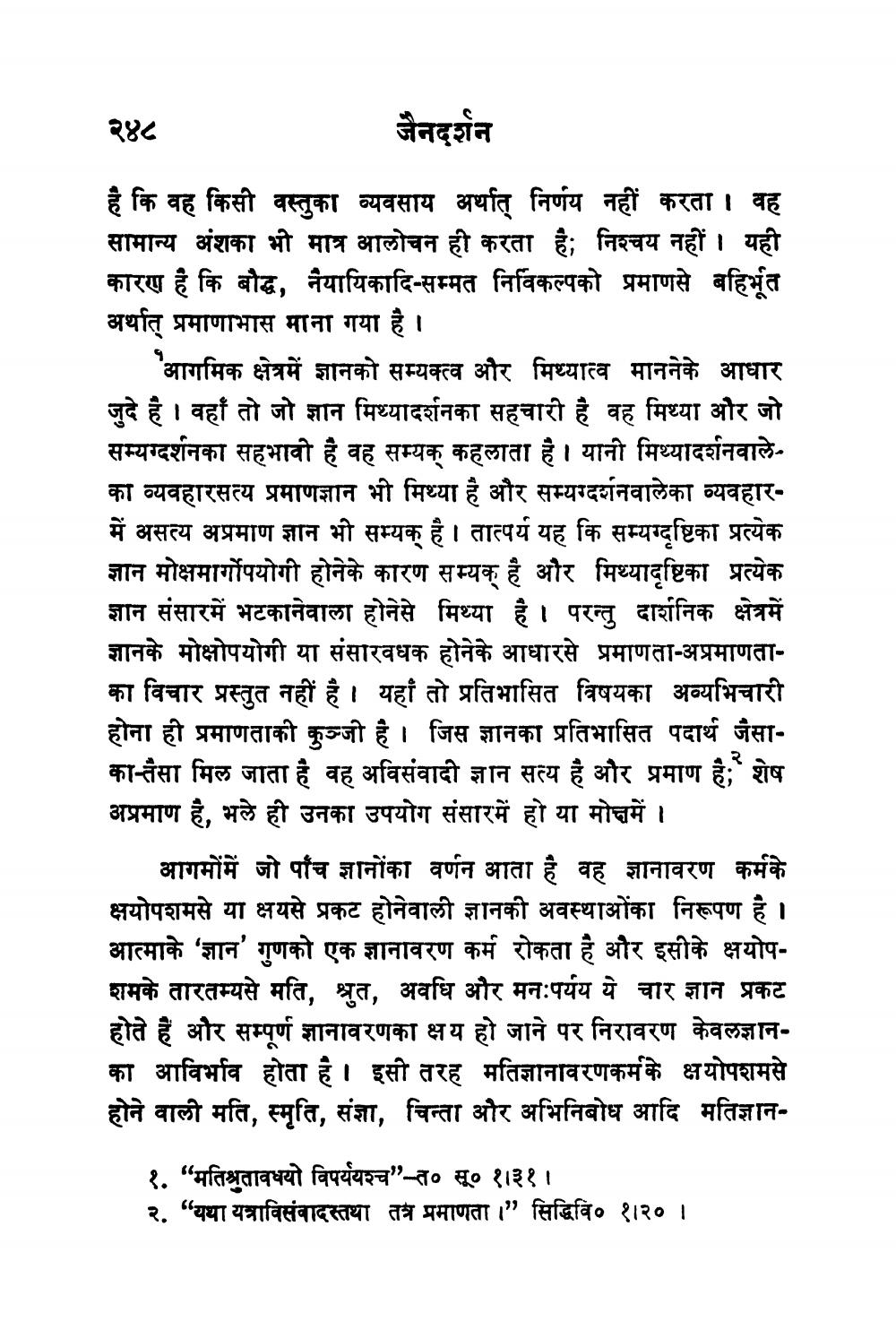________________
२४८
जैनदर्शन
है कि वह किसी वस्तुका व्यवसाय अर्थात् निर्णय नहीं करता। वह सामान्य अंशका भी मात्र आलोचन ही करता है; निश्चय नहीं। यही कारण है कि बौद्ध, नैयायिकादि-सम्मत निर्विकल्पको प्रमाणसे बहिर्भूत अर्थात् प्रमाणाभास माना गया है ।
'आगमिक क्षेत्रमें ज्ञानको सम्यक्त्व और मिथ्यात्व माननेके आधार जुदे है । वहाँ तो जो ज्ञान मिथ्यादर्शनका सहचारी है वह मिथ्या और जो सम्यग्दर्शनका सहभावी है वह सम्यक् कहलाता है। यानी मिथ्यादर्शनवाले. का व्यवहारसत्य प्रमाणज्ञान भी मिथ्या है और सम्यग्दर्शनवालेका व्यवहारमें असत्य अप्रमाण ज्ञान भी सम्यक् है । तात्पर्य यह कि सम्यग्दृष्टिका प्रत्येक ज्ञान मोक्षमार्गोपयोगी होनेके कारण सम्यक् है और मिथ्यादृष्टिका प्रत्येक ज्ञान संसारमें भटकानेवाला होनेसे मिथ्या है। परन्तु दार्शनिक क्षेत्रमें ज्ञानके मोक्षोपयोगी या संसारवधक होनेके आधारसे प्रमाणता-अप्रमाणताका विचार प्रस्तुत नहीं है। यहां तो प्रतिभासित विषयका अव्यभिचारी होना ही प्रमाणताकी कुञ्जी है। जिस ज्ञानका प्रतिभासित पदार्थ जैसाका-तैसा मिल जाता है वह अविसंवादी ज्ञान सत्य है और प्रमाण है; शेष अप्रमाण है, भले ही उनका उपयोग संसारमें हो या मोक्षमें ।
आगमोंमें जो पाँच ज्ञानोंका वर्णन आता है वह ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे या क्षयसे प्रकट होनेवाली ज्ञानकी अवस्थाओंका निरूपण है। आत्माके 'ज्ञान' गुणको एक ज्ञानावरण कर्म रोकता है और इसीके क्षयोपशमके तारतम्यसे मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये चार ज्ञान प्रकट होते हैं और सम्पूर्ण ज्ञानावरणका क्षय हो जाने पर निरावरण केवलज्ञानका आविर्भाव होता है। इसी तरह मतिज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशमसे होने वाली मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध आदि मतिज्ञान
१. "मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च"-त० सू० १।३१ । २. “यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता।" सिद्धिवि० १।२० ।