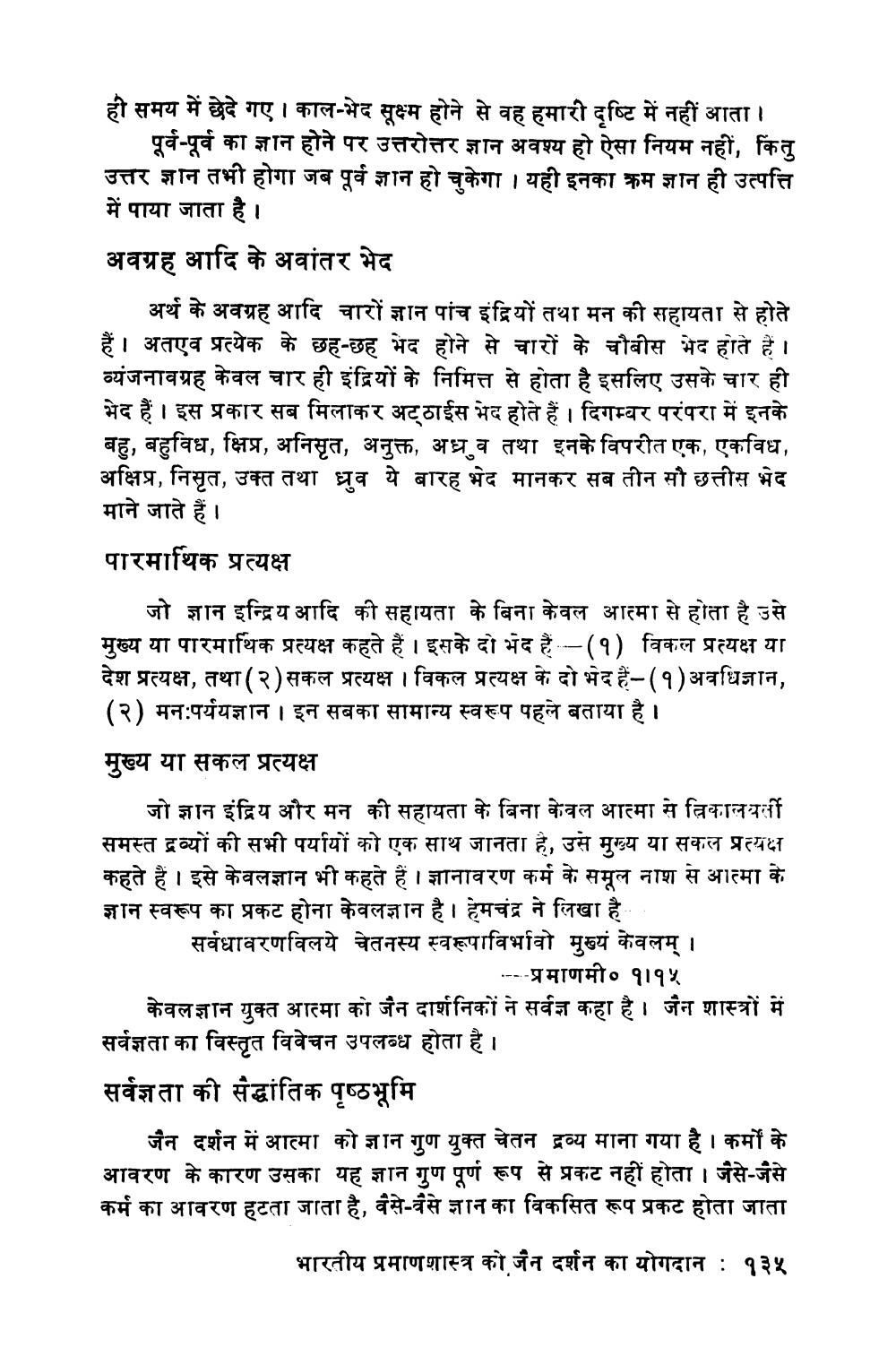________________
ही समय में छेदे गए । काल-भेद सूक्ष्म होने से वह हमारी दृष्टि में नहीं आता।
पूर्व-पूर्व का ज्ञान होने पर उत्तरोत्तर ज्ञान अवश्य हो ऐसा नियम नहीं, किंतु उत्तर ज्ञान तभी होगा जब पूर्व ज्ञान हो चुकेगा । यही इनका क्रम ज्ञान ही उत्पत्ति में पाया जाता है। अवग्रह आदि के अवांतर भेद
अर्थ के अवग्रह आदि चारों ज्ञान पांच इंद्रियों तथा मन की सहायता से होते हैं। अतएव प्रत्येक के छह-छह भेद होने से चारों के चौबीस भेद होते हैं। व्यंजनावग्रह केवल चार ही इंद्रियों के निमित्त से होता है इसलिए उसके चार ही भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर अट्ठाईस भेद होते हैं। दिगम्बर परंपरा में इनके बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, अध्र व तथा इनके विपरीत एक, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त तथा ध्रुव ये बारह भेद मानकर सब तीन सौ छत्तीस भेद माने जाते हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष
जो ज्ञान इन्द्रिय आदि की सहायता के बिना केवल आत्मा से होता है उसे मुख्य या पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं । इसके दो भेद हैं -(१) विकल प्रत्यक्ष या देश प्रत्यक्ष, तथा (२)सकल प्रत्यक्ष । विकल प्रत्यक्ष के दो भेद हैं-(१) अवधिज्ञान, (२) मन:पर्ययज्ञान । इन सबका सामान्य स्वरूप पहले बताया है। मुख्य या सकल प्रत्यक्ष
जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा से त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, उसे मुख्य या सकल प्रत्यक्ष कहते हैं । इसे केवलज्ञान भी कहते हैं । ज्ञानावरण कर्म के समूल नाश से आत्मा के ज्ञान स्वरूप का प्रकट होना केवलज्ञान है। हेमचंद्र ने लिखा है सर्वधावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्भावो मुख्यं केवलम् ।
___---प्रमाणमी० १।१५ केवलज्ञान युक्त आत्मा को जैन दार्शनिकों ने सर्वज्ञ कहा है। जैन शास्त्रों में सर्वज्ञता का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। सर्वज्ञता की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि
जैन दर्शन में आत्मा को ज्ञान गुण युक्त चेतन द्रव्य माना गया है । कर्मों के आवरण के कारण उसका यह ज्ञान गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता। जैसे-जैसे कर्म का आवरण हटता जाता है, वैसे-वैसे ज्ञान का विकसित रूप प्रकट होता जाता
भारतीय प्रमाणशास्त्र को जैन दर्शन का योगदान : १३५