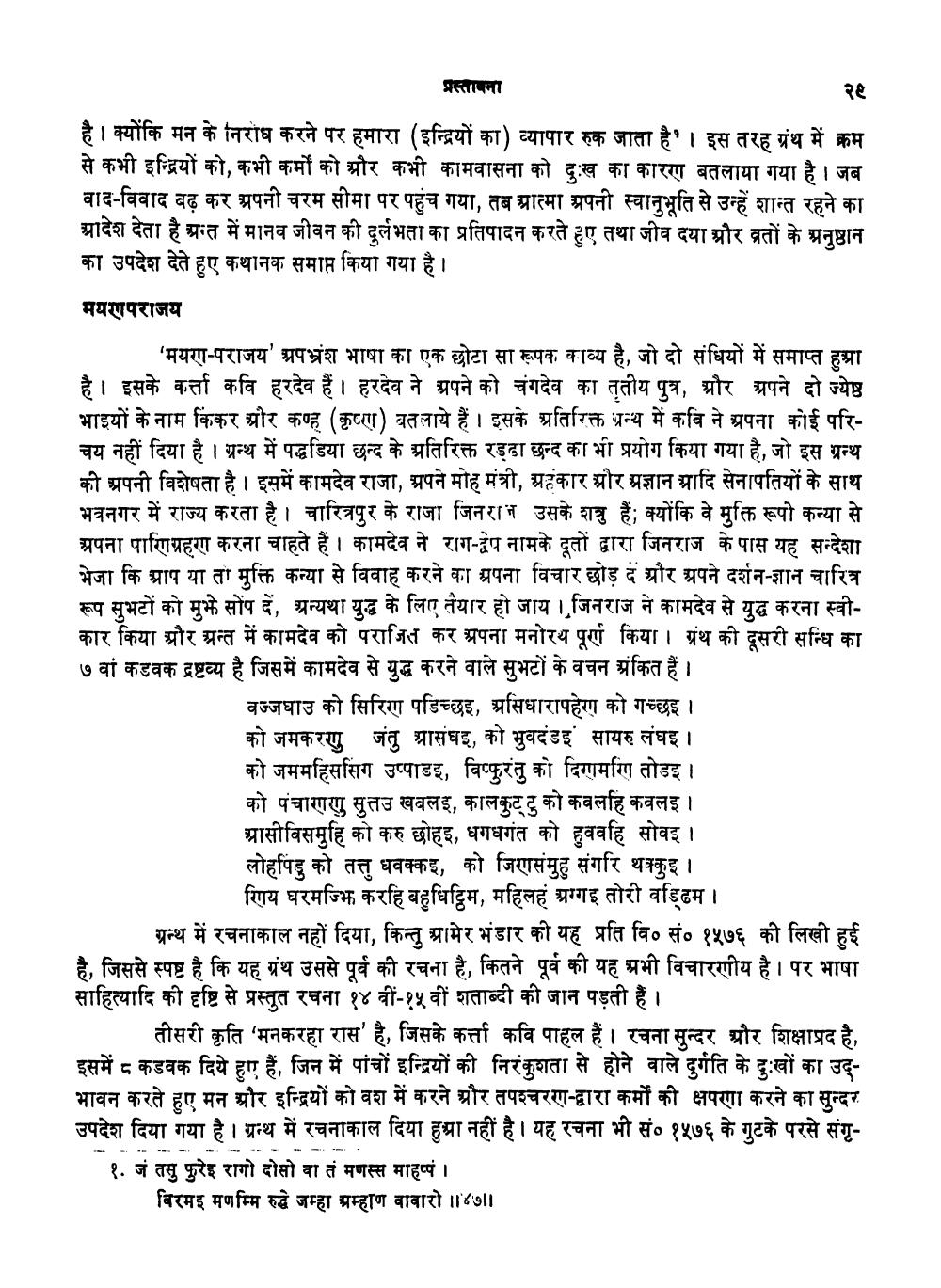________________
प्रस्तावना
२९
है। क्योंकि मन के निरोध करने पर हमारा (इन्द्रियों का) व्यापार रुक जाता है। इस तरह ग्रंथ में क्रम से कभी इन्द्रियों को, कभी कर्मों को और कभी कामवासना को दुःख का कारण बतलाया गया है। जब वाद-विवाद बढ़ कर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब आत्मा अपनी स्वानुभूति से उन्हें शान्त रहने का आदेश देता है अन्त में मानव जीवन की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए तथा जीव दया और व्रतों के अनुष्ठान का उपदेश देते हुए कथानक समाप्त किया गया है। मयणपराजय
'मयण-पराजय' अपभ्रंश भाषा का एक छोटा सा रूपक काव्य है, जो दो संधियों में समाप्त हुआ है। इसके कर्ता कवि हरदेव हैं। हरदेव ने अपने को चंगदेव का तृतीय पुत्र, और अपने दो ज्येष्ठ भाइयों के नाम किंकर और कण्ह (कृष्ण) बतलाये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य में कवि ने अपना कोई परिचय नहीं दिया है । ग्रन्थ में पद्धडिया छन्द के अतिरिक्त रड्ढा छन्द का भी प्रयोग किया गया है, जो इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। इसमें कामदेव राजा, अपने मोह मंत्री, अहंकार और प्रज्ञान आदि सेनापतियों के साथ भवनगर में राज्य करता है। चारित्रपुर के राजा जिनरान उसके शत्रु हैं; क्योंकि वे मुक्ति रूपो कन्या से अपना पाणिग्रहण करना चाहते हैं। कामदेव ने राग-द्वेप नामके दूतों द्वारा जिनराज के पास यह सन्देशा भेजा कि आप या ता मुक्ति कन्या से विवाह करने का अपना विचार छोड़ द और अपने दर्शन-ज्ञान चारित्र रूप सुभटों को मुझे सोंप दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाय । जिनराज ने कामदेव से युद्ध करना स्वीकार किया और अन्त में कामदेव को पराजित कर अपना मनोरथ पूर्ण किया। ग्रंथ की दूसरी सन्धि का ७ वां कडवक द्रष्टव्य है जिसमें कामदेव से युद्ध करने वाले सुभटों के वचन अंकित हैं।
वज्जघाउ को सिरिण पडिच्छइ, असिधारापहेण को गच्छइ । को जमकरणु जंतु यासंघइ, को भुवदंडइ सायरु लंघइ। को जममहिससिंग उप्पाडइ, विप्फुरंतु को दिणमरिग तोडइ । को पंचाणणु सुत्तउ खवलइ, कालकुट टु को कवलहि कवलइ । पासीविसमुहि को करु छोहइ, धगधगंत को हुववहि सोवइ । लोहपिडु को तत्तु धवक्कइ, को जिणसंमुहु संगरि थक्कुइ ।
रिणय घरमज्झि करहि बहुधिट्टिम, महिलहं अग्गइ तोरी वढिम । ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया, किन्तु आमेर भंडार की यह प्रति वि० सं० १५७६ की लिखी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ उससे पूर्व की रचना है, कितने पूर्व की यह अभी विचारणीय है। पर भाषा साहित्यादि की दृष्टि से प्रस्तुत रचना १४ वीं-१५ वीं शताब्दी की जान पड़ती हैं।
तीसरी कृति 'मनकरहा रास' है, जिसके कर्ता कवि पाहल हैं। रचना सुन्दर और शिक्षाप्रद है, इसमें ८ कडवक दिये हुए हैं, जिन में पांचों इन्द्रियों की निरंकुशता से होने वाले दुर्गति के दुःखों का उद्भावन करते हुए मन और इन्द्रियों को वश में करने और तपश्चरण-द्वारा कर्मों की क्षपणा करने का सुन्दर उपदेश दिया गया है । ग्रन्थ में रचनाकाल दिया हुआ नहीं है। यह रचना भी सं० १५७६ के गुटके परसे संगृ१. जं तसु फुरेइ रागो दोसो वा तं मणस्स माहप्पं ।
विरमइ मणम्मि रुद्ध जम्हा अम्हाण वावारो॥४७॥