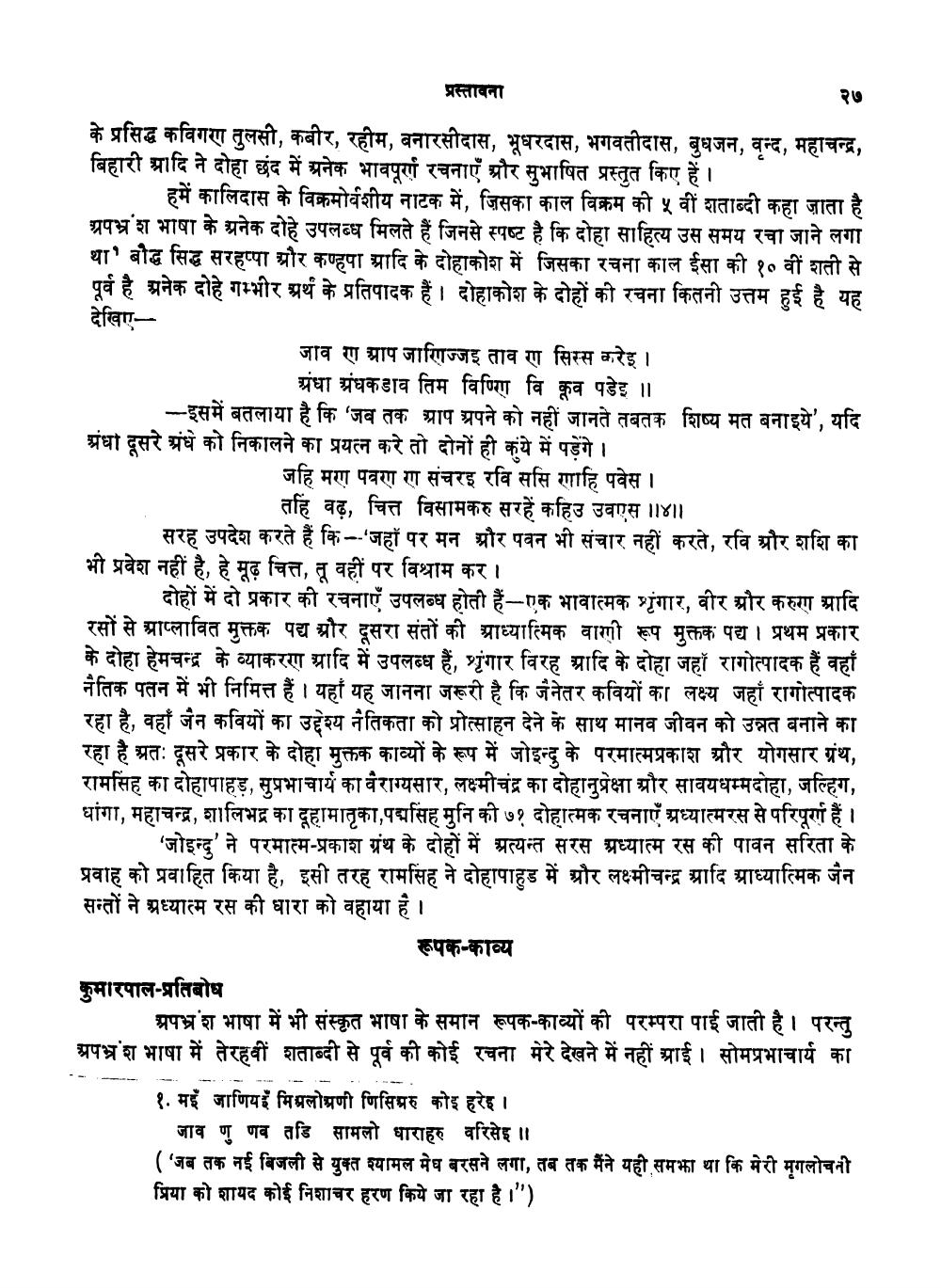________________
२७
प्रस्तावना के प्रसिद्ध कविगण तुलसी, कबीर, रहीम, बनारसीदास, भूधरदास, भगवतीदास, बुधजन, वृन्द, महाचन्द्र, बिहारी आदि ने दोहा छंद में अनेक भावपूर्ण रचनाएँ और सुभाषित प्रस्तुत किए हैं।
___हमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में, जिसका काल विक्रम की ५ वीं शताब्दी कहा जाता है अपभ्रंश भाषा के अनेक दोहे उपलब्ध मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि दोहा साहित्य उस समय रचा जाने लगा था' बौद्ध सिद्ध सरहप्पा और कण्हपा आदि के दोहाकोश में जिसका रचना काल ईसा की १० वीं शती से पूर्व है अनेक दोहे गम्भीर अर्थ के प्रतिपादक हैं। दोहाकोश के दोहों की रचना कितनी उत्तम हुई है यह देखिए
जाव रण आप जाणिज्जइ ताव ण सिस्स करेइ ।
अंधा अंधकडाव तिम विणि वि कूव पडेइ ॥ -इसमें बतलाया है कि 'जब तक आप अपने को नहीं जानते तबतक शिष्य मत बनाइये', यदि अंधो दूसरे अंधे को निकालने का प्रयत्न करे तो दोनों ही कुंये में पड़ेंगे।
जहि मण पवरण ण संचरइ रवि ससि रणाहि पवेस ।
तहिं बढ़, चित्त विसामकरु सरहें कहिउ उवएस ॥४॥ सरह उपदेश करते हैं कि-'जहाँ पर मन और पवन भी संचार नहीं करते, रवि और शशि का भी प्रवेश नहीं है, हे मूढ़ चित्त, तू वहीं पर विश्राम कर ।
दोहों में दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं-एक भावात्मक शृंगार, वीर और करुण आदि रसों से प्राप्लावित मुक्तक पद्य और दूसरा संतों की आध्यात्मिक वागी रूप मुक्तक पद्य । प्रथम प्रकार के दोहा हेमचन्द्र के व्याकरण आदि में उपलब्ध हैं, शृंगार विरह आदि के दोहा जहाँ रागोत्पादक हैं वहाँ नैतिक पतन में भी निमित्त हैं । यहाँ यह जानना जरूरी है कि जैनेतर कवियों का लक्ष्य जहाँ रागोत्पादक रहा है, वहाँ जैन कवियों का उद्देश्य नैतिकता को प्रोत्साहन देने के साथ मानव जीवन को उन्नत बनाने का रहा है अतः दूसरे प्रकार के दोहा मुक्तक काव्यों के रूप में जोइन्दु के परमात्मप्रकाश और योगसार ग्रंथ, रामसिंह का दोहापाहड़, सुप्रभाचार्य का वैराग्यसार, लक्ष्मीचंद्र का दोहानुप्रेक्षा और सावयधम्मदोहा, जल्हिग, धांगा, महाचन्द्र, शालिभद्र का दूहामातृका,पद्मसिंह मुनि की ७१ दोहात्मक रचनाएँ अध्यात्मरस से परिपूर्ण हैं ।
'जोइन्दु' ने परमात्म-प्रकाश ग्रंथ के दोहों में अत्यन्त सरस अध्यात्म रस की पावन सरिता के प्रवाह को प्रवाहित किया है, इसी तरह रामसिंह ने दोहापाहुड में और लक्ष्मीचन्द्र आदि आध्यात्मिक जैन सन्तों ने अध्यात्म रस की धारा को वहाया है।
रूपक-काव्य कुमारपाल-प्रतिबोध
अपभ्रंश भाषा में भी संस्कृत भाषा के समान रूपक-काव्यों की परम्परा पाई जाती है। परन्तु अपभ्रंश भाषा में तेरहवीं शताब्दी से पूर्व की कोई रचना मेरे देखने में नहीं आई। सोमप्रभाचार्य का
१. मई जाणियाँ मिप्रलोमणी णिसिमरु कोइ हरेइ ।
जाव णु णव तडि सामलो धाराहरु वरिसेइ ॥ ('जब तक नई बिजली से युक्त श्यामल मेघ बरसने लगा, तब तक मैंने यही समझा था कि मेरी मगलोचनी प्रिया को शायद कोई निशाचर हरण किये जा रहा है।")