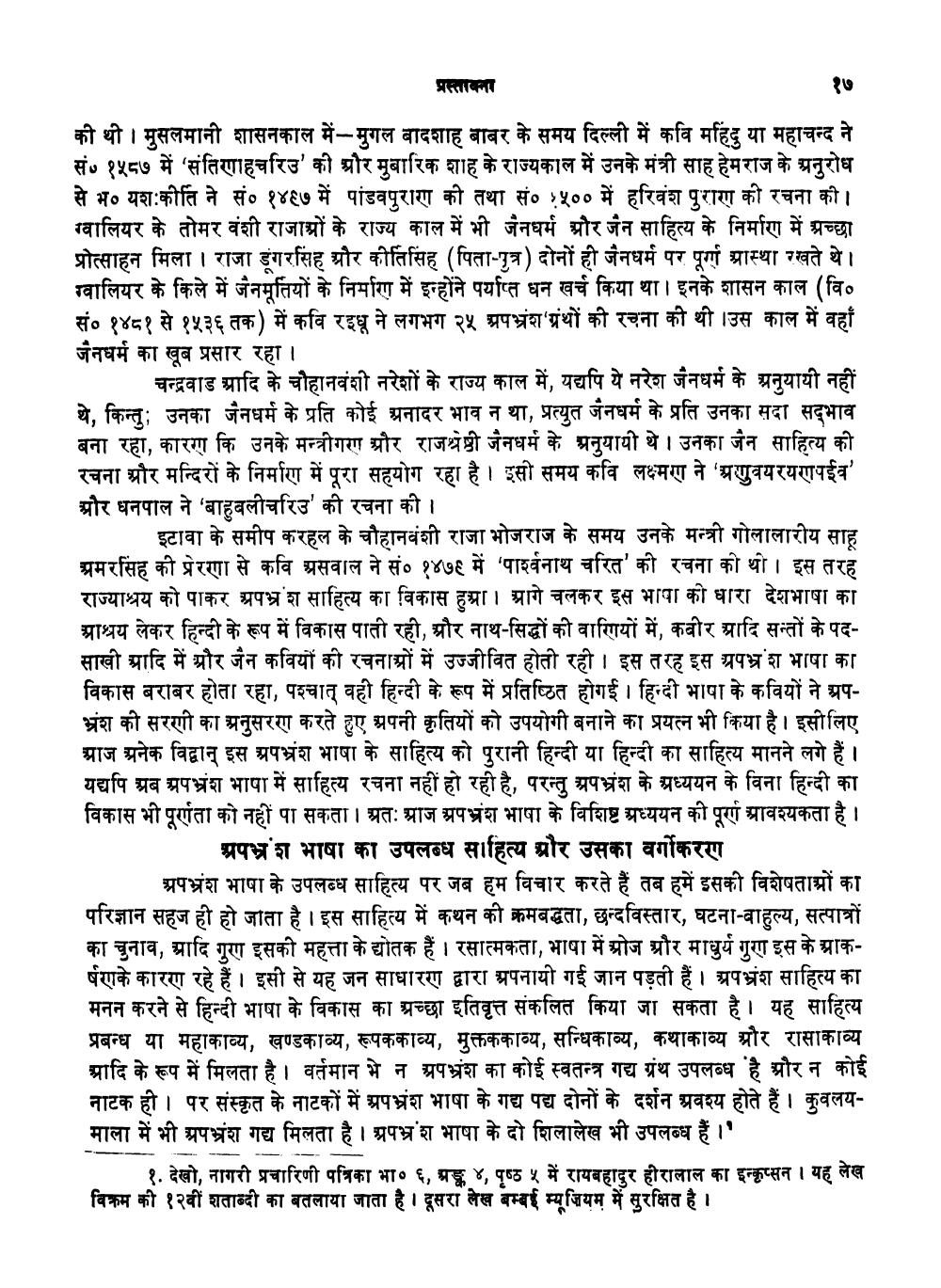________________
प्रस्तावना
की थी। मुसलमानी शासनकाल में-मुगल बादशाह बाबर के समय दिल्ली में कवि महिंदु या महाचन्द ने सं० १५८७ में 'संतिणाहचरिउ' की और मुबारिक शाह के राज्यकाल में उनके मंत्री साह हेमराज के अनुरोध से भ० यशःकीर्ति ने सं० १४६७ में पांडवपुराण को तथा सं० १५०० में हरिवंश पुराण की रचना की। ग्वालियर के तोमर वंशी राजाओं के राज्य काल में भी जैनधर्म और जैन साहित्य के निर्माण में अच्छा प्रोत्साहन मिला। राजा डूंगरसिंह और कीर्तिसिंह (पिता-पुत्र) दोनों ही जैनधर्म पर पूर्ण आस्था रखते थे। ग्वालियर के किले में जैनमूर्तियों के निर्माण में इन्होंने पर्याप्त धन खर्च किया था। इनके शासन काल (वि. सं० १४८१ से १५३६ तक) में कवि रइधू ने लगभग २५ अपभ्रंश ग्रंथों की रचना की थी ।उस काल में वहाँ जैनधर्म का खूब प्रसार रहा।
चन्द्रवाड आदि के चौहानवंशी नरेशों के राज्य काल में, यद्यपि ये नरेश जैनधर्म के अनुयायी नहीं थे, किन्तु; उनका जैनधर्म के प्रति कोई अनादर भाव न था, प्रत्युत जैनधर्म के प्रति उनका सदा सद्भाव बना रहा, कारण कि उनके मन्त्रीगण और राजश्रेष्ठी जैनधर्म के अनुयायी थे। उनका जैन साहित्य की रचना और मन्दिरों के निर्माण में पूरा सहयोग रहा है। इसी समय कवि लक्ष्मण ने 'अणुवयरयणपईव' और धनपाल ने 'बाहुबलीचरिउ' की रचना की।
इटावा के समीप करहल के चौहानवंशी राजा भोजराज के समय उनके मन्त्री गोलालारीय साहू अमरसिंह की प्रेरणा से कवि असवाल ने सं० १४७६ में 'पार्श्वनाथ चरित' की रचना की थी। इस तरह राज्याश्रय को पाकर अपभ्रश साहित्य का विकास हुआ। आगे चलकर इस भाषा की धारा देशभाषा का आश्रय लेकर हिन्दी के रूप में विकास पाती रही, और नाथ-सिद्धों की वाणियों में, कबीर आदि सन्तों के पदसाखी आदि में और जैन कवियों की रचनाओं में उज्जीवित होती रही। इस तरह इस अपभ्रंश भाषा का विकास बराबर होता रहा, पश्चात् वही हिन्दी के रूप में प्रतिष्ठित होगई। हिन्दी भाषा के कवियों ने अपभ्रंश की सरणी का अनुसरण करते हुए अपनी कृतियों को उपयोगी बनाने का प्रयत्न भी किया है। इसीलिए आज अनेक विद्वान् इस अपभ्रंश भाषा के साहित्य को पुरानी हिन्दी या हिन्दी का साहित्य मानने लगे हैं। यद्यपि अब अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना नहीं हो रही है, परन्तु अपभ्रंश के अध्ययन के विना हिन्दी का विकास भी पूर्णता को नहीं पा सकता । अतः अाज अपभ्रंश भाषा के विशिष्ट अध्ययन की पूर्ण आवश्यकता है ।
__ अपभ्रंश भाषा का उपलब्ध साहित्य और उसका वर्गीकरण
अपभ्रंश भाषा के उपलब्ध साहित्य पर जब हम विचार करते हैं तब हमें इसकी विशेषताओं का परिज्ञान सहज ही हो जाता है । इस साहित्य में कथन की क्रमबद्धता, छन्दविस्तार, घटना-बाहुल्य, सत्पात्रों का चुनाव, आदि गुरण इसकी महत्ता के द्योतक हैं। रसात्मकता, भाषा में ओज और माधुर्य गुण इस के प्राकर्षणके कारण रहे हैं। इसी से यह जन साधारण द्वारा अपनायी गई जान पड़ती हैं। अपभ्रंश साहित्य का मनन करने से हिन्दी भाषा के विकास का अच्छा इतिवृत्त संकलित किया जा सकता है। यह साहित्य प्रबन्ध या महाकाव्य, खण्डकाव्य, रूपककाव्य, मुक्तककाव्य, सन्धिकाव्य, कथाकाव्य और रासाकाव्य आदि के रूप में मिलता है। वर्तमान भे न अपभ्रंश का कोई स्वतन्त्र गद्य ग्रंथ उपलब्ध है और न कोई नाटक ही। पर संस्कृत के नाटकों में अपभ्रंश भाषा के गद्य पद्य दोनों के दर्शन अवश्य होते हैं। कुवलयमाला में भी अपभ्रंश गद्य मिलता है । अपभ्रंश भाषा के दो शिलालेख भी उपलब्ध हैं।'
१. देखो, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भा०६, अङ्क ४, पृष्ठ ५ में रायबहादुर हीरालाल का इन्कृप्सन । यह लेख विक्रम की १२वीं शताब्दी का बतलाया जाता है । दूसरा लेख बम्बई म्यूजियम में सुरक्षित है ।