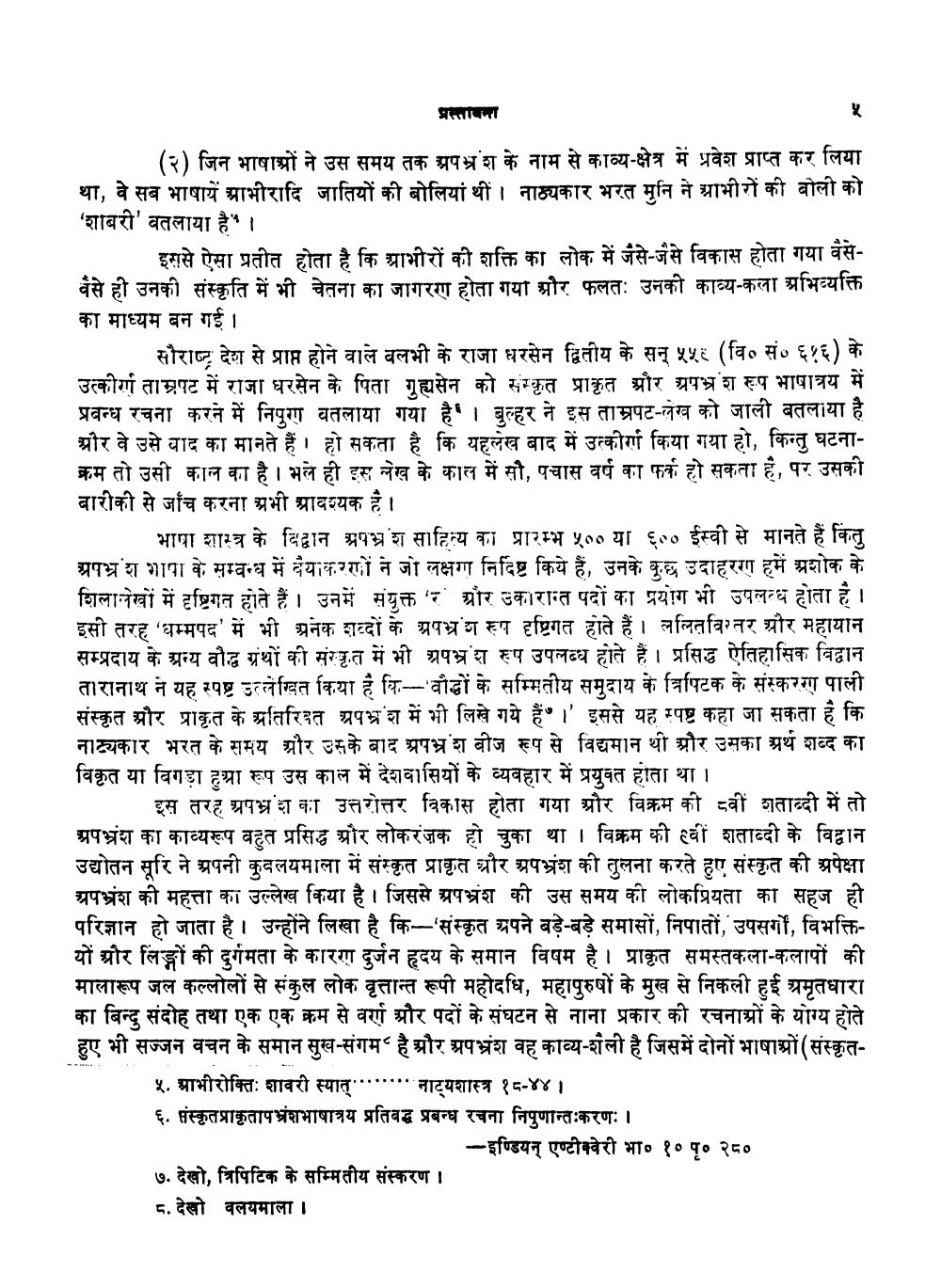________________
(२) जिन भाषाओं ने उस समय तक अपभ्रंश के नाम से काव्य-क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लिया था, वे सब भाषायें आभीरादि जातियों की बोलियां थीं। नाठ्यकार भरत मुनि ने आभीरों की बोली को 'शाबरी' बतलाया है।
____इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आभीरों की शक्ति का लोक में जैसे-जैसे विकास होता गया वैसेवैसे ही उनकी संस्कृति में भी चेतना का जागरण होता गया और फलतः उनकी काव्य-कला अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई।
सौराष्ट्र देश से प्राप्त होने वाले बलभी के राजा धरसेन द्वितीय के सन् ५५६ (वि० सं० ६१६) के उत्कीर्ण ताम्रपट में राजा धरसेन के पिता गृह्यसेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रश रूप भाषात्रय में प्रबन्ध रचना करने में निपुण बतलाया गया है। बुल्हर ने इस ताम्रपट-लेख को जाली बतलाया है और वे उसे वाद का मानते हैं। हो सकता है कि यहलेख बाद में उत्कीर्ण किया गया हो, किन्तु घटनाक्रम तो उसी काल का है। भले ही इस लेख के काल में सौ, पचास वर्ष का फर्क हो सकता है, पर उसकी बारीकी से जाँच करना अभी आवश्यक है।
भाषा शास्त्र के विद्वान अपभ्रश साहित्य का प्रारम्भ ५०० या ६०० ईस्वी से मानते हैं किंतु अपभ्रंश भाषा के सम्बन्ध में वैयाकरणों ने जो लक्षण निर्दिष्ट किये हैं, उनके कुछ उदाहरण हमें अशोक के शिलालेखों में दृष्टिगत होते हैं। उनमें संयुक्त र और उकारान्त पदों का प्रयोग भी उपलब्ध होता है । इसी तरह 'धम्मपद' में भी अनेक शब्दों के अपभ्रंग रूप दृष्टिगत होते हैं। ललितविस्तर और महायान सम्प्रदाय के अन्य वौद्ध ग्रंथों की संस्कृत में भी अपभ्रंश रूप उपलब्ध होते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान तारानाथ ने यह स्पष्ट उल्लेखित किया है कि.-'वौद्धों के सम्मितीय समुदाय के त्रिपिटक के संस्करण पाली संस्कृत और प्राकृत के अतिरिक्त अपभ्रश में भी लिखे गये हैं।' इससे यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि नाट्यकार भरत के समय और उसके बाद अपभ्रंश बीज रूप से विद्यमान थी और उसका अर्थ शब्द का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप उस काल में देशवासियों के व्यवहार में प्रयुक्त होता था।
इस तरह अपभ्रश का उत्तरोत्तर विकास होता गया और विक्रम की ८वीं शताब्दी में तो अपभ्रंश का काव्यरूप बहुत प्रसिद्ध और लोकरंजक हो चुका था । विक्रम की हवीं शताब्दी के विद्वान उद्योतन सूरि ने अपनी कुदलयमाला में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की तुलना करते हुए संस्कृत की अपेक्षा अपभ्रंश की महत्ता का उल्लेख किया है। जिससे अपभ्रंश की उस समय की लोकप्रियता का सहज ही परिज्ञान हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि-'संस्कृत अपने बड़े-बड़े समासों, निपातों, उपसर्गों, विभक्तियों और लिङ्गों की दुर्गमता के कारण दुर्जन हृदय के समान विषम है। प्राकृत समस्तकला-कलापों की मालारूप जल कल्लोलों से संकुल लोक वृत्तान्त रूपी महोदधि, महापुरुषों के मुख से निकली हुई अमृतधारा
तथा एक एक क्रम से वर्ण और पदों के संघटन से नाना प्रकार की रचनाओं के योग्य होते हुए भी सज्जन वचन के समान सुख-संगम है और अपभ्रंश वह काव्य-शैली है जिसमें दोनों भाषाओं (संस्कृत
५. आभीरोक्तिः शावरी स्यात् ...... नाट्यशास्त्र १८-४४ । ६. संस्कृतप्राकृतापभ्रंशभाषात्रय प्रतिबद्ध प्रबन्ध रचना निपुणान्तःकरणः ।
-इण्डियन् एण्टीक्वेरी भा० १० पृ० २८० ७. देखो, त्रिपिटिक के सम्मितीय संस्करण । ८. देखो वलयमाला।