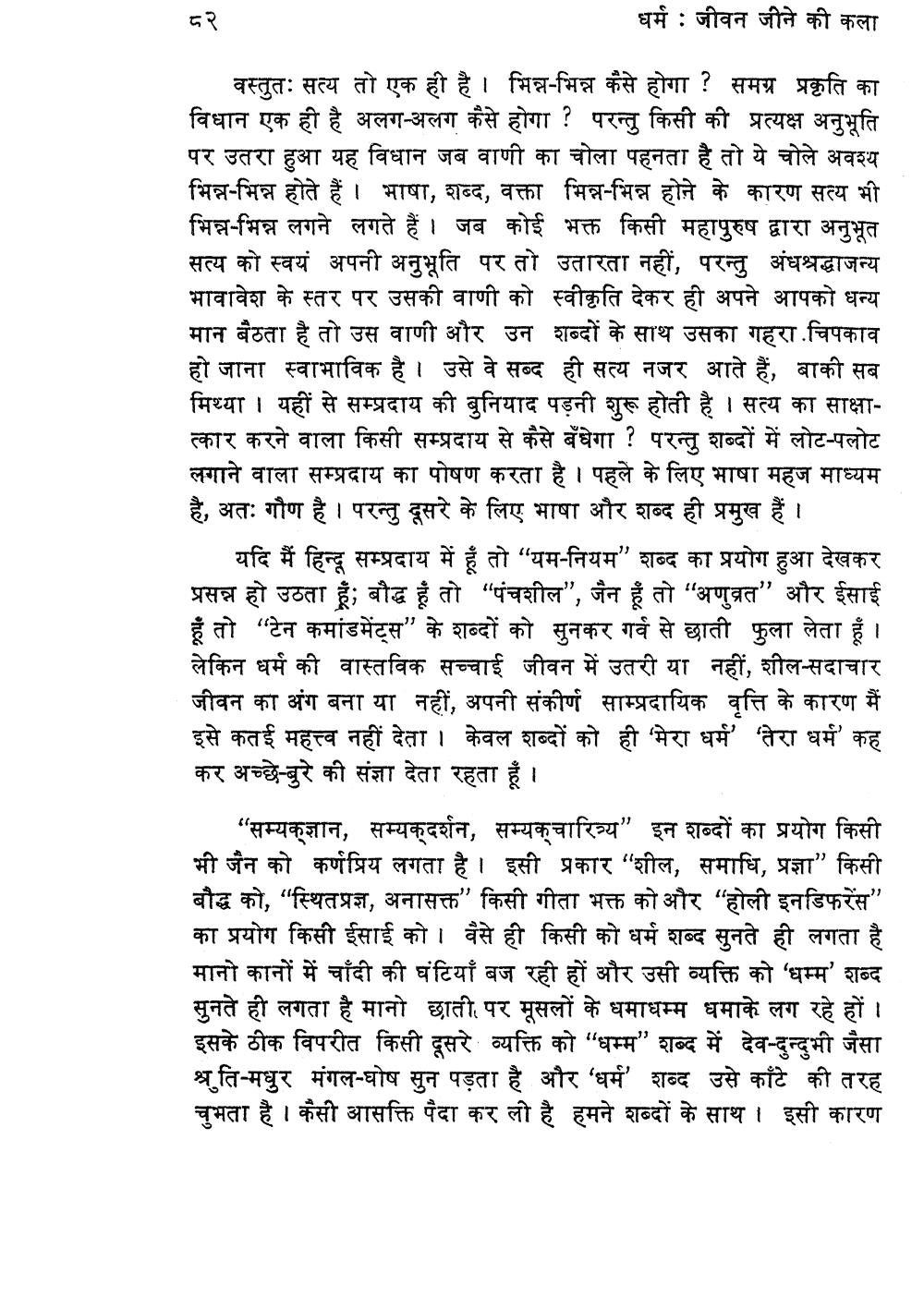________________
८२
धर्म : जीवन जीने की कला
वस्तुतः सत्य तो एक ही है। भिन्न-भिन्न कैसे होगा ? समग्र प्रकृति का विधान एक ही है अलग-अलग कैसे होगा ? परन्तु किसी की प्रत्यक्ष अनुभूति पर उतरा हुआ यह विधान जब वाणी का चोला पहनता है तो ये चोले अवश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। भाषा, शब्द, वक्ता भिन्न-भिन्न होने के कारण सत्य भी भिन्न-भिन्न लगने लगते हैं। जब कोई भक्त किसी महापुरुष द्वारा अनुभूत सत्य को स्वयं अपनी अनुभूति पर तो उतारता नहीं, परन्तु अंधश्रद्धाजन्य भावावेश के स्तर पर उसकी वाणी को स्वीकृति देकर ही अपने आपको धन्य मान बैठता है तो उस वाणी और उन शब्दों के साथ उसका गहरा.चिपकाव हो जाना स्वाभाविक है। उसे वे सब्द ही सत्य नजर आते हैं, बाकी सब मिथ्या। यहीं से सम्प्रदाय की बुनियाद पड़नी शुरू होती है । सत्य का साक्षात्कार करने वाला किसी सम्प्रदाय से कैसे बँधेगा? परन्तु शब्दों में लोट-पलोट लगाने वाला सम्प्रदाय का पोषण करता है । पहले के लिए भाषा महज माध्यम है, अतः गौण है । परन्तु दूसरे के लिए भाषा और शब्द ही प्रमुख हैं। __यदि मैं हिन्दू सम्प्रदाय में हैं तो “यम-नियम" शब्द का प्रयोग हुआ देखकर प्रसन्न हो उठता हूँ; बौद्ध हूँ तो "पंचशील", जैन हूँ तो "अणुव्रत' और ईसाई हूँ तो "टेन कमांडमेंट्स" के शब्दों को सुनकर गर्व से छाती फुला लेता हूँ। लेकिन धर्म की वास्तविक सच्चाई जीवन में उतरी या नहीं, शील-सदाचार जीवन का अंग बना या नहीं, अपनी संकीर्ण साम्प्रदायिक वृत्ति के कारण मैं इसे कतई महत्त्व नहीं देता। केवल शब्दों को ही 'मेरा धर्म' 'तेरा धर्म' कह कर अच्छे-बुरे की संज्ञा देता रहता हूँ। ___ “सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य" इन शब्दों का प्रयोग किसी भी जैन को कर्णप्रिय लगता है। इसी प्रकार "शील, समाधि, प्रज्ञा" किसी बौद्ध को, "स्थितप्रज्ञ, अनासक्त” किसी गीता भक्त को और "होली इनडिफरेंस" का प्रयोग किसी ईसाई को। वैसे ही किसी को धर्म शब्द सुनते ही लगता है मानो कानों में चाँदी की घंटियाँ बज रही हों और उसी व्यक्ति को 'धम्म' शब्द सुनते ही लगता है मानो छाती पर मूसलों के धमाधम्म धमाके लग रहे हों। इसके ठीक विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति को "धम्म” शब्द में देव-दुन्दुभी जैसा श्रुति-मधुर मंगल-घोष सुन पड़ता है और 'धर्म' शब्द उसे काँटे की तरह चुभता है । कैसी आसक्ति पैदा कर ली है हमने शब्दों के साथ। इसी कारण