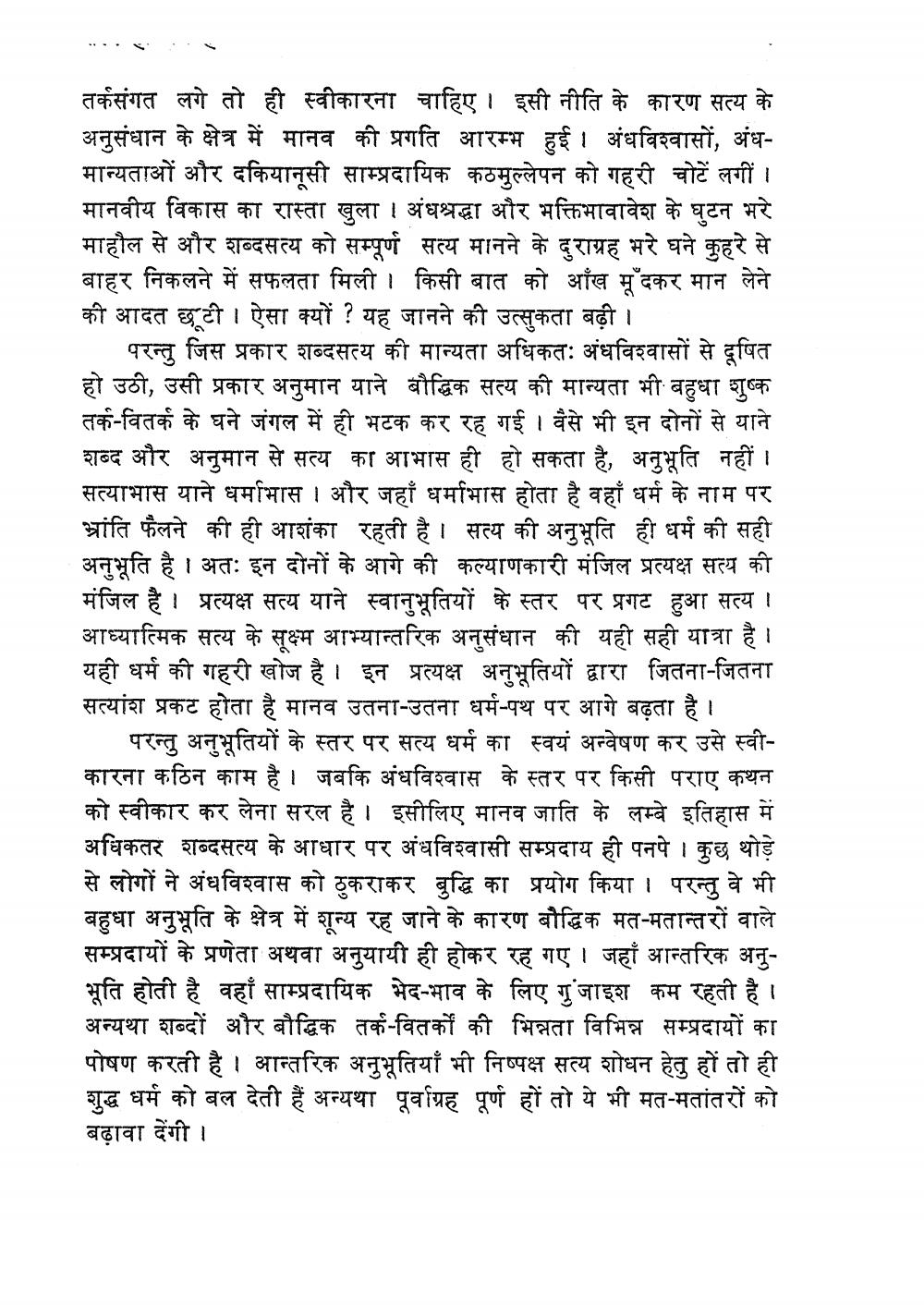________________
तर्कसंगत लगे तो ही स्वीकारना चाहिए। इसी नीति के कारण सत्य के अनुसंधान के क्षेत्र में मानव की प्रगति आरम्भ हुई। अंधविश्वासों, अंधमान्यताओं और दकियानूसी साम्प्रदायिक कठमुल्लेपन को गहरी चोटें लगीं। मानवीय विकास का रास्ता खुला । अंधश्रद्धा और भक्तिभावावेश के घुटन भरे माहौल से और शब्दसत्य को सम्पूर्ण सत्य मानने के दुराग्रह भरे घने कुहरे से बाहर निकलने में सफलता मिली। किसी बात को आँख मूंदकर मान लेने की आदत छटी । ऐसा क्यों ? यह जानने की उत्सुकता बढ़ी।
परन्तु जिस प्रकार शब्दसत्य की मान्यता अधिकतः अंधविश्वासों से दूषित हो उठी, उसी प्रकार अनुमान याने बौद्धिक सत्य की मान्यता भी बहुधा शुष्क तर्क-वितर्क के घने जंगल में ही भटक कर रह गई । वैसे भी इन दोनों से याने शब्द और अनुमान से सत्य का आभास ही हो सकता है, अनुभूति नहीं । सत्याभास याने धर्माभास । और जहाँ धर्माभास होता है वहाँ धर्म के नाम पर भ्रांति फैलने की ही आशंका रहती है। सत्य की अनुभूति ही धर्म की सही अनुभूति है । अतः इन दोनों के आगे की कल्याणकारी मंजिल प्रत्यक्ष सत्य की मंजिल है। प्रत्यक्ष सत्य याने स्वानुभूतियों के स्तर पर प्रगट हुआ सत्य । आध्यात्मिक सत्य के सूक्ष्म आभ्यान्तरिक अनुसंधान की यही सही यात्रा है । यही धर्म की गहरी खोज है। इन प्रत्यक्ष अनुभूतियों द्वारा जितना-जितना सत्यांश प्रकट होता है मानव उतना-उतना धर्म-पथ पर आगे बढ़ता है।
परन्तु अनुभूतियों के स्तर पर सत्य धर्म का स्वयं अन्वेषण कर उसे स्वीकारना कठिन काम है। जबकि अंधविश्वास के स्तर पर किसी पराए कथन को स्वीकार कर लेना सरल है। इसीलिए मानव जाति के लम्बे इतिहास में अधिकतर शब्दसत्य के आधार पर अंधविश्वासी सम्प्रदाय ही पनपे । कुछ थोड़े से लोगों ने अंधविश्वास को ठुकराकर बुद्धि का प्रयोग किया । परन्तु वे भी बहुधा अनुभूति के क्षेत्र में शून्य रह जाने के कारण बौद्धिक मत-मतान्तरों वाले सम्प्रदायों के प्रणेता अथवा अनुयायी ही होकर रह गए । जहाँ आन्तरिक अनुभूति होती है वहाँ साम्प्रदायिक भेद-भाव के लिए गुजाइश कम रहती है । अन्यथा शब्दों और बौद्धिक तर्क-वितर्कों की भिन्नता विभिन्न सम्प्रदायों का पोषण करती है । आन्तरिक अनुभूतियाँ भी निष्पक्ष सत्य शोधन हेतु हों तो ही शुद्ध धर्म को बल देती हैं अन्यथा पूर्वाग्रह पूर्ण हों तो ये भी मत-मतांतरों को बढ़ावा देंगी।