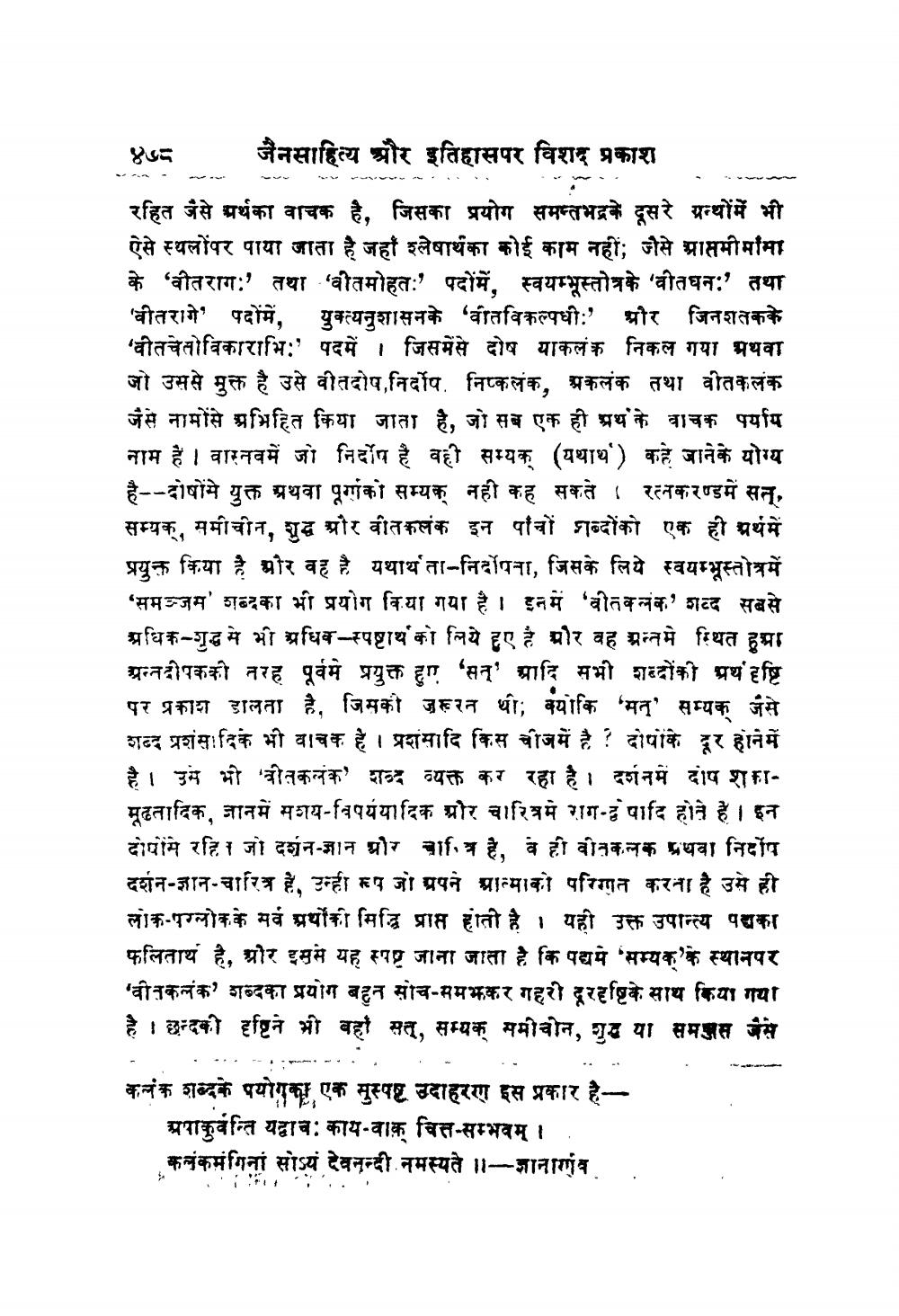________________ 478 जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश रहित जैसे अर्थका वाचक है, जिसका प्रयोग समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंमें भी ऐसे स्थलोंपर पाया जाता है जहाँ श्लेषार्थका कोई काम नहीं; जैसे प्राप्तमीमामा के 'वीतराग:' तथा 'वीतमोहतः' पदोंमें, स्वयम्भूस्तोत्रके 'वीतघन:' तथा 'वीतरागे' पदोंमें, युक्त्यनुशासनके 'वीतविकल्पधीः' और जिनशतकके 'वीतचेतोविकाराभिः' पदमें / जिसमें से दोष याकलंक निकल गया अथवा जो उससे मुक्त है उसे वीतदोष,निर्दोप. निष्कलंक, अकलंक तथा वीतकलंक जैसे नामोंसे अभिहित किया जाता है, जो सब एक ही प्रथके वाचक पर्याय नाम हैं / वास्तव में जो निर्दोष है वही सम्यक् (यथा') कहे जाने के योग्य है--दोषोंमे युक्त अथवा पूर्गको सम्यक् नही कह सकते / रत्नकरण्ड में सत्, सम्यक्, ममीचीन, शुद्ध और वीतकलंक इन पांचों शब्दोंको एक ही अर्थमें प्रयुक्त किया है और वह है यथार्थता-निर्दोपना, जिसके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमें 'समञ्जम' शब्दका भी प्रयोग किया गया है। इनमें 'वीतकलंक' शब्द सबसे अधिक-शुद्ध मे भी अधिक स्पष्टार्थ को लिये हुए है और वह अन्त मे स्थित हमा अन्तदीपककी तरह पूर्वमे प्रयुक्त हुए. 'सत्' आदि सभी शब्दोंकी प्रथहष्टि पर प्रकाश डालता है, जिसकी जरूरत थी; क्योकि 'मत' सम्यक् जसे शब्द प्रशंसादिक भी वाचक है / प्रशंसादि किस चीजमें है ? दोपोंके दूर होने में है। उसे भी 'बीतकलंक' शब्द व्यक्त कर रहा है। दर्शनमें दोष शकामूढतादिक, ज्ञानमें मशय-विपर्ययादिक और चारित्रमे राग-द्वंपादि होते है। इन दोषोंमे रहिर जो दर्शन-ज्ञान और चात्रि है, वे ही बीतकलक प्रथवा निदोप दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, उन्ही रूप जो अपने प्रात्माको परिणत करता है उसे ही लोक-परलोक के मर्व अर्थोकी मिद्धि प्राप्त होती है / यही उक्त उपान्त्य पद्यका फलितार्थ है, और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पद्यमे 'सम्यक् के स्थानपर 'वीतकलंक' शब्दका प्रयोग बहुत सोच-समझकर गहरी दूरदृष्टिके साथ किया गया है / छन्दकी दृष्टिने भी बहाँ सत्, सम्यक् ममीचीन, शुद्ध या समक्षस जैसे कलंक शब्दके पयोगका एक सुस्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है अपाकुर्वन्ति यद्वाच: काय-वाक् वित्त-सम्भवम् / कलंकमंगिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ।।-ज्ञानार्णव .