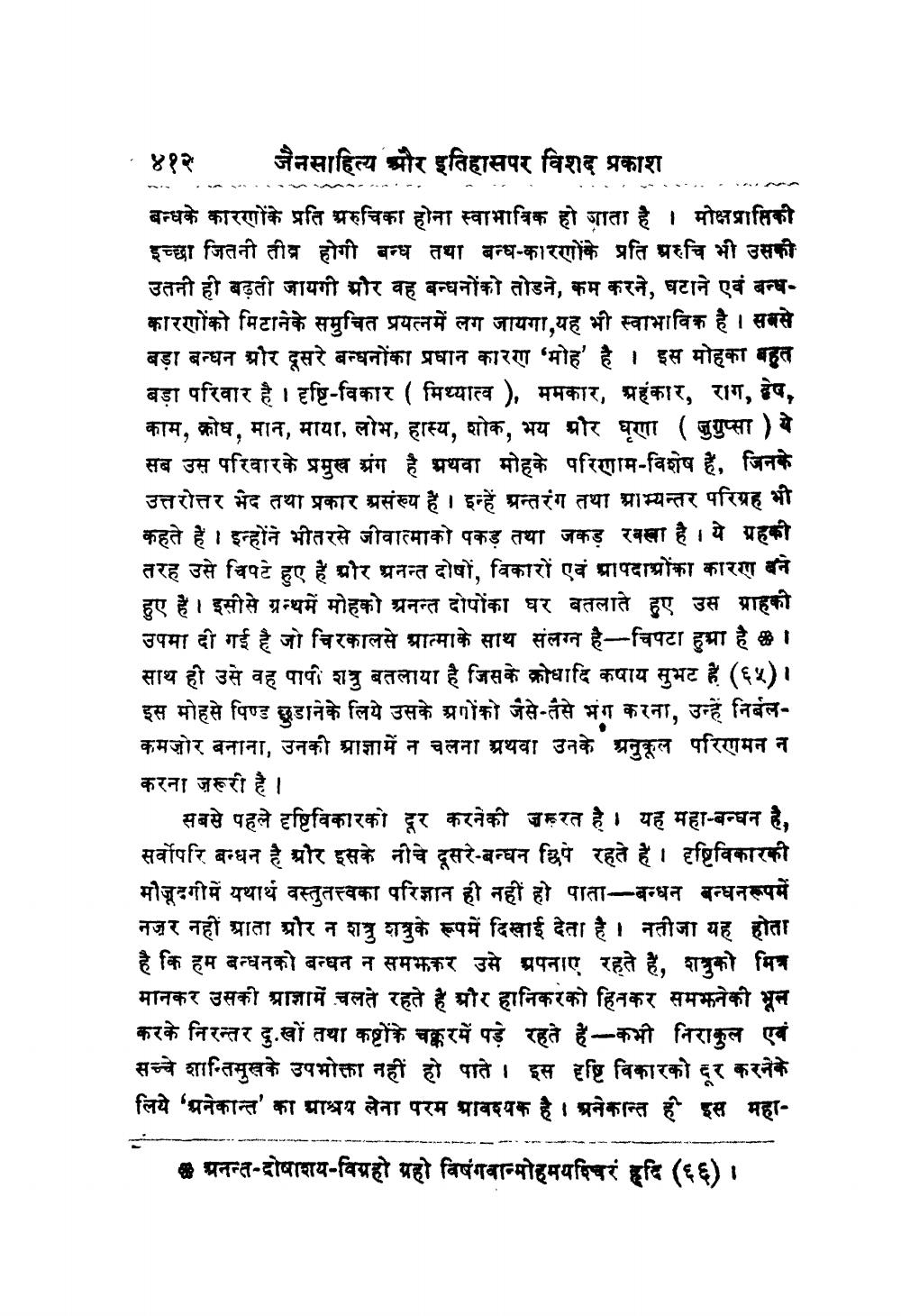________________ * 412 जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश बन्धके कारणोंके प्रति अरुचिका होना स्वाभाविक हो जाता है / मोक्षप्रासिकी इच्छा जितनी तीव्र होगी बन्ध तथा बन्ध-कारणोंके प्रति अरुचि भी उसकी उतनी ही बढ़ती जायगी और वह बन्धनोंको तोडने, कम करने, घटाने एवं बन्धकारणोंको मिटानेके समुचित प्रयत्नमें लग जायगा,यह भी स्वाभाविक है / सबसे बड़ा बन्धन और दूसरे बन्धनोंका प्रधान कारण 'मोह' है / इस मोहका बहुत बड़ा परिवार है / दृष्टि-विकार ( मिथ्यात्व ), ममकार, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय और घृणा ( जुगुप्सा ) ये सब उस परिवार के प्रमुख अंग है अथवा मोहके परिणाम-विशेष हैं, जिनके उत्तरोत्तर भेद तथा प्रकार असंख्य हैं। इन्हें अन्तरंग तथा प्राभ्यन्तर परिग्रह भी कहते हैं / इन्होंने भीतरसे जीवात्माको पकड़ तथा जकड़ रक्खा है / ये ग्रहकी तरह उसे चिपटे हुए हैं और अनन्त दोषों, विकारों एवं प्रापदाओंका कारण बने हुए हैं। इसीसे ग्रन्थमें मोहको अनन्त दोपोंका घर बतलाते हुए उस ग्राहको उपमा दी गई है जो चिरकालसे प्रात्माके साथ संलग्न है-चिपटा हुमा है / साथ ही उसे वह पापी शत्रु बतलाया है जिसके क्रोधादि कषाय सुभट है (65) / इस मोहसे पिण्ड छुडाने के लिये उसके अगोंको जैसे-तैसे भंग करना, उन्हें निर्बलकमजोर बनाना, उनकी प्राज्ञामें न चलना अथवा उनके अनुकूल परिणमन न करना ज़रूरी है। सबसे पहले दृष्टिविकारको दूर करनेकी जरूरत है। यह महा-बन्धन है, सर्वोपरि बन्धन है और इसके नीचे दूसरे-बन्धन छिपे रहते हैं। दृष्टिविकारकी मौजूदगीमें यथार्थ वस्तुतत्त्वका परिज्ञान ही नहीं हो पाता-बन्धन बन्धनरूपमें नज़र नहीं पाता और न शत्रु शत्रुके रूपमें दिखाई देता है। नतीजा यह होता है कि हम बन्धनको बन्धन न समझकर उसे अपनाए रहते हैं, शत्रुको मित्र मानकर उसकी प्राज्ञामें चलते रहते है और हानिकरको हितकर समझनेकी भून करके निरन्तर दु.खों तथा कष्टोंके चक्कर में पड़े रहते है-कभी निराकुल एवं सच्चे शान्तिसुखके उपभोक्ता नहीं हो पाते। इस दृष्टि विकारको दूर करनेके लिये 'अनेकान्त' का माश्रय लेना परम पावश्यक है / अनेकान्त ही इस महा -- ----- - अनन्त-दोषाशय-विग्रहो ग्रहो विषंगवान्मोहमयश्चिरं हृदि (66) /