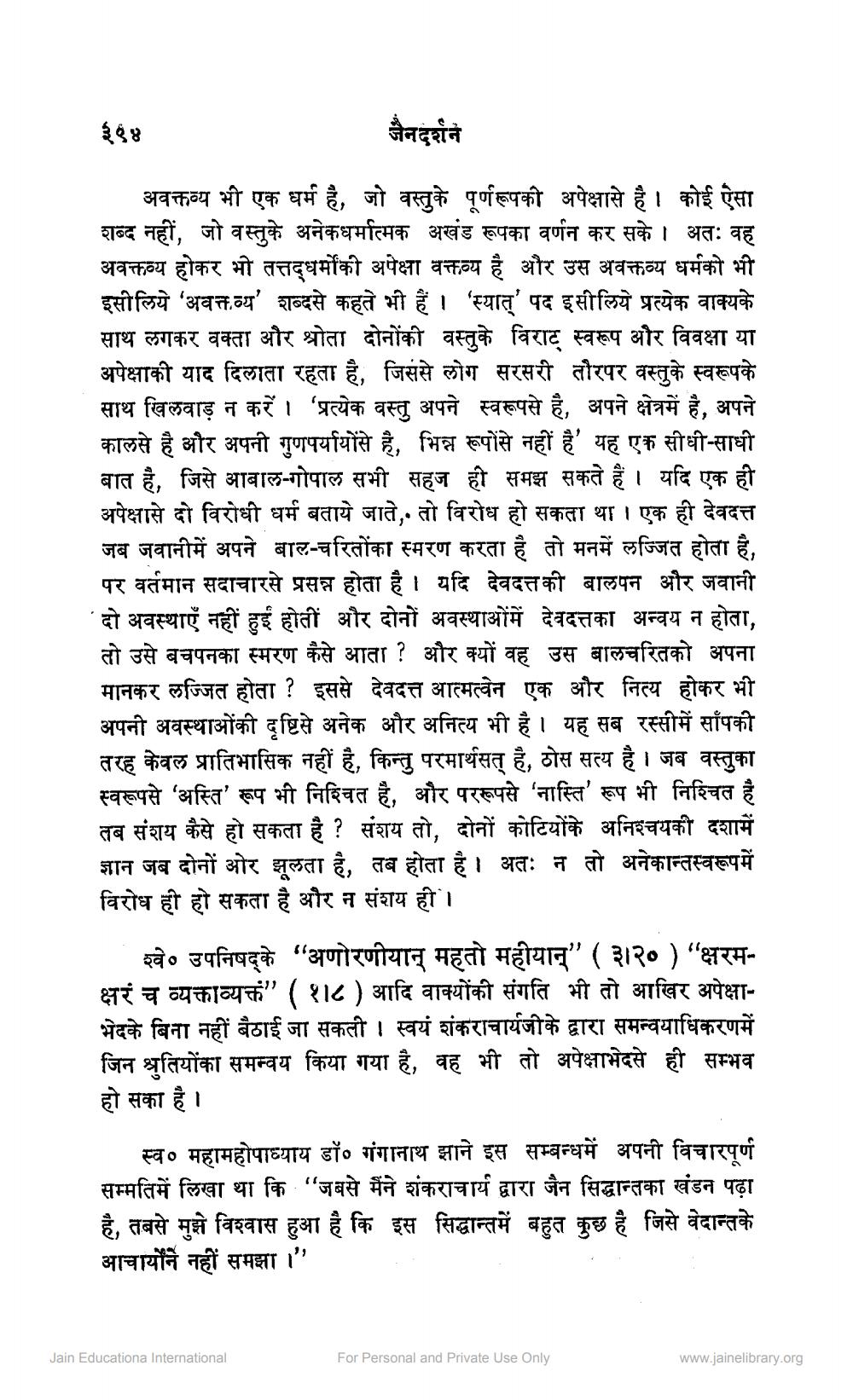________________ 394 जैनदर्शने अवक्तव्य भी एक धर्म है, जो वस्तुके पूर्णरूपकी अपेक्षासे है। कोई ऐसा शब्द नहीं, जो वस्तुके अनेकधर्मात्मक अखंड रूपका वर्णन कर सके। अतः वह अवक्तव्य होकर भी तत्तद्धर्मोकी अपेक्षा वक्तव्य है और उस अवक्तव्य धर्मको भी इसीलिये 'अवक्तव्य' शब्दसे कहते भी हैं / 'स्यात्' पद इसीलिये प्रत्येक वाक्यके साथ लगकर वक्ता और श्रोता दोनोंकी वस्तुके विराट् स्वरूप और विवक्षा या अपेक्षाकी याद दिलाता रहता है, जिससे लोग सरसरी तौरपर वस्तुके स्वरूपके साथ खिलवाड़ न करें। 'प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपसे है, अपने क्षेत्रमें है, अपने कालसे है और अपनी गुणपर्यायोंसे है, भिन्न रूपोंसे नहीं है' यह एक सीधी-साधी बात है, जिसे आबाल-गोपाल सभी सहज ही समझ सकते हैं / यदि एक ही अपेक्षासे दो विरोधी धर्म बताये जाते, तो विरोध हो सकता था। एक ही देवदत्त जब जवानीमें अपने बाल-चरितोंका स्मरण करता है तो मनमें लज्जित होता है, पर वर्तमान सदाचारसे प्रसन्न होता है। यदि देवदत्त की बालपन और जवानी दो अवस्थाएँ नहीं हुई होती और दोनों अवस्थाओंमें देवदत्तका अन्वय न होता, तो उसे बचपनका स्मरण कैसे आता ? और क्यों वह उस बालचरितको अपना मानकर लज्जित होता ? इससे देवदत्त आत्मत्वेन एक और नित्य होकर भी अपनी अवस्थाओंकी दृष्टिसे अनेक और अनित्य भी है। यह सब रस्सीमें साँपकी तरह केवल प्रातिभासिक नहीं है, किन्तु परमार्थसत् है, ठोस सत्य है। जब वस्तुका स्वरूपसे 'अस्ति' रूप भी निश्चित है, और पररूपसे 'नास्ति' रूप भी निश्चित है तब संशय कैसे हो सकता है ? संशय तो, दोनों कोटियोंके अनिश्चयकी दशामें ज्ञान जब दोनों ओर झूलता है, तब होता है। अतः न तो अनेकान्तस्वरूपमें विरोध ही हो सकता है और न संशय ही। ___ श्वे. उपनिषद्के "अणोरणीयान् महतो महीयान्" ( 3 / 20 ) "क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं" ( 118) आदि वाक्योंकी संगति भी तो आखिर अपेक्षाभेदके बिना नहीं बैठाई जा सकती। स्वयं शंकराचार्यजीके द्वारा समन्वयाधिकरणमें जिन श्रुतियोंका समन्वय किया गया है, वह भी तो अपेक्षाभेदसे ही सम्भव हो सका है। ___ स्व० महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झाने इस सम्बन्धमें अपनी विचारपूर्ण सम्मतिमें लिखा था कि “जबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्योंने नहीं समझा।" Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.org