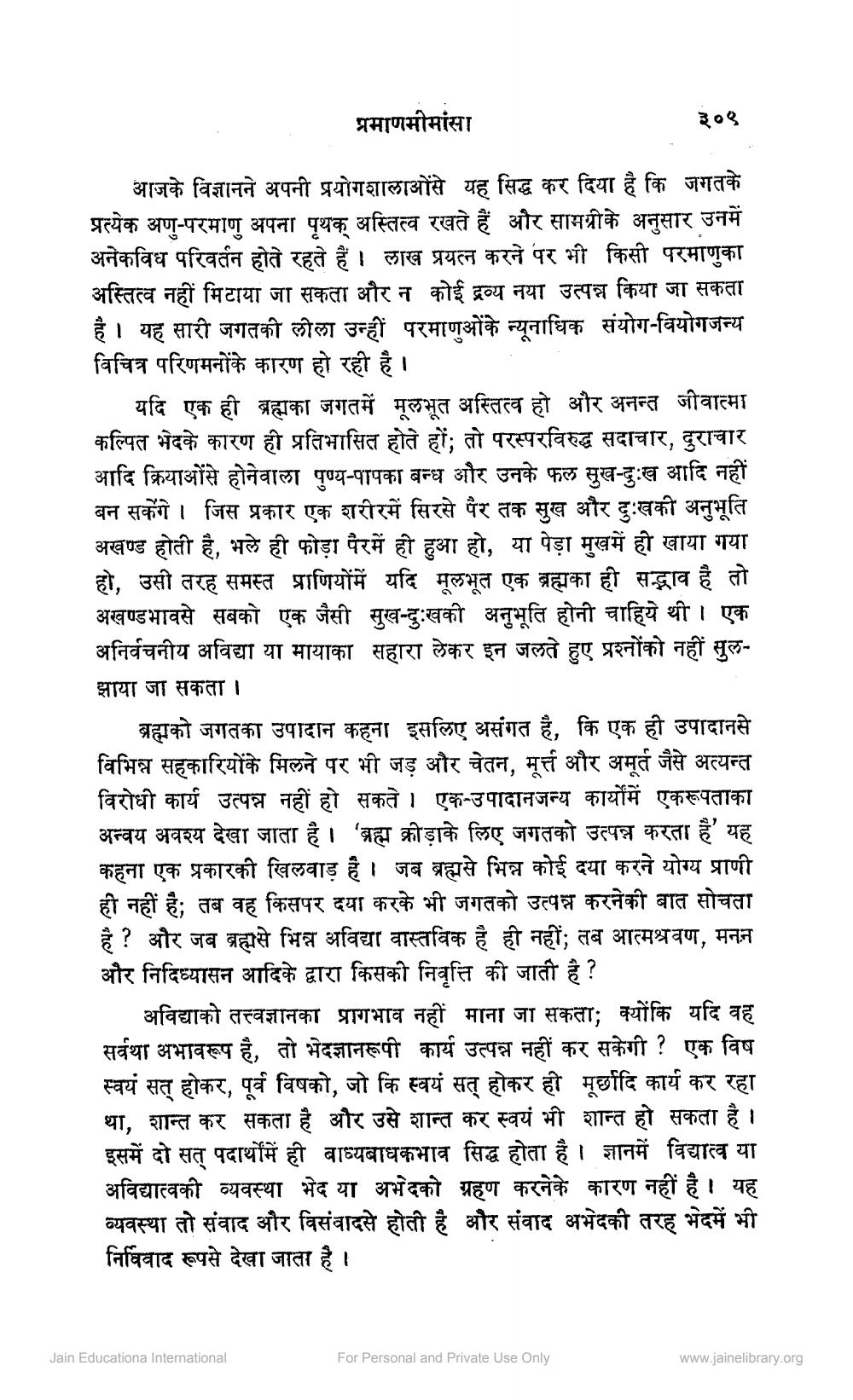________________ प्रमाणमीमांसा 309 आजके विज्ञानने अपनी प्रयोगशालाओंसे यह सिद्ध कर दिया है कि जगतके प्रत्येक अणु-परमाणु अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं और सामग्रीके अनुसार उनमें अनेकविध परिवर्तन होते रहते हैं। लाख प्रयत्न करने पर भी किसी परमाणुका अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता और न कोई द्रव्य नया उत्पन्न किया जा सकता है। यह सारी जगतकी लीला उन्हीं परमाणुओंके न्यूनाधिक संयोग-वियोगजन्य विचित्र परिणमनोंके कारण हो रही है। यदि एक ही ब्रह्मका जगतमें मूलभूत अस्तित्व हो और अनन्त जीवात्मा कल्पित भेदके कारण ही प्रतिभासित होते हों; तो परस्परविरुद्ध सदाचार, दुराचार आदि क्रियाओंसे होनेवाला पुण्य-पापका बन्ध और उनके फल सुख-दुःख आदि नहीं बन सकेंगे। जिस प्रकार एक शरीरमें सिरसे पैर तक सुख और दुःखकी अनुभूति अखण्ड होती है, भले ही फोड़ा पैरमें ही हुआ हो, या पेड़ा मुखमें ही खाया गया हो, उसी तरह समस्त प्राणियोंमें यदि मूलभूत एक ब्रह्मका ही सद्भाव है तो अखण्डभावसे सबको एक जैसी सुख-दुःखकी अनुभूति होनी चाहिये थी। एक अनिर्वचनीय अविद्या या मायाका सहारा लेकर इन जलते हुए प्रश्नोंको नहीं सुलझाया जा सकता। ब्रह्मको जगतका उपादान कहना इसलिए असंगत है, कि एक ही उपादानसे विभिन्न सहकारियोंके मिलने पर भी जड़ और चेतन, मूर्त और अमूर्त जैसे अत्यन्त विरोधी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। एक-उपादानजन्य कार्योंमें एकरूपताका अन्वय अवश्य देखा जाता है। 'ब्रह्म क्रीड़ाके लिए जगतको उत्पन्न करता है यह कहना एक प्रकारकी खिलवाड़ है। जब ब्रह्मसे भिन्न कोई दया करने योग्य प्राणी ही नहीं है; तब वह किसपर दया करके भी जगतको उत्पन्न करनेकी बात सोचता है ? और जब ब्रह्मसे भिन्न अविद्या वास्तविक है ही नहीं; तब आत्मश्रवण, मनन और निदिध्यासन आदिके द्वारा किसकी निवृत्ति की जाती है ? ___ अविद्याको तत्त्वज्ञानका प्रागभाव नहीं माना जा सकता; क्योंकि यदि वह सर्वथा अभावरूप है, तो भेदज्ञानरूपी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकेगी ? एक विष स्वयं सत् होकर, पूर्व विषको, जो कि स्वयं सत् होकर ही मुर्छादि कार्य कर रहा था, शान्त कर सकता है और उसे शान्त कर स्वयं भी शान्त हो सकता है। इसमें दो सत् पदार्थों में ही बाध्यबाधकभाव सिद्ध होता है। ज्ञानमें विद्यात्व या अविद्यात्वकी व्यवस्था भेद या अभेदको ग्रहण करनेके कारण नहीं है। यह व्यवस्था तो संवाद और विसंवादसे होती है और संवाद अभेदकी तरह भेदमें भी निर्विवाद रूपसे देखा जाता है / Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.org