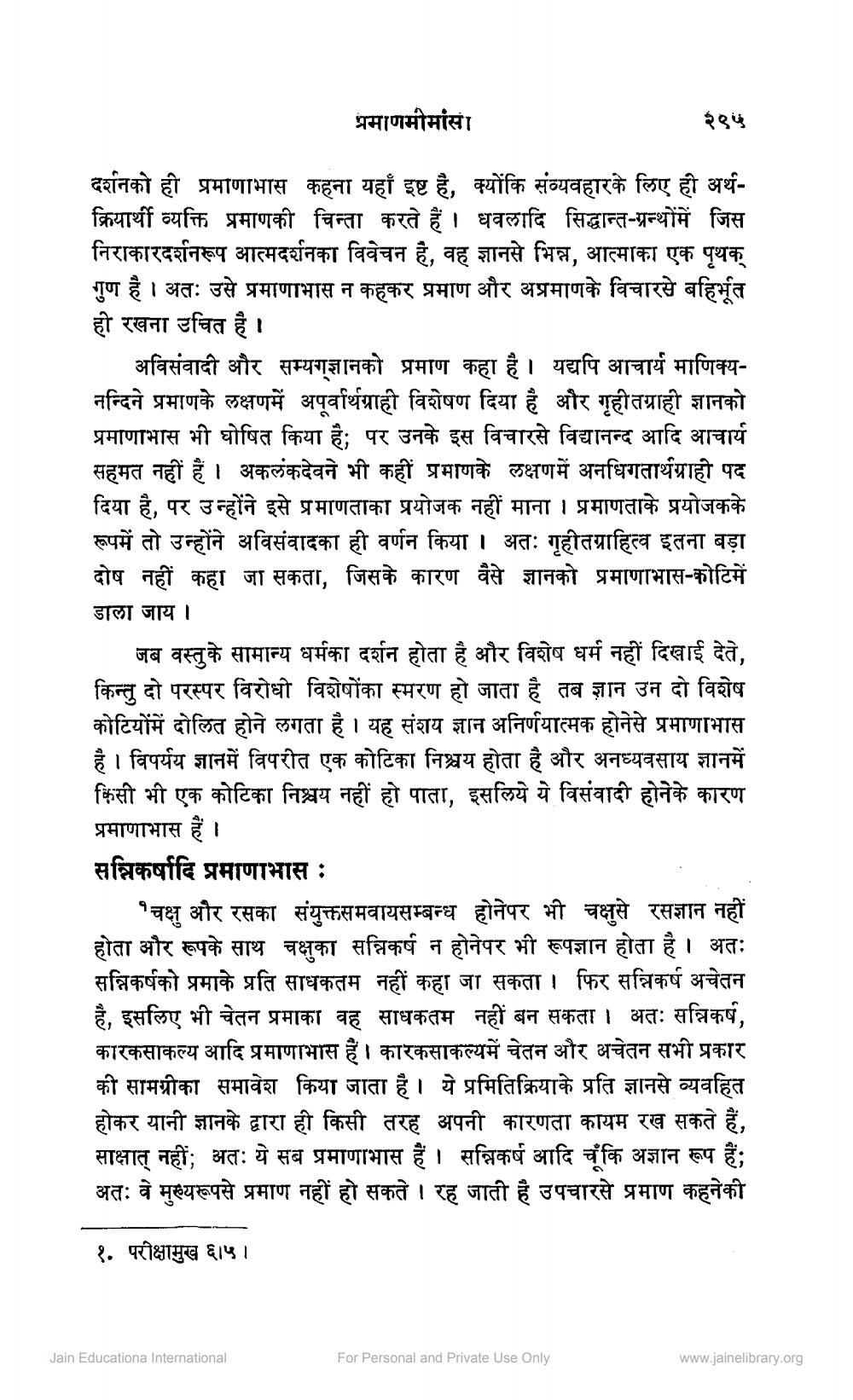________________ प्रमाणमीमांसा 295 दर्शनको ही प्रमाणाभास कहना यहाँ इष्ट है, क्योंकि संव्यवहारके लिए ही अर्थक्रियार्थी व्यक्ति प्रमाणकी चिन्ता करते हैं। धवलादि सिद्धान्त-ग्रन्थोंमें जिस निराकारदर्शनरूप आत्मदर्शनका विवेचन है, वह ज्ञानसे भिन्न, आत्माका एक पृथक् गुण है / अतः उसे प्रमाणाभास न कहकर प्रमाण और अप्रमाणके विचारसे बहिर्भूत ही रखना उचित है। अविसंवादी और सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहा है। यद्यपि आचार्य माणिक्यनन्दिने प्रमाणके लक्षणमें अपूर्वार्थग्राही विशेषण दिया है और गृहीतग्राही ज्ञानको प्रमाणाभास भी घोषित किया है; पर उनके इस विचारसे विद्यानन्द आदि आचार्य सहमत नहीं हैं / अकलंकदेवने भी कहीं प्रमाणके लक्षणमें अनधिगतार्थग्राही पद दिया है, पर उन्होंने इसे प्रमाणताका प्रयोजक नहीं माना / प्रमाणताके प्रयोजकके रूपमें तो उन्होंने अविसंवादका ही वर्णन किया / अतः गृहीतग्राहित्व इतना बड़ा दोष नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण वैसे ज्ञानको प्रमाणाभास-कोटिमें डाला जाय। ___ जब वस्तु के सामान्य धर्मका दर्शन होता है और विशेष धर्म नहीं दिखाई देते, किन्तु दो परस्पर विरोधी विशेषोंका स्मरण हो जाता है तब ज्ञान उन दो विशेष कोटियोंमें दोलित होने लगता है / यह संशय ज्ञान अनिर्णयात्मक होनेसे प्रमाणाभास है। विपर्यय ज्ञानमें विपरीत एक कोटिका निश्चय होता है और अनध्यवसाय ज्ञानमें किसी भी एक कोटिका निश्चय नहीं हो पाता, इसलिये ये विसंवादी होनेके कारण प्रमाणाभास हैं। सन्निकर्षादि प्रमाणाभास : 'चक्षु और रसका संयुक्तसमवायसम्बन्ध होनेपर भी चक्षुसे रसज्ञान नहीं होता और रूपके साथ चक्षुका सन्निकर्ष न होनेपर भी रूपज्ञान होता है। अतः सन्निकर्षको प्रमाके प्रति साधकतम नहीं कहा जा सकता। फिर सन्निकर्ष अचेतन है, इसलिए भी चेतन प्रमाका वह साधकतम नहीं बन सकता। अतः सन्निकर्ष, कारकसाकल्य आदि प्रमाणाभास हैं। कारकसाकल्यमें चेतन और अचेतन सभी प्रकार की सामग्रीका समावेश किया जाता है। ये प्रमितिक्रियाके प्रति ज्ञानसे व्यवहित होकर यानी ज्ञानके द्वारा ही किसी तरह अपनी कारणता कायम रख सकते हैं, साक्षात् नहीं; अतः ये सब प्रमाणाभास हैं। सन्निकर्ष आदि चूंकि अज्ञान रूप हैं; अतः वे मुख्यरूपसे प्रमाण नहीं हो सकते / रह जाती है उपचारसे प्रमाण कहनेकी 1. परीक्षामुख 6 / 5 / Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.org