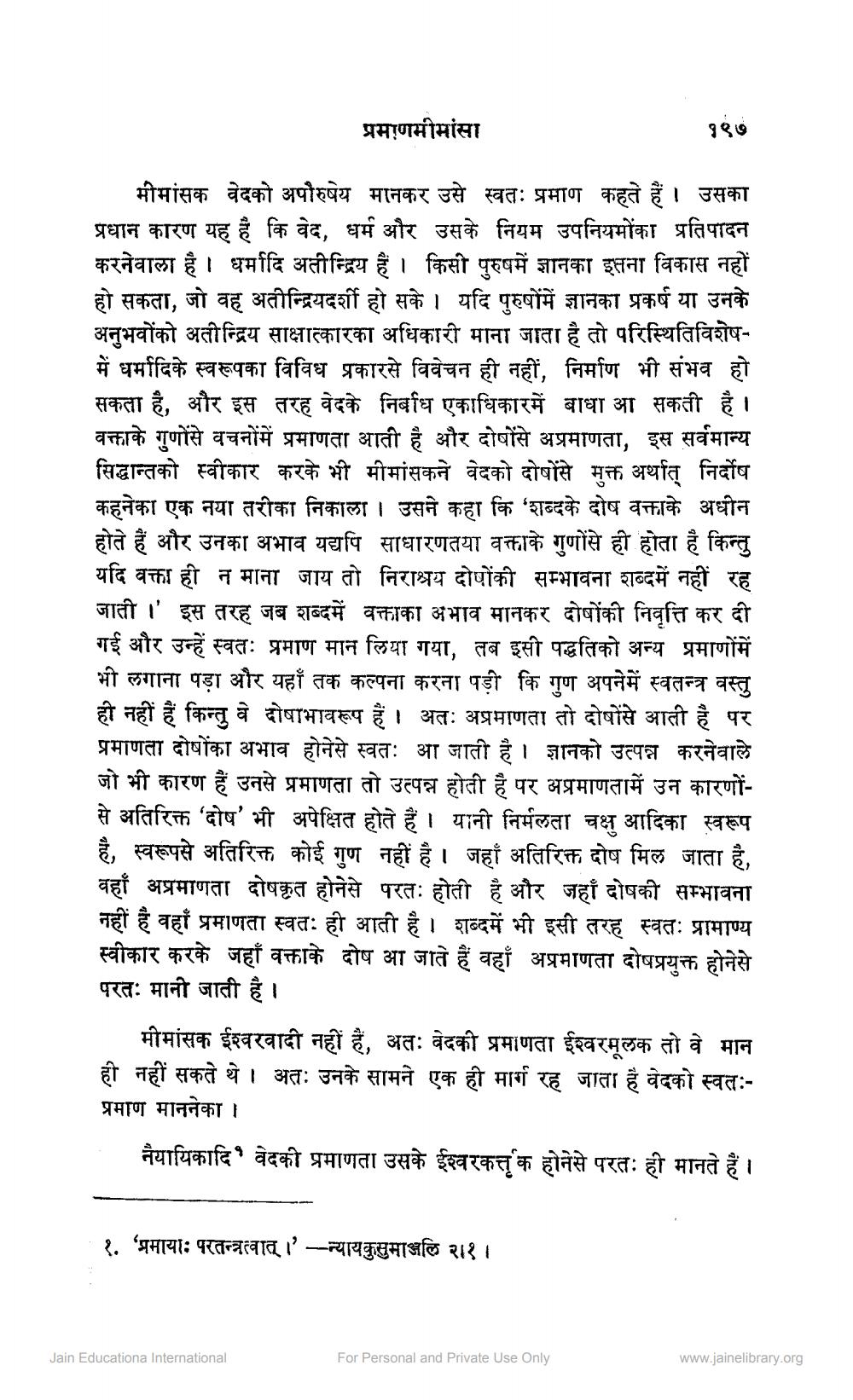________________ प्रमाणमीमांसा 197 मीमांसक वेदको अपौरुषेय मानकर उसे स्वतः प्रमाण कहते हैं। उसका प्रधान कारण यह है कि वेद, धर्म और उसके नियम उपनियमोंका प्रतिपादन करनेवाला है। धर्मादि अतीन्द्रिय हैं। किसी पुरुषमें ज्ञानका इतना विकास नहीं हो सकता, जो वह अतीन्द्रियदर्शी हो सके। यदि पुरुषोंमें ज्ञानका प्रकर्ष या उनके अनुभवोंको अतीन्द्रिय साक्षात्कारका अधिकारी माना जाता है तो परिस्थितिविशेषमें धर्मादिके स्वरूपका विविध प्रकारसे विवेचन ही नहीं, निर्माण भी संभव हो सकता है, और इस तरह वेदके निर्बाध एकाधिकारमें बाधा आ सकती है। वक्ताके गुणोंसे वचनोंमें प्रमाणता आती है और दोषोंसे अप्रमाणता, इस सर्वमान्य सिद्धान्तको स्वीकार करके भी मीमांसकने वेदको दोषोंसे मुक्त अर्थात् निर्दोष कहनेका एक नया तरीका निकाला। उसने कहा कि 'शब्दके दोष वक्ताके अधीन होते हैं और उनका अभाव यद्यपि साधारणतया वक्ताके गुणोंसे ही होता है किन्तु यदि वक्ता ही न माना जाय तो निराश्रय दोषोंकी सम्भावना शब्दमें नहीं रह जाती।' इस तरह जब शब्दमें वक्ताका अभाव मानकर दोषोंकी निवृत्ति कर दी गई और उन्हें स्वतः प्रमाण मान लिया गया, तब इसी पद्धतिको अन्य प्रमाणोंमें भी लगाना पड़ा और यहाँ तक कल्पना करना पड़ी कि गुण अपनेमें स्वतन्त्र वस्तु ही नहीं हैं किन्तु वे दोषाभावरूप हैं। अतः अप्रमाणता तो दोषोंसे आती है पर प्रमाणता दोषोंका अभाव होनेसे स्वतः आ जाती है। ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले जो भी कारण हैं उनसे प्रमाणता तो उत्पन्न होती है पर अप्रमाणतामें उन कारणोंसे अतिरिक्त 'दोष' भी अपेक्षित होते हैं। यानी निर्मलता चक्षु आदिका स्वरूप है, स्वरूपसे अतिरिक्त कोई गुण नहीं है। जहाँ अतिरिक्त दोष मिल जाता है, वहाँ अप्रमाणता दोषकृत होनेसे परतः होती है और जहाँ दोषकी सम्भावना नहीं है वहाँ प्रमाणता स्वतः ही आती है। शब्दमें भी इसी तरह स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करके जहाँ वक्ताके दोष आ जाते हैं वहाँ अप्रमाणता दोषप्रयुक्त होनेसे परतः मानी जाती है। ___ मीमांसक ईश्वरवादी नहीं हैं, अतः वेदकी प्रमाणता ईश्वरमूलक तो वे मान ही नहीं सकते थे। अतः उनके सामने एक ही मार्ग रह जाता है वेदको स्वतःप्रमाण माननेका। नैयायिकादि' वेदकी प्रमाणता उसके ईश्वरकर्तृक होनेसे परतः ही मानते हैं / 1. 'प्रमायाः परतन्त्रत्वात् / ' -न्यायकुसुमाञ्जलि 21 / Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.org