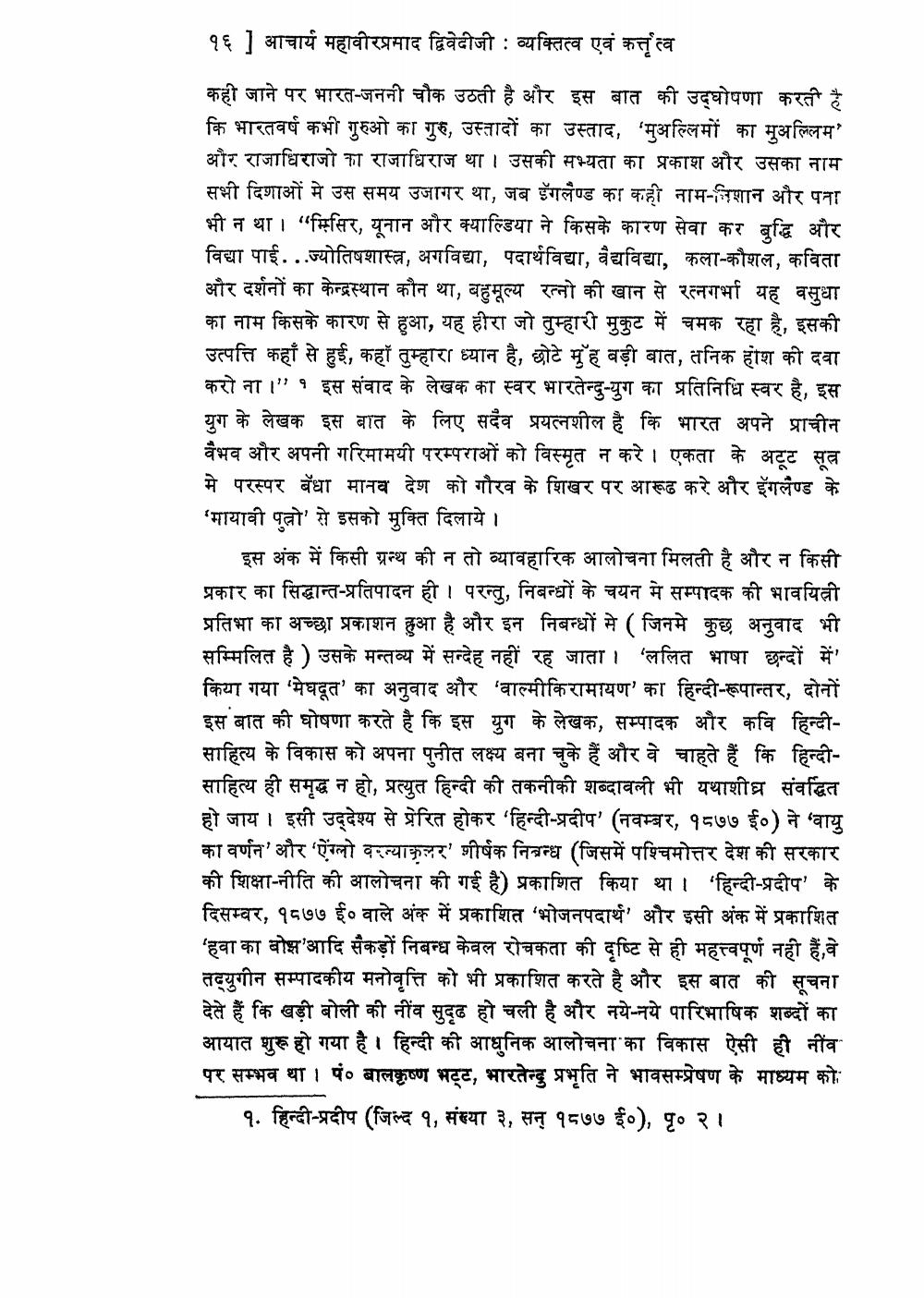________________
१६ ] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व
कही जाने पर भारत-जननी चौक उठती है और इस बात की उद्घोषणा करती है। कि भारतवर्ष कभी गुरुओ का गुरु, उस्तादों का उस्ताद, 'मुअल्लिमों का मुअल्लिम' और राजाधिराजो का राजाधिराज था । उसकी सभ्यता का प्रकाश और उसका नाम सभी दिशाओं में उस समय उजागर था, जब इंगलैण्ड का कही नाम-निशान और पता भी न था । "मिसिर, यूनान और क्याल्डिया ने किसके कारण सेवा कर बुद्धि और विद्या पाई... ज्योतिषशास्त्र, अगविद्या, पदार्थविद्या, वैद्यविद्या, कला-कौशल, कविता और दर्शनों का केन्द्रस्थान कौन था, बहुमूल्य रत्नों की खान से रत्नगर्भा यह वसुधा का नाम किसके कारण से हुआ, यह हीरा जो तुम्हारी मुकुट में चमक रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ तुम्हारा ध्यान है, छोटे मुँह बड़ी बात, तनिक होश की दवा करो ना ।" १ इस संवाद के लेखक का स्वर भारतेन्दु-युग का प्रतिनिधि स्वर है, इस युग के लेखक इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील है कि भारत अपने प्राचीन वैभव और अपनी गरिमामयी परम्पराओं को विस्मृत न करे । एकता के अटूट सूत्र मे परस्पर बँधा मानव देश को गौरव के शिखर पर आरूढ करे और इंगलैण्ड के 'मायावी पुत्रो' से इसको मुक्ति दिलाये ।
इस अंक में किसी ग्रन्थ की न तो व्यावहारिक आलोचना मिलती है और न किसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादन ही । परन्तु, निबन्धों के चयन में सम्पादक की भावयित्री प्रतिभा का अच्छा प्रकाशन हुआ है और इन निबन्धों मे ( जिनमे कुछ अनुवाद भी सम्मिलित है ) उसके मन्तव्य में सन्देह नहीं रह जाता । 'ललित भाषा छन्दों में' किया गया 'मेघदूत' का अनुवाद और 'वाल्मीकिरामायण' का हिन्दी-रूपान्तर, दोनों इस बात की घोषणा करते है कि इस युग के लेखक, सम्पादक और कवि हिन्दी - साहित्य के विकास को अपना पुनीत लक्ष्य बना चुके हैं और वे चाहते हैं कि हिन्दी - साहित्य ही समृद्ध न हो, प्रत्युत हिन्दी की तकनीकी शब्दावली भी यथाशीघ्र संवद्धित हो जाय । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 'हिन्दी- प्रदीप' (नवम्बर, १८७७ ई०) ने 'वायु का वर्णन' और 'ऐंग्लो वरन्याकुलर' शीर्षक निबन्ध (जिसमें पश्चिमोत्तर देश की सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना की गई है) प्रकाशित किया था । ' हिन्दी - प्रदीप' के दिसम्बर, १८७७ ई० वाले अंक में प्रकाशित 'भोजनपदार्थ' और इसी अंक में प्रकाशित 'हवा का बोझ' आदि सैकड़ों निबन्ध केवल रोचकता की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नही हैं, वे तयुगीन सम्पादकीय मनोवृत्ति को भी प्रकाशित करते है और इस बात की सूचना देते हैं कि खड़ी बोली की नींव सुदृढ हो चली है और नये-नये पारिभाषिक शब्दों का आयात शुरू हो गया है । हिन्दी की आधुनिक आलोचना का विकास ऐसी ही नींव पर सम्भव था । पं० बालकृष्ण भट्ट, भारतेन्दु प्रभृति ने भावसम्प्रेषण के माध्यम को
१. हिन्दी - प्रदीप (जिल्द १, संख्या ३, सन् १८७७ ई०), पृ० २ ।