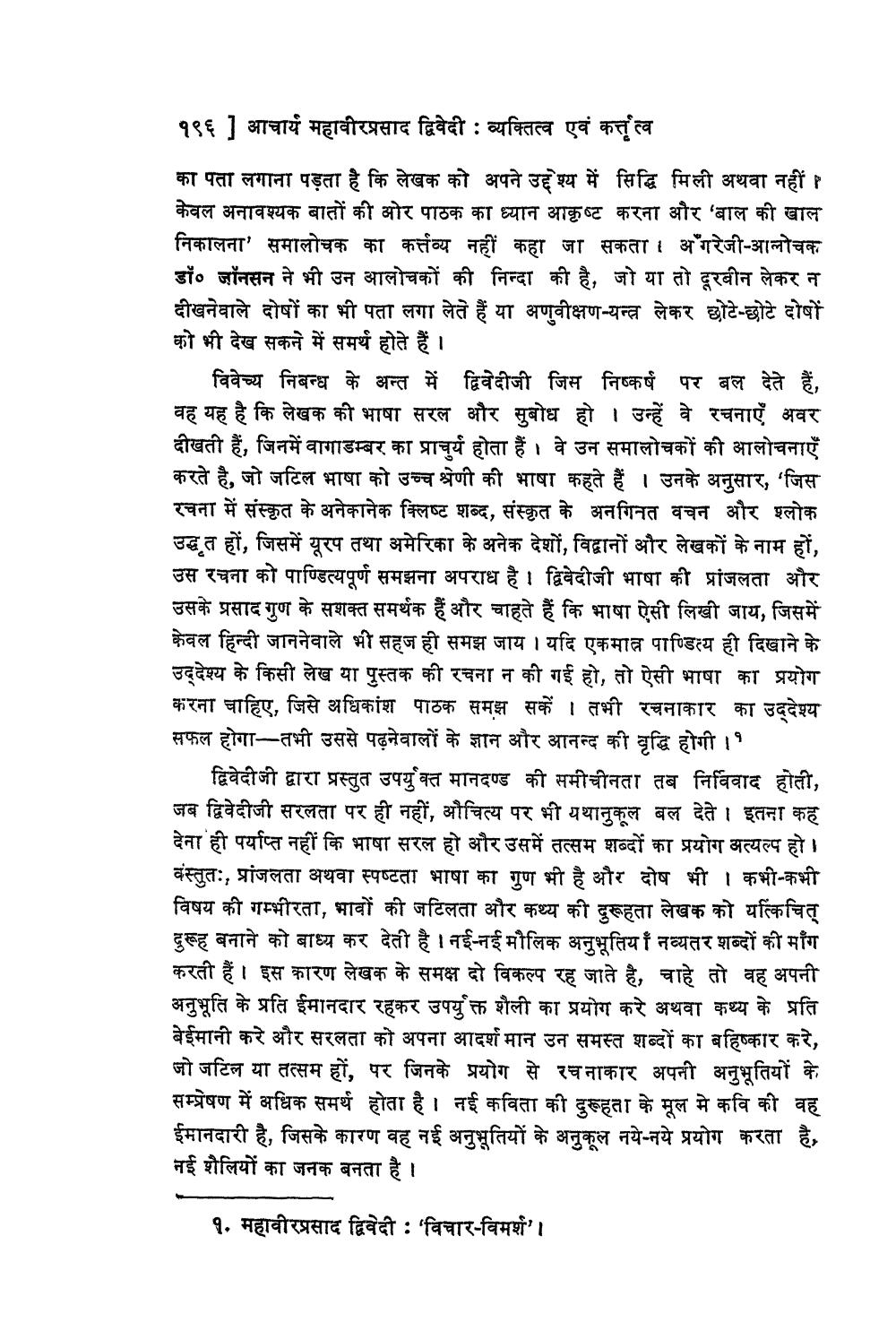________________
१९६ ] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का पता लगाना पड़ता है कि लेखक को अपने उद्देश्य में सिद्धि मिली अथवा नहीं। केवल अनावश्यक बातों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करना और 'बाल की खाल निकालना' समालोचक का कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। अंगरेजी-आलोचक डॉ० जॉनसन ने भी उन आलोचकों की निन्दा की है, जो या तो दूरबीन लेकर न दीखनेवाले दोषों का भी पता लगा लेते हैं या अणुवीक्षण-यन्त्र लेकर छोटे-छोटे दोषों को भी देख सकने में समर्थ होते हैं।
विवेच्य निबन्ध के अन्त में द्विवेदीजी जिस निष्कर्ष पर बल देते हैं, वह यह है कि लेखक की भाषा सरल और सुबोध हो । उन्हें वे रचनाएँ अवर दीखती हैं, जिनमें वागाडम्बर का प्राचुर्य होता हैं। वे उन समालोचकों की आलोचनाएँ करते है, जो जटिल भाषा को उच्च श्रेणी की भाषा कहते हैं । उनके अनुसार, 'जिस रचना में संस्कृत के अनेकानेक क्लिष्ट शब्द, संस्कृत के अनगिनत वचन और श्लोक उद्धृत हों, जिसमें यूरप तथा अमेरिका के अनेक देशों, विद्वानों और लेखकों के नाम हों, उस रचना को पाण्डित्यपूर्ण समझना अपराध है। द्विवेदीजी भाषा की प्रांजलता और उसके प्रसाद गुण के सशक्त समर्थक हैं और चाहते हैं कि भाषा ऐसी लिखी जाय, जिसमें केवल हिन्दी जाननेवाले भी सहज ही समझ जाय । यदि एकमात्र पाण्डित्य ही दिखाने के उद्देश्य के किसी लेख या पुस्तक की रचना न की गई हो, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे अधिकांश पाठक समझ सकें । तभी रचनाकार का उद्देश्य सफल होगा-तभी उससे पढ़नेवालों के ज्ञान और आनन्द की वृद्धि होगी।'
द्विवेदीजी द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त मानदण्ड की समीचीनता तब निर्विवाद होती, जब द्विवेदीजी सरलता पर ही नहीं, औचित्य पर भी यथानुकूल बल देते। इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं कि भाषा सरल हो और उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अत्यल्प हो। वस्तुतः, प्रांजलता अथवा स्पष्टता भाषा का गुण भी है और दोष भी । कभी-कभी विषय की गम्भीरता, भावों की जटिलता और कथ्य की दुरूहता लेखक को यत्किचित् दुरूह बनाने को बाध्य कर देती है। नई-नई मौलिक अनुभूतियाँ नव्यतर शब्दों की मांग करती हैं। इस कारण लेखक के समक्ष दो विकल्प रह जाते है, चाहे तो वह अपनी अनुभूति के प्रति ईमानदार रहकर उपर्युक्त शैली का प्रयोग करे अथवा कथ्य के प्रति बेईमानी करे और सरलता को अपना आदर्श मान उन समस्त शब्दों का बहिष्कार करे, जो जटिल या तत्सम हों, पर जिनके प्रयोग से रचनाकार अपनी अनुभूतियों के सम्प्रेषण में अधिक समर्थ होता है। नई कविता की दुरूहता के मूल मे कवि की वह ईमानदारी है, जिसके कारण वह नई अनुभूतियों के अनुकूल नये-नये प्रयोग करता है, नई शैलियों का जनक बनता है।
१. महावीरप्रसाद द्विवेदी : 'विचार-विमर्श'।