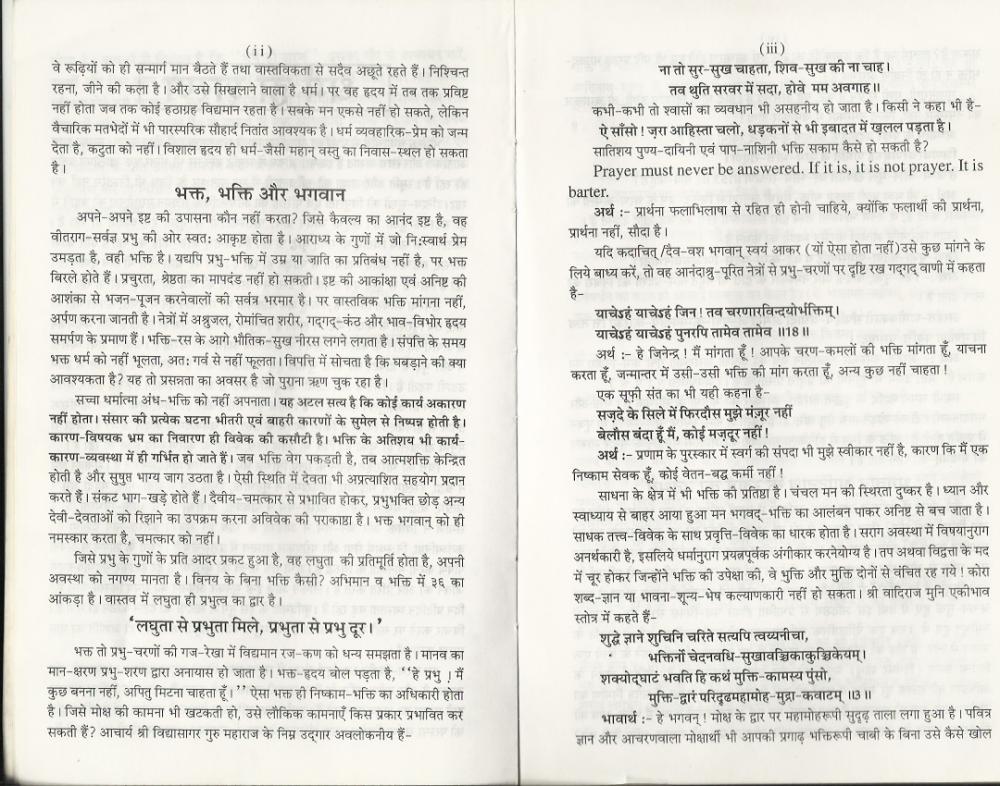________________
वे रूढ़ियों को ही सन्मार्ग मान बैठते हैं तथा वास्तविकता से सदैव अछूते रहते हैं। निश्चिन्त रहना, जीने की कला है। और उसे सिखलाने वाला है धर्म। पर वह हृदय में तब तक प्रविष्ट नहीं होता जब तक कोई हठाग्रह विद्यमान रहता है। सबके मन एकसे नहीं हो सकते, लेकिन वैचारिक मतभेदों में भी पारस्परिक सौहार्द नितांत आवश्यक है। धर्म व्यवहारिक-प्रेम को जन्म देता है, कटुता को नहीं। विशाल हदय ही धर्म-जैसी महान् वस्तु का निवास स्थल हो सकता
है।
ना तो सुर-सुख चाहता, शिव-सुख की ना चाह।
तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह॥ कभी-कभी तो श्वासों का व्यवधान भी असहनीय हो जाता है। किसी ने कहा भी हैऐसाँसो ! जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। सातिशय पुण्य-दायिनी एवं पाप-नाशिनी भक्ति सकाम कैसे हो सकती है?
Prayer must never be answered. If it is, it is not prayer. It is barter.
अर्थ :- प्रार्थना फलाभिलाषा से रहित ही होनी चाहिये, क्योंकि फलार्थी की प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, सौदा है।
यदि कदाचित् /दैव-वश भगवान् स्वयं आकर (यों ऐसा होता नहीं)उसे कुछ मांगने के लिये बाध्य करें, तो वह आनंदाश्रु-पूरित नेत्रों से प्रभु-चरणों पर दृष्टि रख गद्गद् वाणी में कहता
भक्त, भक्ति और भगवान अपने-अपने इष्ट की उपासना कौन नहीं करता? जिसे कैवल्य का आनंद इष्ट है, वह वीतराग-सर्वज्ञ प्रभु की ओर स्वत: आकृष्ट होता है। आराध्य के गुणों में जो नि:स्वार्थ प्रेम उमड़ता है, वही भक्ति है। यद्यपि प्रभु-भक्ति में उम्र या जाति का प्रतिबंध नहीं है, पर भक्त बिरले होते हैं। प्रचुरता, श्रेष्ठता का मापदंड नहीं हो सकती। इष्ट की आकांक्षा एवं अनिष्ट की आशंका से भजन-पूजन करनेवालों की सर्वत्र भरमार है। पर वास्तविक भक्ति मांगना नहीं, अर्पण करना जानती है। नेत्रों में अश्रुजल, रोमांचित शरीर, गद्गद्-कंठ और भाव-विभोर हृदय समर्पण के प्रमाण हैं। भक्ति-रस के आगे भौतिक-सुख नीरस लगने लगता है। संपत्ति के समय भक्त धर्म को नहीं भूलता, अत: गर्व से नहीं फूलता। विपत्ति में सोचता है कि घबड़ाने की क्या आवश्यकता है? यह तो प्रसन्नता का अवसर है जो पुराना ऋण चुक रहा है।।
सच्चा धर्मात्मा अंध-भक्ति को नहीं अपनाता। यह अटल सत्य है कि कोई कार्य अकारण नहीं होता। संसार की प्रत्येक घटना भीतरी एवं बाहरी कारणों के सुमेल से निष्पन्न होती है। कारण-विषयक भ्रम का निवारण ही विवेक की कसौटी है। भक्ति के अतिशय भी कार्यकारण-व्यवस्था में ही गर्भित हो जाते हैं। जब भक्ति वेग पकड़ती है, तब आत्मशक्ति केन्द्रित होती है और सुषुप्त भाग्य जाग उठता है। ऐसी स्थिति में देवता भी अप्रत्याशित सहयोग प्रदान करते हैं। संकट भाग-खड़े होते हैं। दैवीय-चमत्कार से प्रभावित होकर, प्रभुभक्ति छोड़ अन्य देवी-देवताओं को रिझाने का उपक्रम करना अविवेक की पराकाष्ठा है। भक्त भगवान् को ही नमस्कार करता है, चमत्कार को नहीं।
जिसे प्रभु के गुणों के प्रति आदर प्रकट हुआ है, वह लघुता की प्रतिमूर्ति होता है, अपनी अवस्था को नगण्य मानता है। विनय के बिना भक्ति कैसी? अभिमान व भक्ति में ३६ का आंकड़ा है। वास्तव में लघुता ही प्रभुत्व का द्वार है।
'लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुदूर।' भक्त तो प्रभु-चरणों की गज-रेखा में विद्यमान रज-कण को धन्य समझता है। मानव का मान-क्षरण प्रभु-शरण द्वारा अनायास हो जाता है। भक्त-हृदय बोल पड़ता है, "हे प्रभु । मैं कुछ बनना नहीं, अपितु मिटना चाहता हूँ।" ऐसा भक्त ही निष्काम-भक्ति का अधिकारी होता है। जिसे मोक्ष की कामना भी खटकती हो, उसे लौकिक कामनाएँ किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं? आचार्य श्री विद्यासागर गुरु महाराज के निम्न उद्गार अवलोकनीय हैं
याचेऽहं याचेऽहं जिन ! तव चरणारविन्दयोर्भक्तिम्। याचेऽहं याचेऽहं पुनरपि तामेव तामेव ॥18॥
अर्थ :- हे जिनेन्द्र ! मैं मांगता हूँ। आपके चरण-कमलों की भक्ति मांगता हूँ, याचना करता हूँ, जन्मान्तर में उसी-उसी भक्ति की मांग करता हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहता!
एक सूफी संत का भी यही कहना हैसज़दे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं बेलौस बंदा हूँ मैं, कोई मज़दूर नहीं!
अर्थ :- प्रणाम के पुरस्कार में स्वर्ग की संपदा भी मुझे स्वीकार नहीं है, कारण कि मैं एक निष्काम सेवक हूँ, कोई वेतन-बद्ध कर्मी नहीं!
साधना के क्षेत्र में भी भक्ति की प्रतिष्ठा है। चंचल मन की स्थिरता दुष्कर है। ध्यान और स्वाध्याय से बाहर आया हुआ मन भगवद्-भक्ति का आलंबन पाकर अनिष्ट से बच जाता है। साधक तत्त्व-विवेक के साथ प्रवृत्ति-विवेक का धारक होता है। सराग अवस्था में विषयानुराग अनर्थकारी है, इसलिये धर्मानुराग प्रयत्नपूर्वक अंगीकार करनेयोग्य है । तप अथवा विद्वत्ता के मद में चूर होकर जिन्होंने भक्ति की उपेक्षा की, वे भुक्ति और मुक्ति दोनों से वंचित रह गये ! कोरा शब्द-ज्ञान या भावना शून्य-भेष कल्याणकारी नहीं हो सकता। श्री वादिराज मुनि एकीभाव स्तोत्र में कहते हैंशुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा,
भक्तिों चेदनवधि-सुखावञ्चिकाकुझिकेयम्। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्ति-कामस्य पुंसी,
मुक्ति-द्वारं परिदृढमहामोह-मुद्रा-कवाटम् ।।३।। भावार्थ :- हे भगवन् ! मोक्ष के द्वार पर महामोहरूपी सुदृढ़ ताला लगा हुआ है। पवित्र ज्ञान और आचरणवाला मोक्षार्थी भी आपकी प्रगाढ़ भक्तिरूपी चाबी के बिना उसे कैसे खोल