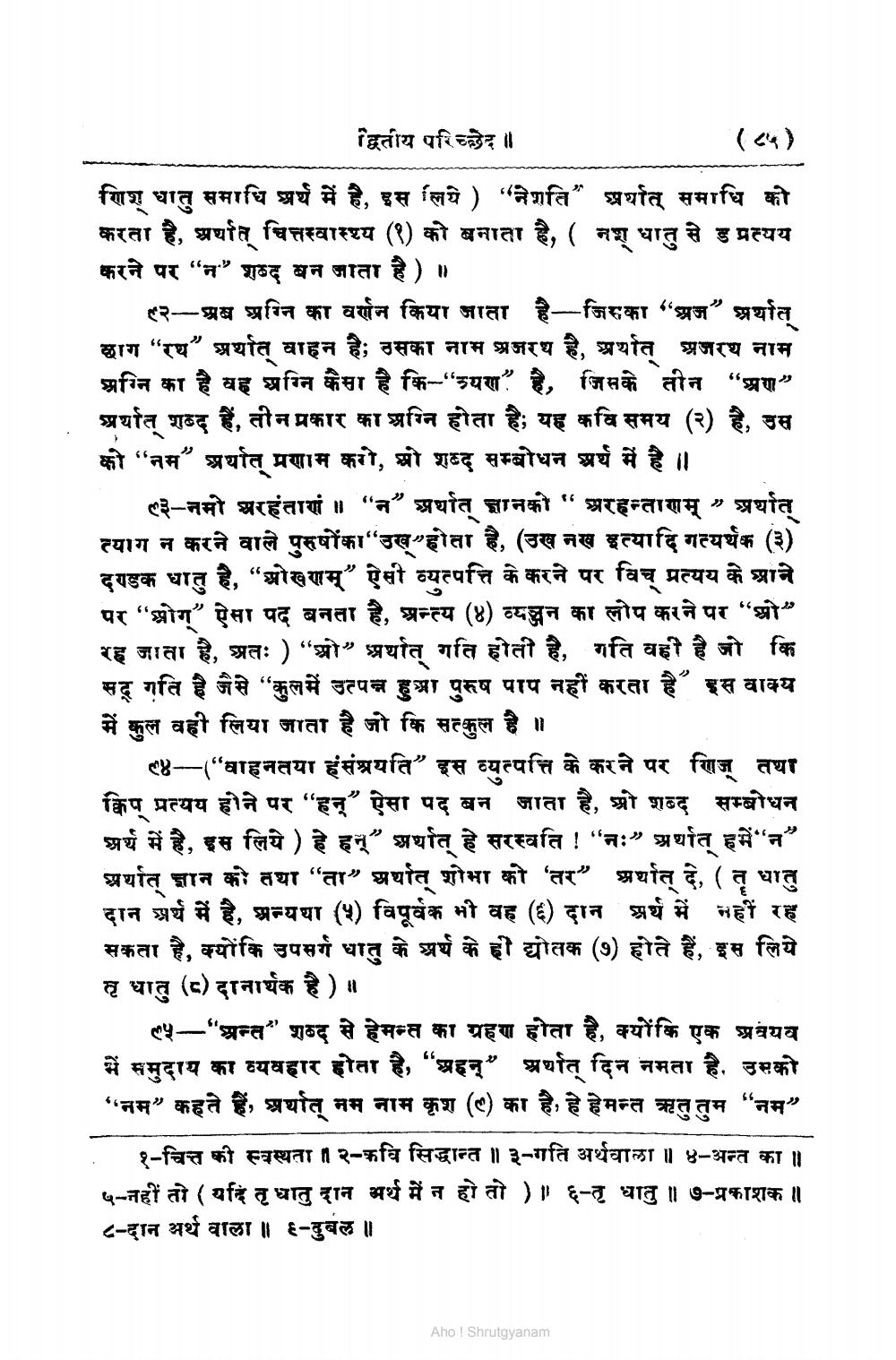________________
द्वितीय परिच्छेद ॥
णिश् धातु समाधि अर्थ में है, इस लिये ) “नेशति” अर्थात् समाधि को करता है, अर्थात् चित्तस्वास्थ्य (१) को बनाता है, ( नश् धातु से ड प्रत्यय करने पर "न" शब्द बन जाता है) ॥
१२--अब अग्नि का वर्णन किया जाता है-जिसका "अज” अर्थात छाग “रथ” अर्थात् वाहन है; उसका नाम अजरथ है, अर्थात अजरथ नाम अग्नि का है वह अग्नि कैसा है कि-"ज्यण” है, जिसके तीन "अण" अर्थात् शब्द हैं, तीन प्रकार का अग्नि होता है। यह कवि समय (२) है, उस को “नम” अर्थात् प्रणाम करो, सो शब्द सम्बोधन अर्थ में है ॥ ___९३-नमो अरहंताणं ॥ “न” अर्थात् ज्ञानको “ अरहन्ताणम् ” अर्थात् त्याग न करने वाले पुरुषोंका"उख होता है, (उख नख इत्यादि गत्यर्थक (३) दण्डक धातु है, "मोखणम्” ऐसी व्युत्पत्ति के करने पर विच् प्रत्यय के आने पर "प्रोग्” ऐसा पद बनता है, अन्त्य (४) व्यञ्जन का लोप करने पर "श्री" रह जाता है, अतः ) “ो” अर्थात् गति होती है, गति वही है जो कि सद् गति है जैसे "कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष पाप नहीं करता है इस वाक्य में कुल वही लिया जाता है जो कि सत्कुल है ॥ ___४-(“वाहनतया हंसंश्रयति” इस व्युत्पत्ति के करने पर णिज् तथा विप प्रत्यय होने पर "हन्” ऐसा पद बन जाता है, प्रो शब्द सम्बोधन अर्थ में है, इस लिये ) हे हन्" अर्थात् हे सरस्वति ! "नः" अर्थात हमें"न" अर्थात ज्ञान को तथा "ता" अर्थात शोभा को 'तर" अर्थात दे, ( त धातु दान अर्थ में है, अन्यथा (५) विपूर्वक भी वह (६) दान अर्थ में नहीं रह सकता है, क्योंकि उपसर्ग धातु के अर्थ के ही द्योतक (७) होते हैं, इस लिये तृ धातु (८) दानार्थक है)। ___९५-"अन्त" शब्द से हेमन्त का ग्रहण होता है, क्योंकि एक अवयव में समुदाय का व्यवहार होता है, "अहन्" अर्थात् दिन नमता है. उसको "नम” कहते हैं, अर्थात् नम नाम कृश (क) का है। हे हेमन्त ऋतु तुम "नम"
१-चित्त की स्वस्थता ॥ २-कवि सिद्धान्त ॥ ३-गति अर्थवाला ॥ ४-अन्त का ॥ ५-नहीं तो ( यदि तृ धातु दान अर्थ में न हो तो )॥ ६-तृ धातु ॥ ७-प्रकाशक ॥ ८-दान अर्थ वाला ॥ -दुबल ॥
Aho! Shrutgyanam