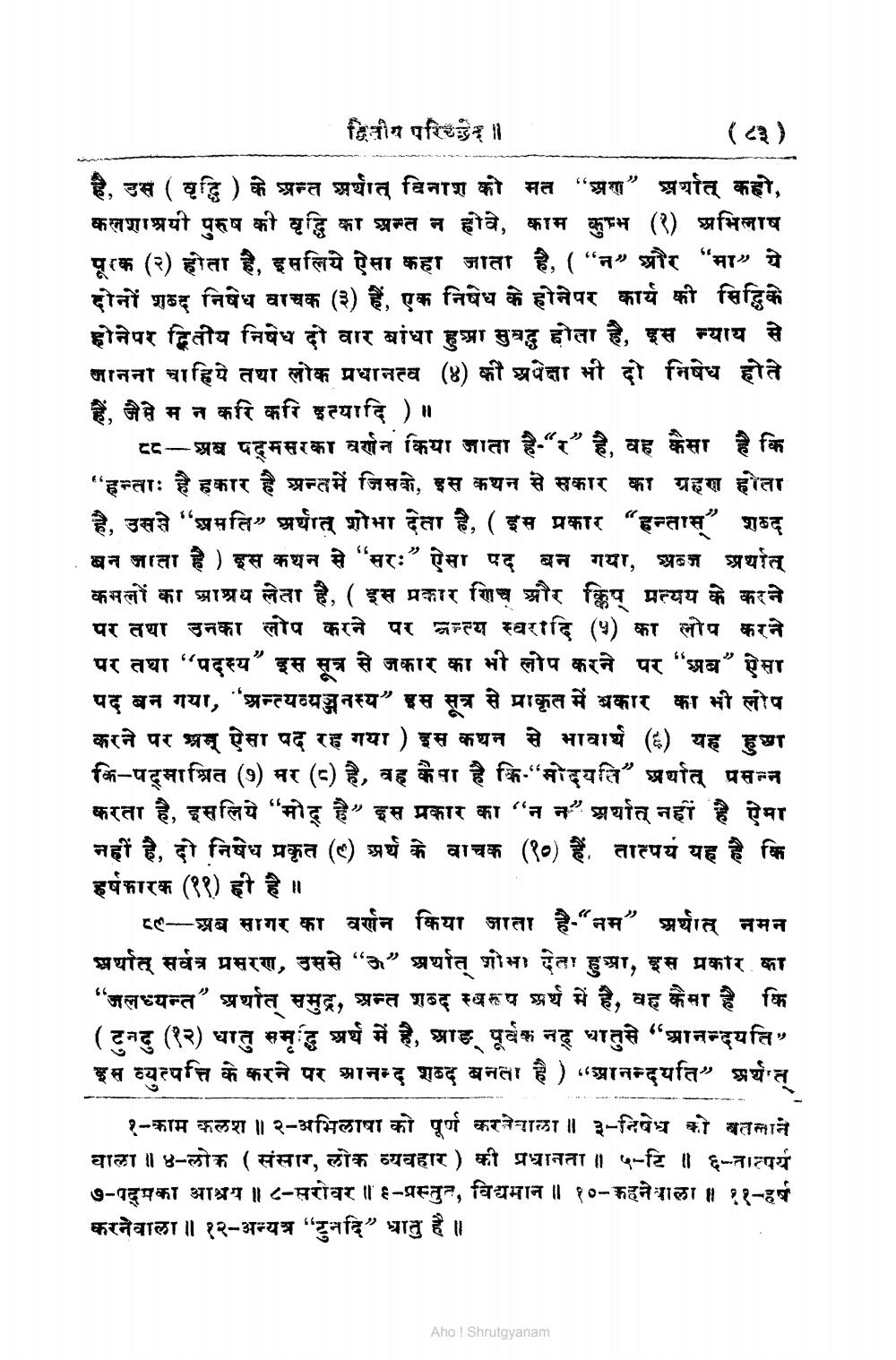________________
द्वितीय परिच्छेद ॥
(८३) है, उस ( वृद्धि ) के अन्त अर्थात् विनाश को मत “ण” अर्थात् कहो, कलशाश्रयी पुरुष की वृद्धि का अन्त न होवे, काम कुम्भ (१) अभिलाष पूरक (२) होता है, इसलिये ऐसा कहा जाता है, ( "न" और "मा” ये दोनों शब्द निषेध वाचक (३) हैं, एक निषेध के होने पर कार्य की सिद्धिके होनेपर द्वितीय निषेध दो वार बांधा हुआ सुबद्ध होता है, इस न्याय से जानना चाहिये तथा लोक प्रधानत्व (४) की अपेक्षा भी दो निषेध होते हैं, जैसे म न करि करि इत्यादि )॥ ____८८-अब पद्मसर का वर्णन किया जाता है-“र” है, वह कैसा है कि "हन्ताः है हकार है अन्त में जिसके, इस कथन से सकार का ग्रहण होता है, उससे "अमति” अर्थात् शोभा देता है, ( इस प्रकार “हन्तास्” शब्द बन जाता है ) इस कथन से “सरः” ऐसा पद बन गया, अब्ज अर्थात् कमलों का आश्रय लेता है, ( इस प्रकार णिच और क्किय् प्रत्यय के करने पर तथा उनका लोप करने पर अन्त्य स्वरादि (५) का लोप करने पर तथा “पदस्य” इस सूत्र से जकार का भी लोप करने पर "अब” ऐसा पद बन गया, “अन्त्यव्यञ्जनस्य” इस सूत्र से प्राकृत में अकार का भी लोप करने पर श्रम ऐसा पद रह गया ) इस कथन से भावार्थ (६) यह हुधा कि-पद्नाश्रित (७) मर (८) है, वह कैसा है कि "मोदयति” अर्थात् प्रसन्न करता है, इसलिये "मोद् है" इस प्रकार का "न न" अर्थात् नहीं है ऐमा नहीं है, दो निषेध प्रकृत (e) अर्थ के वाचक (१०) हैं, तात्पर्य यह है कि हर्षकारक (११) ही है ॥ ___-अब सागर का वर्णन किया जाता है."नम” अर्थात् नमन अर्थात् सर्वत्र प्रसरण, उससे "3" अर्थात् शोभा देता हुआ, इस प्रकार का "जलध्यन्त” अर्थात समुद्र, अन्त शब्द स्वरूप अर्थ में है, वह कैसा है कि (टुनदु (१२) धातु समृद्धि अर्थ में है, प्राङ पूर्वक नद् धातुसे “प्रानन्दयति" इस व्युत्पत्ति के करने पर प्रानन्द शब्द बनता है ) 'आनन्दयति” अर्थात
१-काम कलश ॥२-अभिलाषा को पूर्ण करनेवाला ॥ ३-निषेध को बतलाने वाला ॥४-लोक ( संसार, लोक व्यवहार ) की प्रधानता ॥ ५-टि ॥ ६-तात्पर्य ७-पद्मका आश्रय ॥ ८-सरोवर ॥-प्रस्तुत, विद्यमान ॥ १०-कहने वाला ॥ ११-हर्ष करनेवाला ॥ १२-अन्यत्र "टुनदि” धातु है ।
Aho! Shrutgyanam