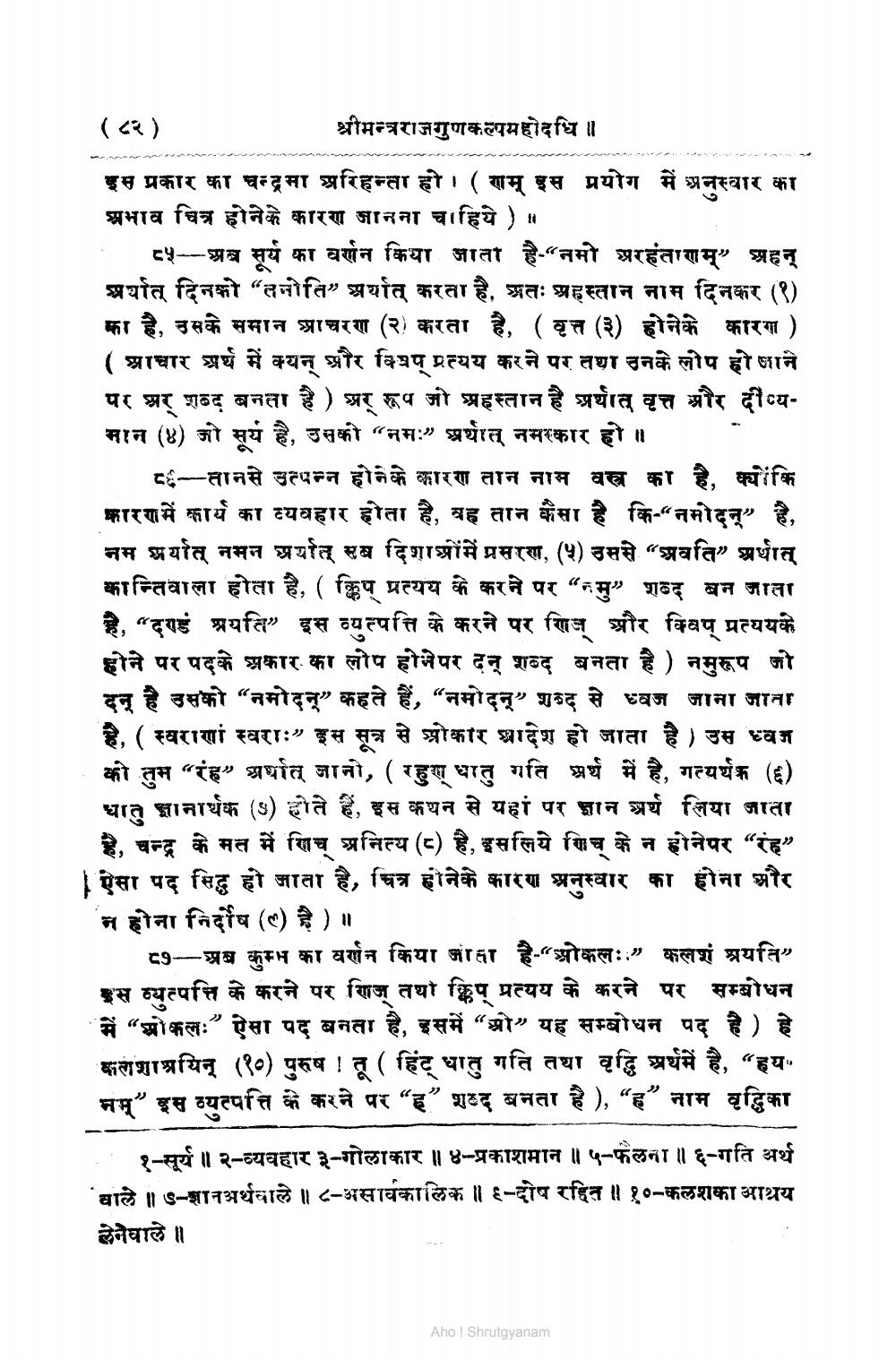________________
(८२)
श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहोदधि ॥ इस प्रकार का चन्द्रमा अरिहन्ता हो। ( गम् इस प्रयोग में अनुस्वार का प्रभाव चित्र होने के कारण जानना चाहिये) ॥
८५--अब सूर्य का वर्णन किया जाता है-"नमो अरहंताणम्” अहन् अर्थात् दिनको “तनोति” अर्थात् करता है, अतः अहस्तान नाम दिनकर (१) का है, उसके समान पाचरण (२) करता है, ( वृत्त (३) होनेके कारण ) (प्राचार अर्थ में क्यन् और विषप् प्रत्यय करने पर तथा उनके लोप हो जाने पर भर् शब्द बनता है ) अर् रूप जो अहस्तान है अर्थात वृत्त और दीव्यमान (४) जो सूर्य है, उसको “नमः” अर्थात् नमस्कार हो । _____८६-तानसे उत्पन्न होने के कारण तान नाम वस्त्र का है, क्योंकि कारण में कार्य का व्यवहार होता है, वह तान कैसा है कि-"नमोदन्” है, नम अर्यात् नमन अर्यात् सब दिशाओं में प्रसरण, (५) उससे “प्रवति" अर्थात् कान्तिवाला होता है, (क्किप प्रत्यय के करने पर “कमु” शब्द बन जाता है, "दगडं अयति" इस व्युत्पत्ति के करने पर णिज और क्विप् प्रत्ययके होने पर पदके प्रकार का लोप होने पर दन् शब्द बनता है ) नमुरूप जो दन है उसको “नमोदन” कहते हैं, “नमोदन” शब्द से ध्वज जाना जाता है, ( स्वराणां स्वराः” इस सत्र से प्रोकार प्रादेश हो जाता है। उस ध्वज को तुम “रंह" अर्थात् जानो, ( रहुण धातु गति अर्थ में है, गत्यर्थक (६) धात ज्ञानार्थक (७) होते हैं, इस कथन से यहां पर ज्ञान अर्थ लिया जाता
है, चन्द्र के मत में णिच् अनित्य (८) है, इसलिये गिाच् के न होनेपर "रंह" | ऐसा पद सिद्ध हो जाता है, चित्र होने के कारणा अनुस्वार का होना और न होना निर्दोष (९) है ) ॥
८-अब कुम्भ का वर्णन किया जाता है-“ओकलः” कलशं श्रयति” इस व्यत्पत्ति के करने पर णिज तथो क्लिप् प्रत्यय के करने पर सम्बोधन में “मोकलः” ऐसा पद बनता है, इसमें “मो” यह सम्बोधन पद है) हे कलाशायिन् (१०) पुरुष ! तू ( हिंट् धातु गति तथा वृद्धि अर्थमें है, "हय. मम्" इस व्युत्पत्ति के करने पर “ह” शब्द बनता है ), "ह" नाम वृद्धिका - १-सूर्य ॥ २-व्यवहार ३-गोलाकार ॥ ४-प्रकाशमान ॥ ५-फैलना ॥६-गति अर्थ वाले ॥ ७-शानअर्थवाले ॥ ८-असार्वकालिक ॥ १-दोष रहित ॥१०-कलशका आश्रय लेनेवाले॥
Aho! Shrutgyanam