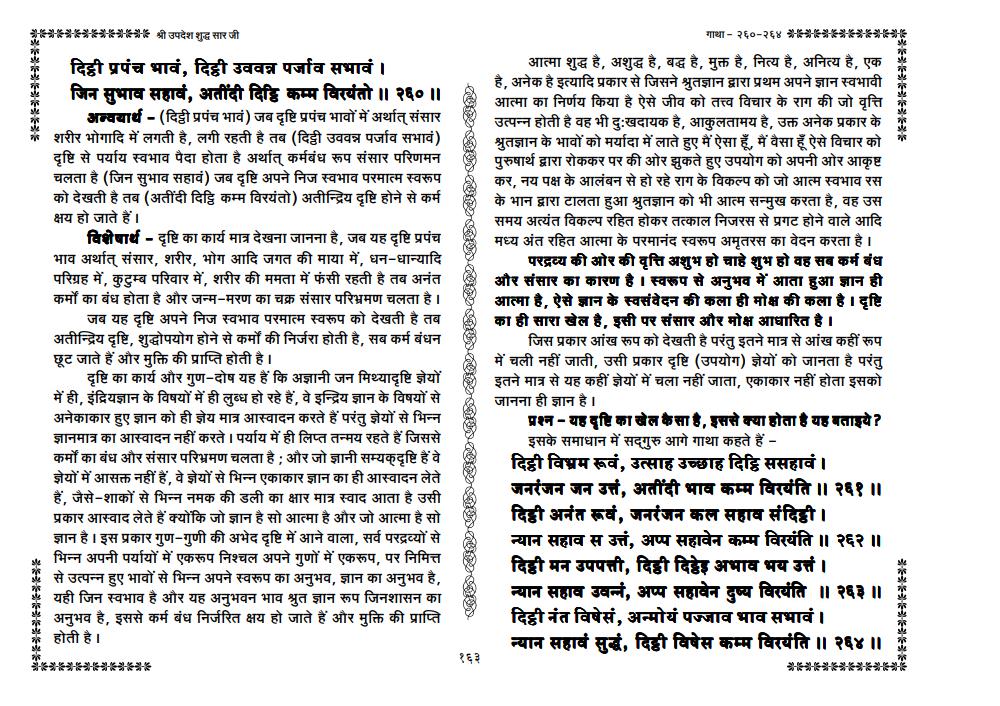________________
9-5-19-5
*****-*-* श्री उपदेश शुद्ध सार जी
गाथा-२६०-२६४---
-
-
दिट्ठी प्रपंच भावं, दिट्ठी उववन्न पर्जाव सभावं । जिन सुभाव सहावं, अतींदी दिडि कम्म विरयंतो ॥ २६०॥
अन्वयार्थ-(दिट्ठी प्रपंच भावं) जब दृष्टि प्रपंच भावों में अर्थात् संसार * शरीर भोगादि में लगती है, लगी रहती है तब (दिट्ठी उववन्न पर्जाव सभावं)
दृष्टि से पर्याय स्वभाव पैदा होता है अर्थात् कर्मबंध रूप संसार परिणमन चलता है (जिन सुभाव सहावं) जब दृष्टि अपने निज स्वभाव परमात्म स्वरूप को देखती है तब (अतींदी दिट्टि कम्म विरयंतो) अतीन्द्रिय दृष्टि होने से कर्म क्षय हो जाते हैं।
विशेषार्थ- दृष्टि का कार्य मात्र देखना जानना है, जब यह दृष्टि प्रपंच भाव अर्थात् संसार, शरीर, भोग आदि जगत की माया में, धन-धान्यादि परिग्रह में, कुटुम्ब परिवार में, शरीर की ममता में फंसी रहती है तब अनंत कर्मों का बंध होता है और जन्म-मरण का चक्र संसार परिभ्रमण चलता है।
ह दृष्टि अपने निज स्वभाव परमात्म स्वरूप को देखती है तब अतीन्द्रिय दृष्टि, शुद्धोपयोग होने से कर्मों की निर्जरा होती है, सब कर्म बंधन छूट जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है।
दृष्टि का कार्य और गुण-दोष यह हैं कि अज्ञानी जन मिथ्यादृष्टि ज्ञेयों में ही, इंद्रियज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं. वे इन्द्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञानमात्र का आस्वादन नहीं करते। पर्याय में ही लिप्त तन्मय रहते हैं जिससे कर्मों का बंध और संसार परिभ्रमण चलता है और जो ज्ञानी सम्यक्दृष्टि हैं वे ज्ञेयों में आसक्त नहीं हैं, वे ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वादन लेते हैं, जैसे-शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इस प्रकार गुण-गुणी की अभेद दृष्टि में आने वाला, सर्व परद्रव्यों से भिन्न अपनी पर्यायों में एकरूप निश्चल अपने गुणों में एकरूप, पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव, ज्ञान का अनुभव है, यही जिन स्वभाव है और यह अनुभवन भाव श्रुत ज्ञान रूप जिनशासन का अनुभव है, इससे कर्म बंध निर्जरित क्षय हो जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है।
आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध है, बद्ध है, मुक्त है, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है इत्यादि प्रकार से जिसने श्रुतज्ञान द्वारा प्रथम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया है ऐसे जीव को तत्त्व विचार के राग की जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह भी दु:खदायक है, आकुलतामय है, उक्त अनेक प्रकार के
श्रुतज्ञान के भावों को मर्यादा में लाते हुए मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ऐसे विचार को 6 पुरुषार्थ द्वारा रोककर पर की ओर झुकते हुए उपयोग को अपनी ओर आकृष्ट
कर, नय पक्ष के आलंबन से हो रहे राग के विकल्प को जो आत्म स्वभाव रस के भान द्वारा टालता हुआ श्रुतज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता है, वह उस समय अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निजरस से प्रगट होने वाले आदि मध्य अंत रहित आत्मा के परमानंद स्वरूप अमृतरस का वेदन करता है।
परद्रव्य की ओर की वृत्ति अशुभ हो चाहे शुभ हो वह सब कर्म बंध और संसार का कारण है । स्वरूप से अनुभव में आता हुआ ज्ञान ही आत्मा है, ऐसे ज्ञान के स्वसंवेदन की कला ही मोक्ष की कला है। दृष्टि का ही सारा खेल है. इसी पर संसार और मोक्ष आधारित है।
जिस प्रकार आंख रूप को देखती है परंतु इतने मात्र से आंख कहीं रूप 8 में चली नहीं जाती, उसी प्रकार दृष्टि (उपयोग) ज्ञेयों को जानता है परंतु
इतने मात्र से यह कहीं ज्ञेयों में चला नहीं जाता, एकाकार नहीं होता इसको जानना ही ज्ञान है।
प्रश्न- यह दृष्टि का खेल कैसा है, इससे क्या होता है यह बताइये?
इसके समाधान में सद्गुरु आगे गाथा कहते हैंदिट्ठी विभ्रम रूवं, उत्साह उच्छाह दिट्टि ससहावं । जनरंजन जन उत्तं, अतींदी भाव कम्म विरयंति ॥ २६१॥ दिड्डी अनंत रूर्व, जनरंजन कल सहाव संदिट्ठी। न्यान सहाव स उत्तं, अप्प सहावेन कम्म विरयंति ॥ २६२ ॥ दिड्डी मन उपपत्ती, दिड्डी दिड्डेइ अभाव भय उत्तं । न्यान सहाव उवन्नं, अप्प सहावेन दुष्य विरयंति ॥ २६३ ॥ दिट्ठीनंत विषेसं, अन्मोयं पज्जाव भाव सभावं। न्यान सहावं सुद्ध, दिडी विषेस कम्म विरयंति ॥ २६४ ॥
EE-E
E-
--HE-