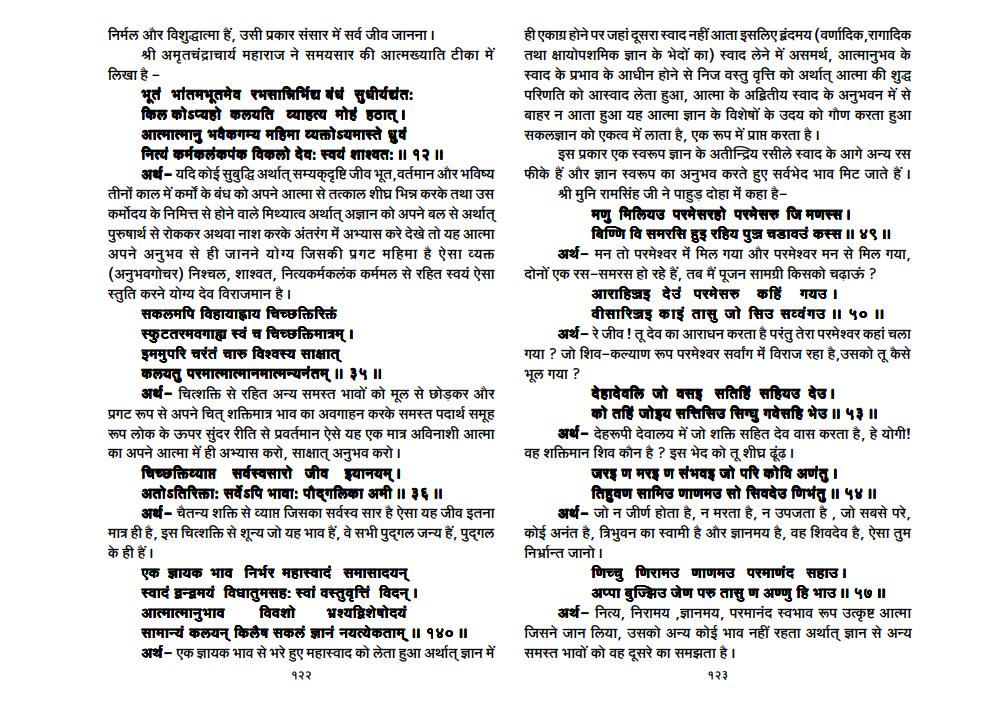________________
निर्मल और विशुद्धात्मा हैं, उसी प्रकार संसार में सर्व जीव जानना।
श्री अमृतचंद्राचार्य महाराज ने समयसार की आत्मख्याति टीका में लिखा है -
भूतं भातमभूतमेव रभसानिर्भिधबंध सुधीर्यचंत: किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठात् ।
आत्मात्मानु भवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते पूर्व नित्यं कर्मकलंकपंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२॥
अर्थ- यदि कोई सुबुद्धि अर्थात् सम्यक्दृष्टि जीव भूत,वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अर्थात् अज्ञान को अपने बल से अर्थात् पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा व्यक्त (अनुभवगोचर) निश्चल, शाश्वत, नित्यकर्मकलंक कर्ममल से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है।
सकलमपि विहायालाय चिच्छक्तिरिक्त स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् । इममुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम् ॥ ३५॥
अर्थ- चित्शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर और प्रगट रूप से अपने चित् शक्तिमात्र भाव का अवगाहन करके समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान ऐसे यह एक मात्र अविनाशी आत्मा का अपने आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात् अनुभव करो।
चिच्छक्तिच्याप्त सर्वस्वसारो जीव झ्यानयम्। अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावा: पौद्गलिका अमी॥३६॥
अर्थ-चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है ऐसा यह जीव इतना मात्र ही है, इस चित्शक्ति से शून्य जो यह भाव हैं, वे सभी पुद्गल जन्य हैं, पुद्गल के ही हैं।
एक ज्ञायक भाव निर्भर महास्वाद समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसह: स्वां वस्तुवृत्ति विदन्। आत्मात्मानुभाव विवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥ १४०॥ अर्थ- एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ अर्थात् ज्ञान में
१२२
ही एकाग्र होने पर जहां दूसरा स्वाद नहीं आता इसलिए द्वंदमय (वर्णादिक,रागादिक तथा क्षायोपशमिक ज्ञान के भेदों का) स्वाद लेने में असमर्थ, आत्मानुभव के स्वाद के प्रभाव के आधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को अर्थात् आत्मा की शुद्ध परिणति को आस्वाद लेता हुआ, आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभवन में से बाहर न आता हुआ यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सकलज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है।
इस प्रकार एक स्वरूप ज्ञान के अतीन्द्रिय रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं और ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हुए सर्वभेद भाव मिट जाते हैं। श्री मुनि रामसिंह जी ने पाहुड दोहा में कहा है
मण मिलियउ परमेसरहो परमेसरु जिमणस्स।
बिण्णि वि समरसि हुइ रहिय पुज चडावउं कस्स ॥४९॥ अर्थ- मन तो परमेश्वर में मिल गया और परमेश्वर मन से मिल गया, दोनों एक रस-समरस हो रहे हैं, तब मैं पूजन सामग्री किसको चढ़ाऊं?
आराहिजइ देउं परमेसरु कहिं गयउ।
वीसारिजइ काई तासु जो सिउ सव्वंगउ ॥ ५०॥ अर्थ-रे जीव! तू देव का आराधन करता है परंतु तेरा परमेश्वर कहां चला गया? जो शिव-कल्याण रूप परमेश्वर सर्वांग में विराज रहा है,उसको तू कैसे भूल गया ?
देहादेवलि जो वसइ सतिहिं सहियउ देउ।
को तहिं जोइय सत्तिसिउ सिन्धु गवेसहि भेउ ॥ ५३॥ अर्थ- देहरूपी देवालय में जो शक्ति सहित देव वास करता है, हे योगी! वह शक्तिमान शिव कौन है ? इस भेद को तू शीघ्र ढूंढ़।
जरहण मरहण संभवइ जो परिकोवि अणंतु।
तिरवण सामिउ णाणमउ सो सिवदेउ णिभंतु ॥ ५४॥ अर्थ-जो न जीर्ण होता है, न मरता है, न उपजता है , जो सबसे परे, कोई अनंत है, त्रिभुवन का स्वामी है और ज्ञानमय है, वह शिवदेव है, ऐसा तुम निर्धान्त जानो।
णिच्चु णिरामउ णाणमउ परमाणंद सहाउ।
अप्पा बुज्झिउ जेण परु तासुण अण्णु हि भाउ॥ ५७॥ अर्थ- नित्य, निरामय ,ज्ञानमय, परमानंद स्वभाव रूप उत्कृष्ट आत्मा जिसने जान लिया, उसको अन्य कोई भाव नहीं रहता अर्थात् ज्ञान से अन्य समस्त भावों को वह दूसरे का समझता है।
१२३