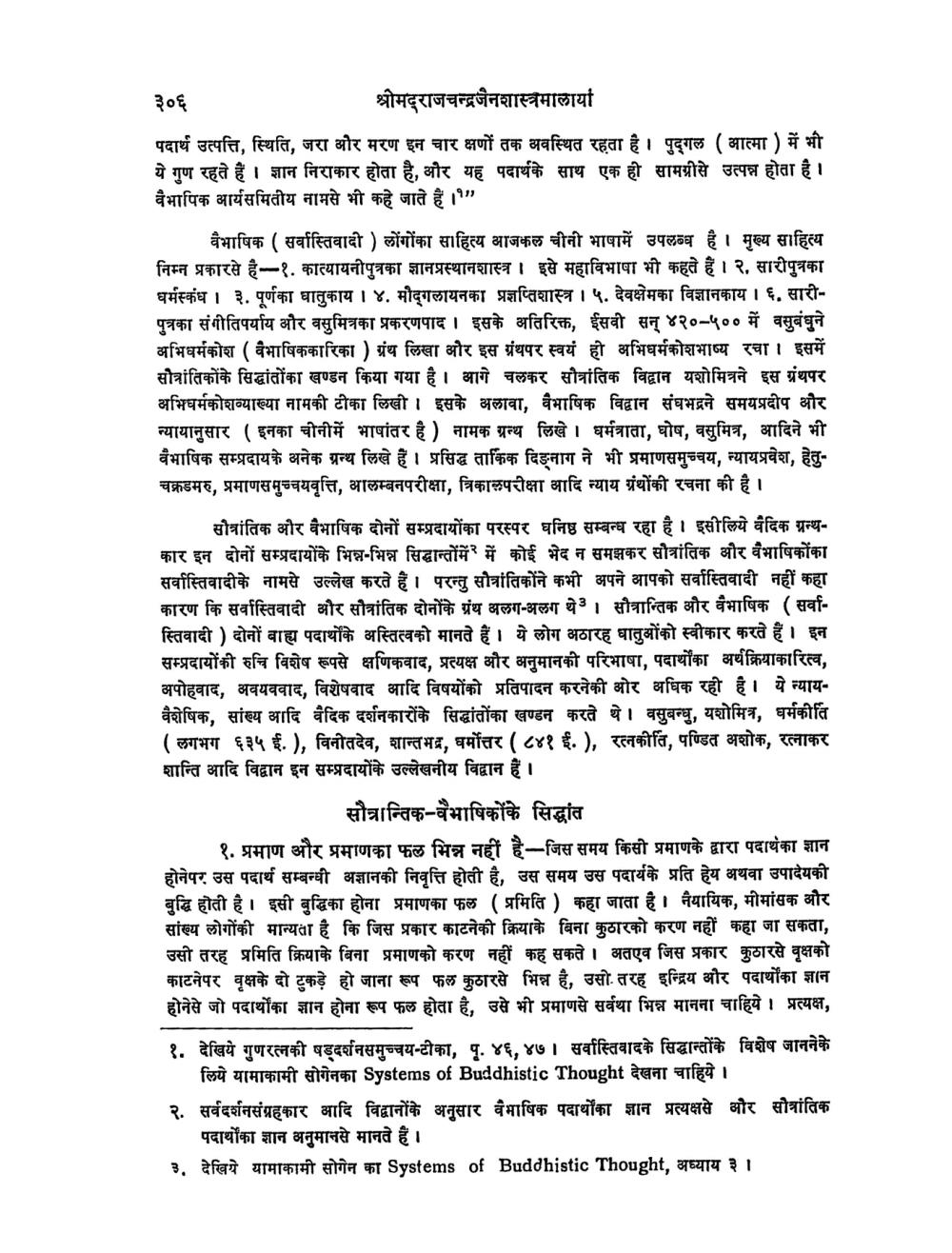________________
३०६
श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायां पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति, जरा और मरण इन चार क्षणों तक अवस्थित रहता है। पुद्गल (आत्मा) में भी ये गुण रहते हैं । ज्ञान निराकार होता है, और यह पदार्थके साथ एक ही सामग्रीसे उत्पन्न होता है। वैभापिक आर्यसमितीय नामसे भी कहे जाते हैं।"
वैभाषिक ( सर्वास्तिवादी ) लोंगोंका साहित्य आजकल चीनी भाषामें उपलब्ध है। मुख्य साहित्य निम्न प्रकारसे है-१. कात्यायनीपुत्रका ज्ञानप्रस्थानशास्त्र । इसे महाविभाषा भी कहते हैं । २. सारीपुत्रका धर्मस्कंध । ३. पूर्णका धातुकाय । ४. मौद्गलायनका प्रज्ञप्तिशास्त्र । ५. देवक्षेमका विज्ञानकाय । ६. सारीपुत्रका संगीतिपर्याय और वसुमित्रका प्रकरणपाद । इसके अतिरिक्त, ईसवी सन् ४२०-५०० में वसुबंधुने अभिधर्मकोश (वैभाषिककारिका ) ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथपर स्वयं ही अभिधर्मकोशभाष्य रचा। इसमें सौत्रांतिकोंके सिद्धांतोंका खण्डन किया गया है। आगे चलकर सौत्रांतिक विद्वान यशोमित्रने इस ग्रंथपर अभिधर्मकोशव्याख्या नामकी टीका लिखी। इसके अलावा, वैभाषिक विद्वान संघभद्रने समयप्रदीप और न्यायानुसार ( इनका चीनीमें भाषांतर है ) नामक ग्रन्थ लिखे। धर्मत्राता, घोष, वसुमित्र, आदिने भी वैभाषिक सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। प्रसिद्ध तार्किक दिङ्नाग ने भी प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश, हेतुचक्रडमरु, प्रमाणसमुच्चयवृत्ति, आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा आदि न्याय ग्रंथोंकी रचना की है।
सौत्रांतिक और वैभाषिक दोनों सम्प्रदायोंका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इसीलिये वैदिक ग्रन्थकार इन दोनों सम्प्रदायोंके भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंमें में कोई भेद न समझकर सौत्रांतिक और वैभाषिकोंका सर्वास्तिवादीके नामसे उल्लेख करते हैं। परन्तु सौत्रांतिकोंने कभी अपने आपको सर्वास्तिवादी नहीं कहा कारण कि सर्वास्तिवादी और सौत्रांतिक दोनोंके ग्रंथ अलग-अलग थे। सौत्रान्तिक और वैभाषिक (सर्वास्तिवादी ) दोनों बाह्य पदार्थों के अस्तित्वको मानते हैं। ये लोग अठारह धातुओंको स्वीकार करते हैं। इन सम्प्रदायोंकी रुचि विशेष रूपसे क्षणिकवाद, प्रत्यक्ष और अनुमानकी परिभाषा, पदार्थोंका अर्थक्रियाकारित्व, अपोहवाद, अवयववाद, विशेषवाद आदि विषयोंको प्रतिपादन करनेकी ओर अधिक रही है। ये न्यायवैशेषिक, सांख्य आदि वैदिक दर्शनकारोंके सिद्धांतोंका खण्डन करते थे। वसुबन्धु, यशोमित्र, धर्मकीर्ति ( लगभग ६३५ ई.), विनीतदेव, शान्तभद्र, धर्मोत्तर (८४१ ई.), रत्नकीति, पण्डित अशोक, रत्नाकर शान्ति आदि विद्वान इन सम्प्रदायोंके उल्लेखनीय विद्वान हैं।
सौत्रान्तिक-वैभाषिकोंके सिद्धांत १. प्रमाण और प्रमाणका फल भिन्न नहीं है-जिस समय किसी प्रमाणके द्वारा पदार्थका ज्ञान होनेपर उस पदार्थ सम्बन्धी अज्ञानको निवृत्ति होती है, उस समय उस पदार्यके प्रति हेय अथवा उपादेयकी बुद्धि होती है। इसी बुद्धिका होना प्रमाणका फल (प्रमिति ) कहा जाता है। नैयायिक, मीमांसक और सांख्य लोगोंकी मान्यता है कि जिस प्रकार काटनेकी क्रियाके बिना कुठारको करण नहीं कहा जा सकता, उसी तरह प्रमिति क्रियाके बिना प्रमाणको करण नहीं कह सकते। अतएव जिस प्रकार कुठारसे वृक्षको काटनेपर वृक्षके दो टुकड़े हो जाना रूप फल कुठारसे भिन्न है, उसी तरह इन्द्रिय और पदार्थोंका ज्ञान होनेसे जो पदार्थोंका ज्ञान होना रूप फल होता है, उसे भी प्रमाणसे सर्वथा भिन्न मानना चाहिये । प्रत्यक्ष,
१. देखिये गुणरत्नकी षड्दर्शनसमुच्चय-टीका, पृ. ४६, ४७ । सर्वास्तिवादके सिद्धान्तोंके विशेष जाननेके
लिये यामाकामी सोगेनका Systems of Buddhistic Thought देखना चाहिये । २. सर्वदर्शनसंग्रहकार आदि विद्वानोंके अनुसार वैभाषिक पदार्थोंका ज्ञान प्रत्यक्षसे और सौत्रांतिक
पदार्थोंका ज्ञान अनुमानसे मानते हैं। ३. देखिये यामाकामी सोगेन का Systems of Buddhistic Thought, अध्याय ३ ।