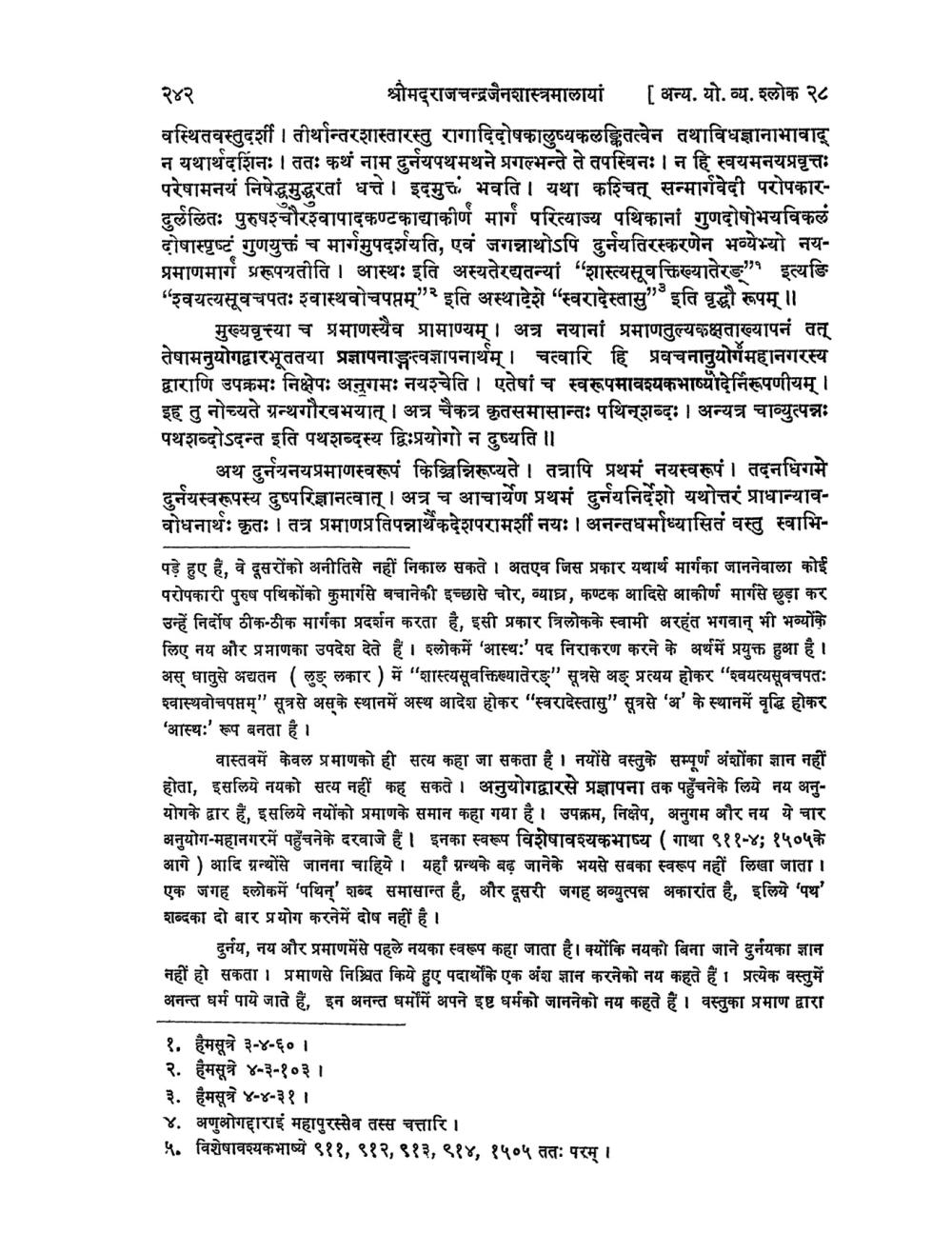________________
२४२
श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायां [अन्य. यो. व्य. श्लोक २८ वस्थितवस्तुदर्शी । तीर्थान्तरशास्तारस्तु रागादिदोषकालुष्यकलङ्कितत्वेन तथाविधज्ञानाभावाद् न यथार्थदर्शिनः । ततः कथं नाम दुर्नयपथमथने प्रगल्भन्ते ते तपस्विनः । न हि स्वयमनयप्रवृत्तः परेषामनयं निषेद्धमुद्धरतां धत्ते । इदमुक्तं भवति । यथा कश्चित् सन्मार्गवेदी परोपकारदुर्ललितः पुरुषश्चौरश्वापादकण्टकाद्याकीर्णं मार्ग परित्याज्य पथिकानां गुणदोषोभयविकलं दोषास्पृष्टं गुणयुक्तं च मार्गमुपदर्शयति, एवं जगन्नाथोऽपि दुर्नयतिरस्करणेन भव्येभ्यो नयप्रमाणमार्ग प्ररूपयतीति । आस्थः इति अस्यतेरद्यतन्यां "शास्त्यसूवक्तिख्यातेरङ१ इत्यङि "श्वयत्यसूवचपतः श्वास्थवोचपप्तम्" इति अस्थादेशे "स्वरादेस्तासु" इति वृद्धौ रूपम् ॥
मुख्यवृत्त्या च प्रमाणस्यैव प्रामाण्यम् । अत्र नयानां प्रमाणतुल्यकक्षताख्यापनं तत् तेषामनयोगद्वारभूततया प्रज्ञापनाङ्गत्वज्ञापनार्थम् । चत्वारि हि प्रवचनानुयोर्गमहानगरस्य द्वाराणि उपक्रमः निक्षेपः अनुगमः नयश्चेति । एतेषां च स्वरूपमावश्यकभाष्योदेनिरूपणीयम् । इह तु नोच्यते ग्रन्थगौरवभयात् । अत्र चैकत्र कृतसमासान्तः पथिन्शब्दः । अन्यत्र चाव्युत्पन्नः पथशब्दोऽदन्त इति पथशब्दस्य द्विःप्रयोगो न दुष्यति ॥
अथ दुर्नयनयप्रमाणस्वरूपं किञ्चिन्निरूप्यते । तत्रापि प्रथमं नयस्वरूपं । तदनधिगमे दुर्नयस्वरूपस्य दुष्परिज्ञानत्वात् । अत्र च आचार्येण प्रथमं दुर्नयनिर्देशो यथोत्तरं प्राधान्याववोधनार्थः कृतः । तत्र प्रमाणप्रतिपन्नार्थंकदेशपरामर्शी नयः । अनन्तधर्माध्यासितं वस्तु स्वाभिपड़े हुए हैं, वे दूसरोंको अनीतिसे नहीं निकाल सकते । अतएव जिस प्रकार यथार्थ मार्गका जाननेवाला कोई परोपकारी पुरुष पथिकोंको कुमार्गसे बचानेकी इच्छासे चोर, व्याघ्र , कण्टक आदिसे आकीर्ण मार्गसे छुड़ा कर उन्हें निर्दोष ठीक-ठीक मार्गका प्रदर्शन करता है, इसी प्रकार त्रिलोकके स्वामी अरहंत भगवान् भी भव्योंके लिए नय और प्रमाणका उपदेश देते हैं। श्लोकमें 'आस्थः' पद निराकरण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अस् धातुसे अद्यतन ( लुङ् लकार ) में "शास्त्यसूवक्तिख्यातेरङ्" सूत्रसे अङ् प्रत्यय होकर “श्वयत्यसूवचपतः श्वास्थवोचपप्तम्" सूत्रसे असके स्थानमें अस्थ आदेश होकर "स्वरादेस्तासु" सूत्रसे 'अ' के स्थानमें वृद्धि होकर 'आस्थः' रूप बनता है।
वास्तवमें केवल प्रमाणको ही सत्य कहा जा सकता है । नयोंसे वस्तुके सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान नहीं होता, इसलिये नयको सत्य नहीं कह सकते । अनुयोगद्वारसे प्रज्ञापना तक पहुँचनेके लिये नय अनुयोगके द्वार है, इसलिये नयोंको प्रमाणके समान कहा गया है। उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय ये चार अनुयोग-महानगरमें पहुँचनेके दरवाजे हैं। इनका स्वरूप विशेषावश्यकभाष्य (गाथा ९११-४; १५०५के आगे ) आदि ग्रन्थोंसे जानना चाहिये । यहाँ ग्रन्थके बढ़ जानेके भयसे सबका स्वरूप नहीं लिखा जाता। एक जगह श्लोकमें 'पथिन्' शब्द समासान्त है, और दूसरी जगह अव्युत्पन्न अकारांत है, इलिये 'पथ' शब्दका दो बार प्रयोग करनेमें दोष नहीं है।
दुर्नय, नय और प्रमाणमेंसे पहले नयका स्वरूप कहा जाता है। क्योंकि नयको बिना जाने दुर्नयका ज्ञान नहीं हो सकता। प्रमाणसे निश्चित किये हुए पदार्थों के एक अंश ज्ञान करनेको नय कहते हैं। प्रत्येक वस्तुमें अनन्त धर्म पाये जाते हैं, इन अनन्त धर्मोमें अपने इष्ट धर्मको जाननेको नय कहते हैं। वस्तुका प्रमाण द्वारा १. हैमसूत्रे ३-४-६० । २. हैमसूत्रे ४-३-१०३ । ३. हैमसूत्रे ४-४-३१ । ४. अणुओगद्दाराई महापुरस्सेव तस्स चत्तारि । ५. विशेषावश्यकभाष्ये ९११, ९१२, ९१३, ९१४, १५०५ ततः परम् ।