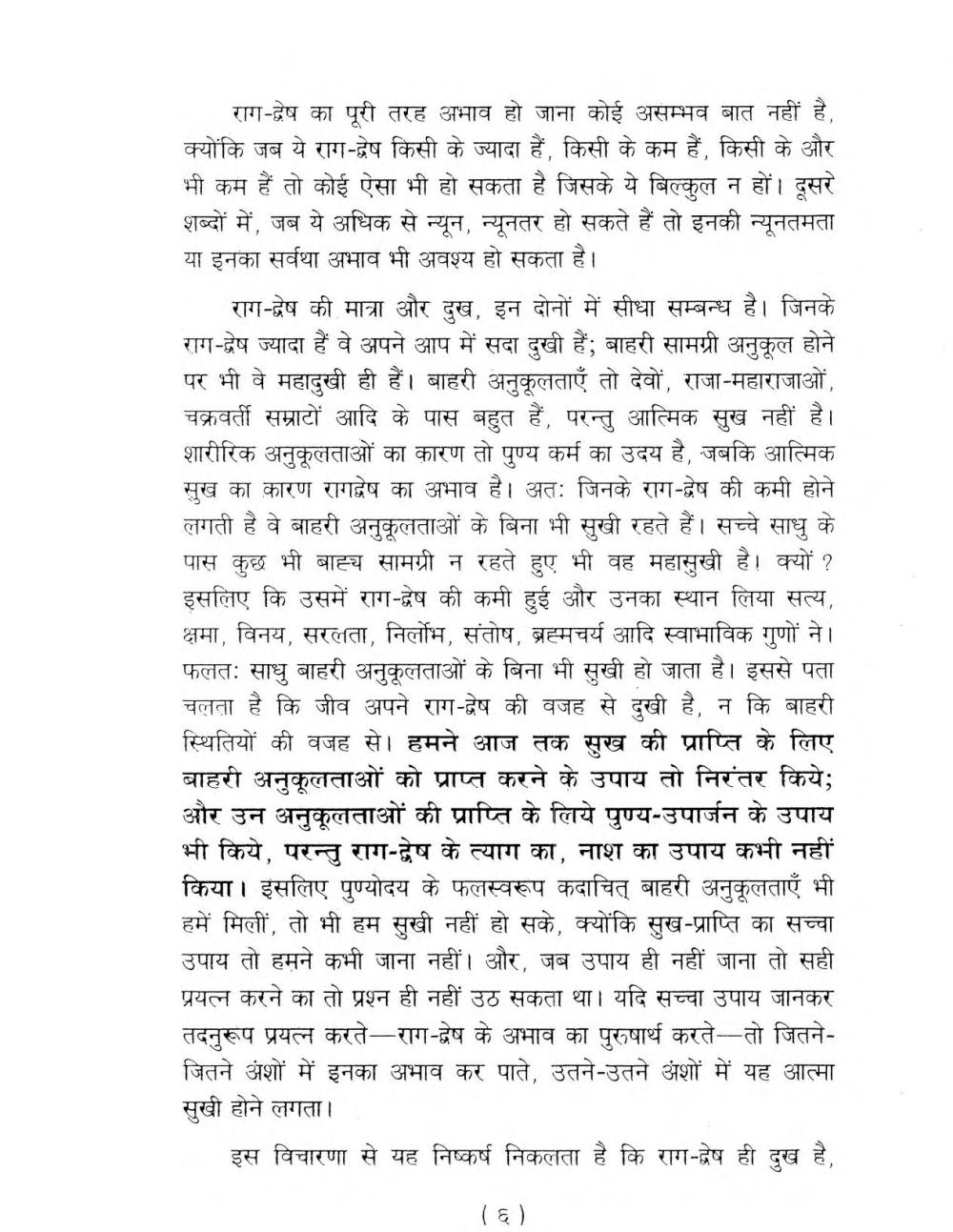________________
राग-द्वेष का पूरी तरह अभाव हो जाना कोई असम्भव बात नहीं है, क्योंकि जब ये राग-द्वेष किसी के ज्यादा हैं, किसी के कम हैं, किसी के और भी कम हैं तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके ये बिल्कुल न हों। दूसरे शब्दों में, जब ये अधिक से न्यून, न्यूनतर हो सकते हैं तो इनकी न्यूनतमता या इनका सर्वथा अभाव भी अवश्य हो सकता है।
राग-द्वेष की मात्रा और दुख, इन दोनों में सीधा सम्बन्ध है। जिनके राग-द्वेष ज्यादा हैं वे अपने आप में सदा दुखी हैं; बाहरी सामग्री अनुकूल होने पर भी वे महादुखी ही हैं। बाहरी अनुकूलताएँ तो देवों, राजा-महाराजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों आदि के पास बहुत हैं, परन्तु आत्मिक सुख नहीं है। शारीरिक अनुकूलताओं का कारण तो पुण्य कर्म का उदय है, जबकि आत्मिक सुख का कारण रागद्वेष का अभाव है। अत: जिनके राग-द्वेष की कमी होने लगती है वे बाहरी अनुकूलताओं के बिना भी सुखी रहते हैं। सच्चे साधु के पास कुछ भी बाह्य सामग्री न रहते हुए भी वह महासुखी है। क्यों ? इसलिए कि उसमें राग-द्वेष की कमी हुई और उनका स्थान लिया सत्य, क्षमा, विनय, सरलता, निर्लोभ, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि स्वाभाविक गुणों ने। फलतः साधु बाहरी अनुकूलताओं के बिना भी सुखी हो जाता है। इससे पता चलता है कि जीव अपने राग-द्वेष की वजह से दुखी है, न कि बाहरी स्थितियों की वजह से। हमने आज तक सुख की प्राप्ति के लिए बाहरी अनुकूलताओं को प्राप्त करने के उपाय तो निरंतर किये; और उन अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिये पुण्य-उपार्जन के उपाय भी किये, परन्तु राग-द्वेष के त्याग का, नाश का उपाय कभी नहीं किया। इसलिए पुण्योदय के फलस्वरूप कदाचित् बाहरी अनुकूलताएँ भी हमें मिलीं, तो भी हम सुखी नहीं हो सके, क्योंकि सुख-प्राप्ति का सच्चा उपाय तो हमने कभी जाना नहीं। और, जब उपाय ही नहीं जाना तो सही प्रयत्न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। यदि सच्चा उपाय जानकर तदनुरूप प्रयत्न करते-राग-द्वेष के अभाव का पुरुषार्थ करते-तो जितनेजितने अंशों में इनका अभाव कर पाते, उतने-उतने अंशों में यह आत्मा सुखी होने लगता।
इस विचारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि राग-द्वेष ही दुख है,
(६)