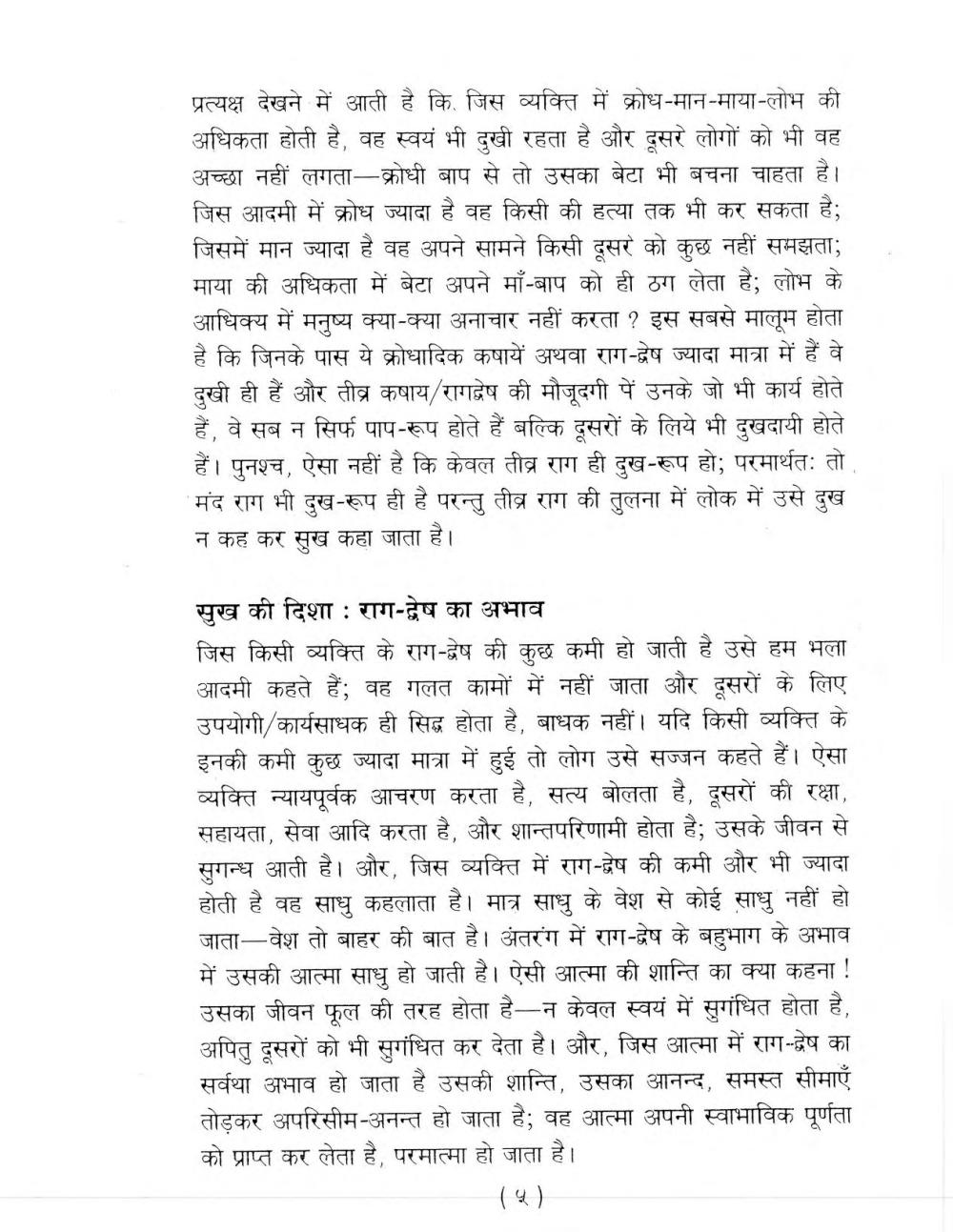________________
प्रत्यक्ष देखने में आती है कि जिस व्यक्ति में क्रोध-मान-माया-लोभ की अधिकता होती है, वह स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरे लोगों को भी वह अच्छा नहीं लगता—क्रोधी बाप से तो उसका बेटा भी बचना चाहता है। जिस आदमी में क्रोध ज्यादा है वह किसी की हत्या तक भी कर सकता है; जिसमें मान ज्यादा है वह अपने सामने किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता; माया की अधिकता में बेटा अपने माँ-बाप को ही ठग लेता है; लोभ के आधिक्य में मनुष्य क्या-क्या अनाचार नहीं करता ? इस सबसे मालूम होता है कि जिनके पास ये क्रोधादिक कषायें अथवा राग-द्वेष ज्यादा मात्रा में हैं वे दुखी ही हैं और तीव्र कषाय/रागद्वेष की मौजूदगी में उनके जो भी कार्य होते हैं, वे सब न सिर्फ पाप-रूप होते हैं बल्कि दूसरों के लिये भी दुखदायी होते हैं। पुनश्च, ऐसा नहीं है कि केवल तीव्र राग ही दुख-रूप हो; परमार्थत: तो मंद राग भी दुख-रूप ही है परन्तु तीव्र राग की तुलना में लोक में उसे दुख न कह कर सुख कहा जाता है।
सुख की दिशा : राग-द्वेष का अभाव जिस किसी व्यक्ति के राग-द्वेष की कुछ कमी हो जाती है उसे हम भला आदमी कहते हैं; वह गलत कामों में नहीं जाता और दूसरों के लिए उपयोगी/कार्यसाधक ही सिद्ध होता है, बाधक नहीं। यदि किसी व्यक्ति के इनकी कमी कुछ ज्यादा मात्रा में हुई तो लोग उसे सज्जन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्वक आचरण करता है, सत्य बोलता है, दूसरों की रक्षा, सहायता, सेवा आदि करता है, और शान्तपरिणामी होता है; उसके जीवन से सुगन्ध आती है। और, जिस व्यक्ति में राग-द्वेष की कमी और भी ज्यादा होती है वह साधु कहलाता है। मात्र साधु के वेश से कोई साधु नहीं हो जाता–वेश तो बाहर की बात है। अंतरंग में राग-द्वेष के बहुभाग के अभाव में उसकी आत्मा साधु हो जाती है। ऐसी आत्मा की शान्ति का क्या कहना ! उसका जीवन फूल की तरह होता है-न केवल स्वयं में सुगंधित होता है, अपितु दूसरों को भी सुगंधित कर देता है। और, जिस आत्मा में राग-द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है उसकी शान्ति, उसका आनन्द, समस्त सीमाएँ तोड़कर अपरिसीम-अनन्त हो जाता है; वह आत्मा अपनी स्वाभाविक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा हो जाता है।
(५)