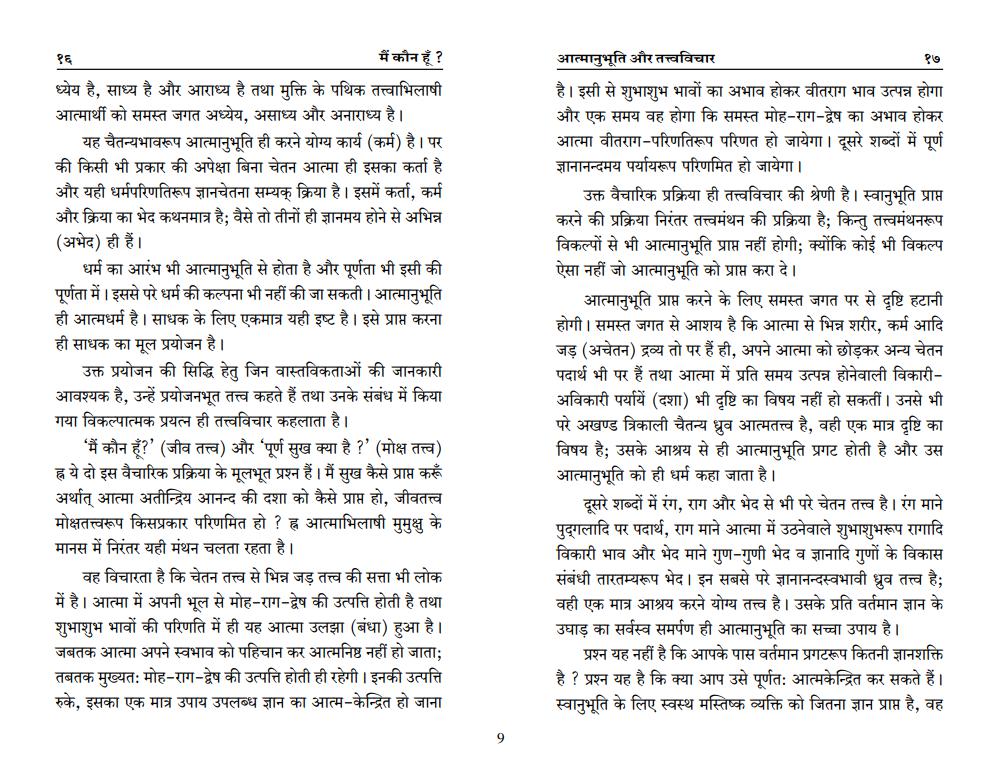________________
मैं कौन हूँ?
ध्येय है, साध्य है और आराध्य है तथा मुक्ति के पथिक तत्त्वाभिलाषी आत्मार्थी को समस्त जगत अध्येय, असाध्य और अनाराध्य है।
यह चैतन्यभावरूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य (कर्म) है। पर की किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका कर्ता है और यही धर्मपरिणतिरूप ज्ञानचेतना सम्यक् क्रिया है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का भेद कथनमात्र है; वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न (अभेद) ही हैं।
धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में । इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है।
उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्त्व कहते हैं तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्त्वविचार कहलाता है। ___मैं कौन हूँ?' (जीव तत्त्व) और पूर्ण सुख क्या है ?' (मोक्ष तत्त्व) ह्र ये दो इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न हैं। मैं सुख कैसे प्राप्त करूँ अर्थात् आत्मा अतीन्द्रिय आनन्द की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीवतत्त्व मोक्षतत्त्वरूप किसप्रकार परिणमित हो ? ह्र आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है।
वह विचारता है कि चेतन तत्त्व से भिन्न जड़ तत्त्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह-राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा (बंधा) हुआ है। जबतक आत्मा अपने स्वभाव को पहिचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता; तबतक मुख्यतः मोह-राग-द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके, इसका एक मात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म-केन्द्रित हो जाना
आत्मानुभूति और तत्त्वविचार है। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा और एक समय वह होगा कि समस्त मोह-राग-द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग-परिणतिरूप परिणत हो जायेगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानन्दमय पर्यायरूप परिणमित हो जायेगा।
उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्त्वविचार की श्रेणी है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्त्वमंथन की प्रक्रिया है; किन्तु तत्त्वमंथनरूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी; क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे।
आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ (अचेतन) द्रव्य तो पर हैं ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होनेवाली विकारीअविकारी पर्यायें (दशा) भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकतीं। उनसे भी परे अखण्ड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्मतत्त्व है, वही एक मात्र दृष्टि का विषय है; उसके आश्रय से ही आत्मानुभूति प्रगट होती है और उस आत्मानुभूति को ही धर्म कहा जाता है। ___ दूसरे शब्दों में रंग, राग और भेद से भी परे चेतन तत्त्व है। रंग माने पुद्गलादि पर पदार्थ, राग माने आत्मा में उठनेवाले शुभाशुभरूप रागादि विकारी भाव और भेद माने गुण-गुणी भेद व ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्यरूप भेद। इन सबसे परे ज्ञानानन्दस्वभावी ध्रुव तत्त्व है; वही एक मात्र आश्रय करने योग्य तत्त्व है। उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। ___ प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रगटरूप कितनी ज्ञानशक्ति है ? प्रश्न यह है कि क्या आप उसे पूर्णत: आत्मकेन्द्रित कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है, वह